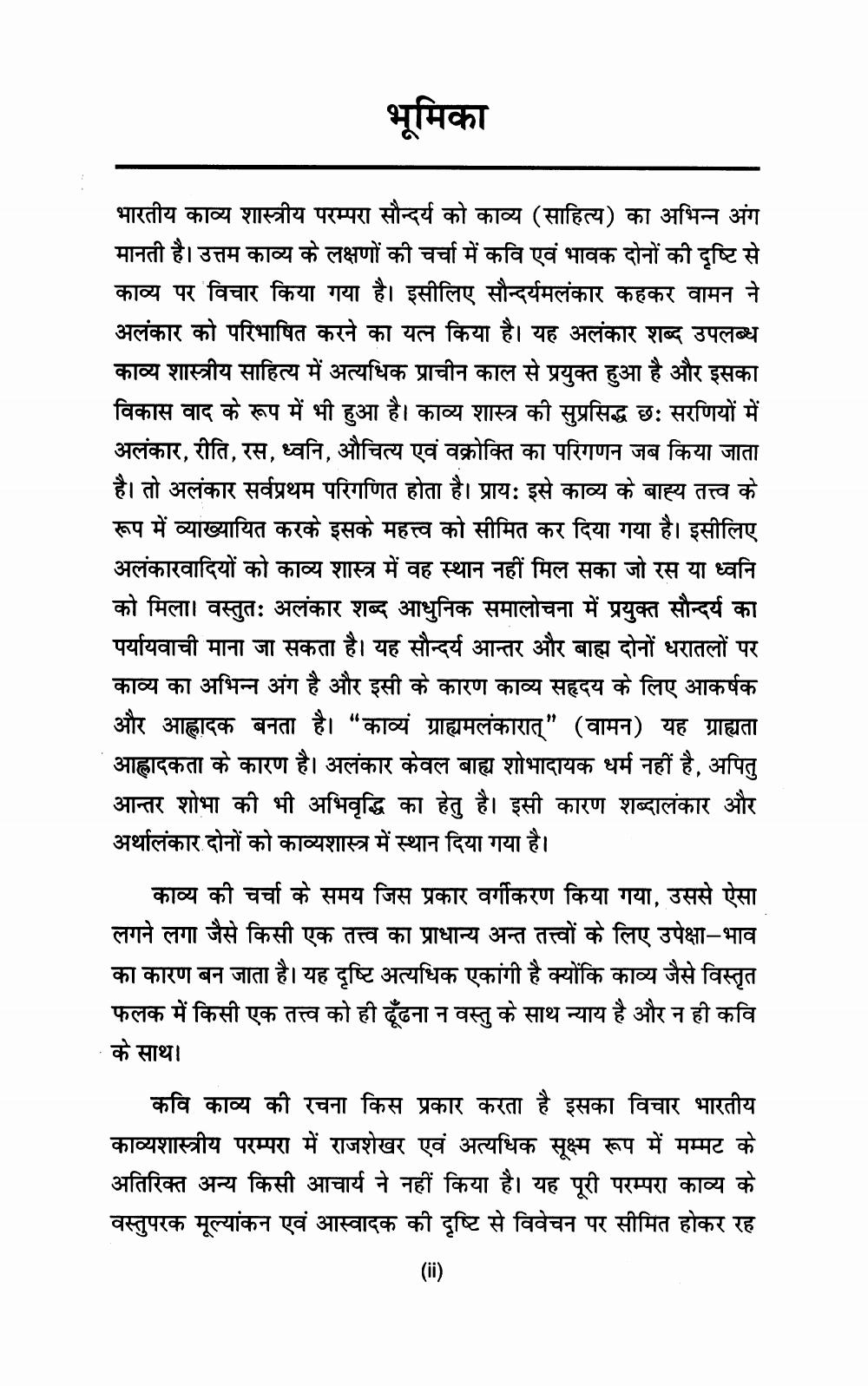________________
भूमिका
भारतीय काव्य शास्त्रीय परम्परा सौन्दर्य को काव्य (साहित्य) का अभिन्न अंग मानती है। उत्तम काव्य के लक्षणों की चर्चा में कवि एवं भावक दोनों की दृष्टि से काव्य पर विचार किया गया है। इसीलिए सौन्दर्यमलंकार कहकर वामन ने अलंकार को परिभाषित करने का यत्न किया है। यह अलंकार शब्द उपलब्ध काव्य शास्त्रीय साहित्य में अत्यधिक प्राचीन काल से प्रयुक्त हुआ है और इसका विकास वाद के रूप में भी हुआ है। काव्य शास्त्र की सुप्रसिद्ध छः सरणियों में अलंकार, रीति, रस, ध्वनि, औचित्य एवं वक्रोक्ति का परिगणन जब किया जाता है। तो अलंकार सर्वप्रथम परिगणित होता है। प्रायः इसे काव्य के बाह्य तत्त्व के रूप में व्याख्यायित करके इसके महत्त्व को सीमित कर दिया गया है। इसीलिए अलंकारवादियों को काव्य शास्त्र में वह स्थान नहीं मिल सका जो रस या ध्वनि को मिला। वस्तुतः अलंकार शब्द आधुनिक समालोचना में प्रयुक्त सौन्दर्य का पर्यायवाची माना जा सकता है। यह सौन्दर्य आन्तर और बाह्म दोनों धरातलों पर काव्य का अभिन्न अंग है और इसी के कारण काव्य सहृदय के लिए आकर्षक और आह्लादक बनता है। "काव्यं ग्राह्यमलंकारात्" (वामन) यह ग्राह्यता आह्लादकता के कारण है। अलंकार केवल बाह्य शोभादायक धर्म नहीं है, अपितु आन्तर शोभा की भी अभिवृद्धि का हेतु है। इसी कारण शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों को काव्यशास्त्र में स्थान दिया गया है।
काव्य की चर्चा के समय जिस प्रकार वर्गीकरण किया गया, उससे ऐसा लगने लगा जैसे किसी एक तत्त्व का प्राधान्य अन्त तत्त्वों के लिए उपेक्षा-भाव का कारण बन जाता है। यह दृष्टि अत्यधिक एकांगी है क्योंकि काव्य जैसे विस्तृत फलक में किसी एक तत्त्व को ही ढूँढना न वस्तु के साथ न्याय है और न ही कवि के साथ।
कवि काव्य की रचना किस प्रकार करता है इसका विचार भारतीय काव्यशास्त्रीय परम्परा में राजशेखर एवं अत्यधिक सूक्ष्म रूप में मम्मट के अतिरिक्त अन्य किसी आचार्य ने नहीं किया है। यह पूरी परम्परा काव्य के वस्तुपरक मूल्यांकन एवं आस्वादक की दृष्टि से विवेचन पर सीमित होकर रह