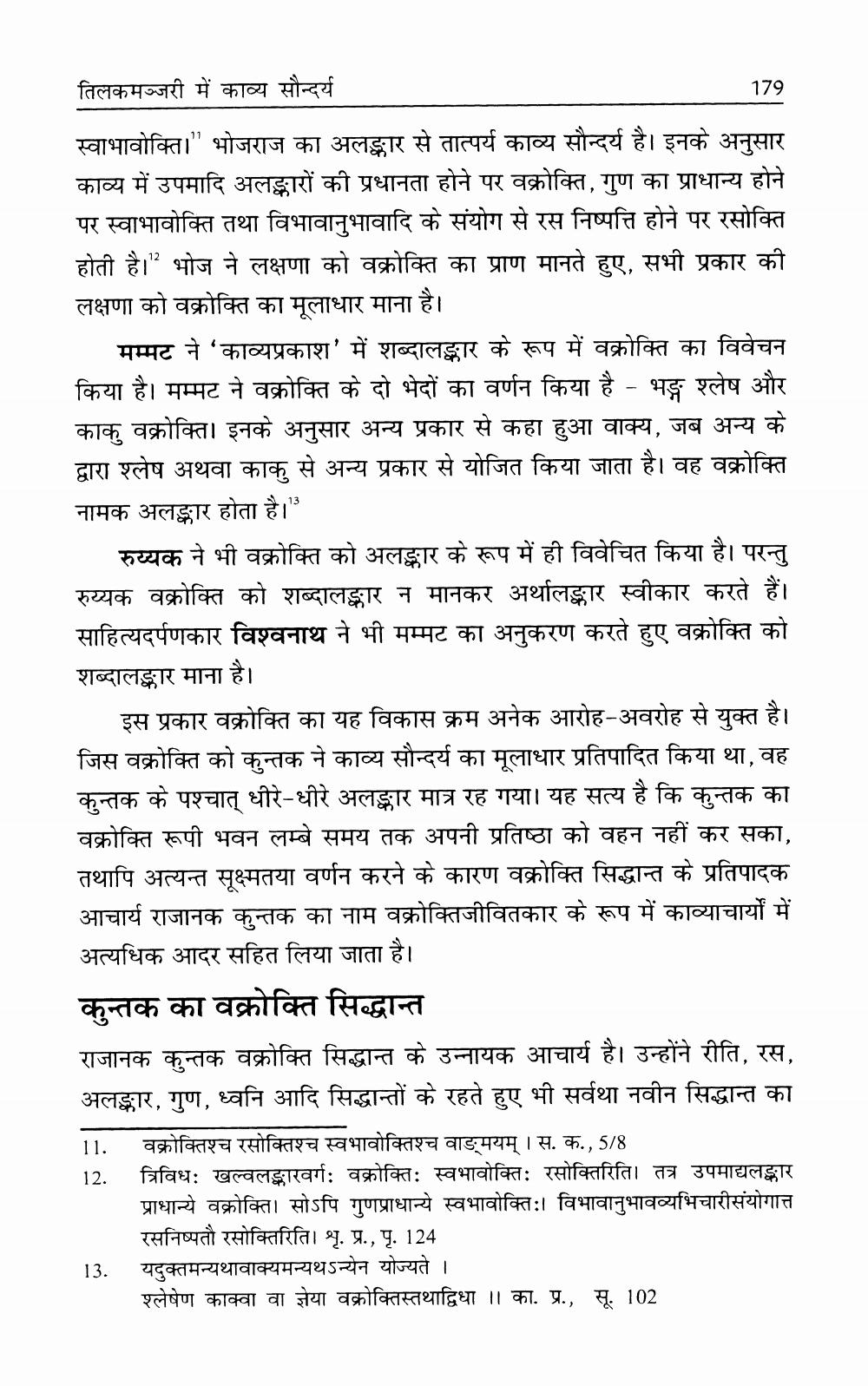________________
तिलकमञ्जरी में काव्य सौन्दर्य
179
स्वाभावोक्ति।" भोजराज का अलङ्कार से तात्पर्य काव्य सौन्दर्य है। इनके अनुसार काव्य में उपमादि अलङ्कारों की प्रधानता होने पर वक्रोक्ति, गुण का प्राधान्य होने पर स्वाभावोक्ति तथा विभावानुभावादि के संयोग से रस निष्पत्ति होने पर रसोक्ति होती है।" भोज ने लक्षणा को वक्रोक्ति का प्राण मानते हुए, सभी प्रकार की लक्षणा को वक्रोक्ति का मूलाधार माना है।
__ मम्मट ने 'काव्यप्रकाश' में शब्दालङ्कार के रूप में वक्रोक्ति का विवेचन किया है। मम्मट ने वक्रोक्ति के दो भेदों का वर्णन किया है - भङ्ग श्लेष और काकु वक्रोक्ति। इनके अनुसार अन्य प्रकार से कहा हुआ वाक्य, जब अन्य के द्वारा श्लेष अथवा काकु से अन्य प्रकार से योजित किया जाता है। वह वक्रोक्ति नामक अलङ्कार होता है।''
रुय्यक ने भी वक्रोक्ति को अलङ्कार के रूप में ही विवेचित किया है। परन्तु रुय्यक वक्रोक्ति को शब्दालङ्कार न मानकर अर्थालङ्कार स्वीकार करते हैं। साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ ने भी मम्मट का अनुकरण करते हुए वक्रोक्ति को शब्दालङ्कार माना है।
इस प्रकार वक्रोक्ति का यह विकास क्रम अनेक आरोह-अवरोह से युक्त है। जिस वक्रोक्ति को कुन्तक ने काव्य सौन्दर्य का मूलाधार प्रतिपादित किया था, वह कुन्तक के पश्चात् धीरे-धीरे अलङ्कार मात्र रह गया। यह सत्य है कि कुन्तक का वक्रोक्ति रूपी भवन लम्बे समय तक अपनी प्रतिष्ठा को वहन नहीं कर सका, तथापि अत्यन्त सूक्ष्मतया वर्णन करने के कारण वक्रोक्ति सिद्धान्त के प्रतिपादक आचार्य राजानक कुन्तक का नाम वक्रोक्तिजीवितकार के रूप में काव्याचार्यों में अत्यधिक आदर सहित लिया जाता है। कुन्तक का वक्रोक्ति सिद्धान्त राजानक कुन्तक वक्रोक्ति सिद्धान्त के उन्नायक आचार्य है। उन्होंने रीति, रस, अलङ्कार, गुण, ध्वनि आदि सिद्धान्तों के रहते हुए भी सर्वथा नवीन सिद्धान्त का 11. वक्रोक्तिश्च रसोक्तिश्च स्वभावोक्तिश्च वाङ्मयम् । स. क., 5/8 12. त्रिविधः खल्वलकारवर्गः वक्रोक्तिः स्वभावोक्तिः रसोक्तिरिति। तत्र उपमाद्यलङ्कार
प्राधान्ये वक्रोक्ति। सोऽपि गुणप्राधान्ये स्वभावोक्तिः। विभावानुभावव्यभिचारीसंयोगात्त
रसनिष्पतौ रसोक्तिरिति। शृ. प्र., पृ. 124 13. यदुक्तमन्यथावाक्यमन्यथऽन्येन योज्यते ।
श्लेषेण काक्वा वा ज्ञेया वक्रोक्तिस्तथाद्विधा ।। का. प्र., सू. 102