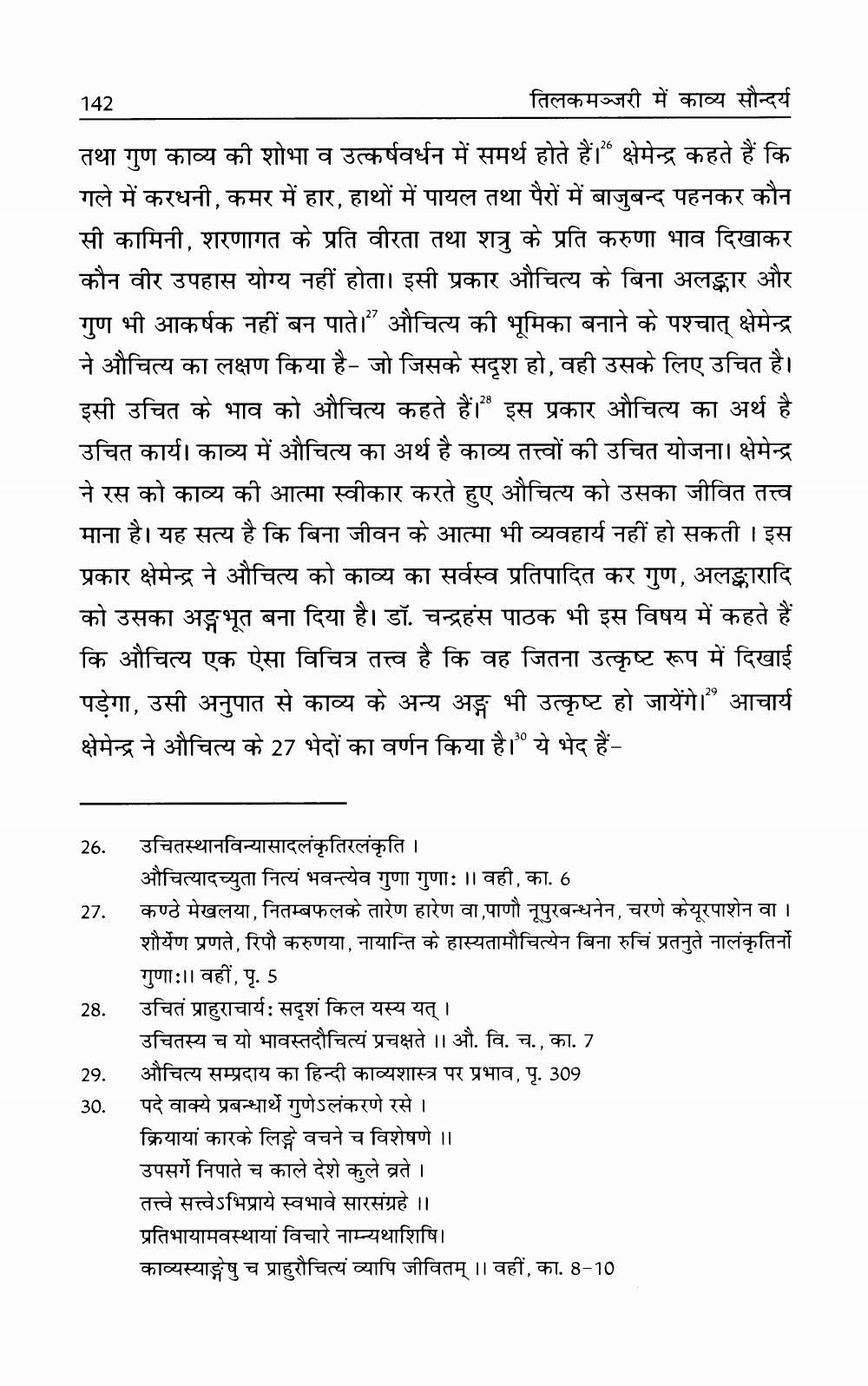________________
142
तिलकमञ्जरी में काव्य सौन्दर्य तथा गुण काव्य की शोभा व उत्कर्षवर्धन में समर्थ होते हैं। क्षेमेन्द्र कहते हैं कि गले में करधनी, कमर में हार, हाथों में पायल तथा पैरों में बाजुबन्द पहनकर कौन सी कामिनी, शरणागत के प्रति वीरता तथा शत्रु के प्रति करुणा भाव दिखाकर कौन वीर उपहास योग्य नहीं होता। इसी प्रकार औचित्य के बिना अलङ्कार और गुण भी आकर्षक नहीं बन पाते।" औचित्य की भूमिका बनाने के पश्चात् क्षेमेन्द्र ने औचित्य का लक्षण किया है- जो जिसके सदृश हो, वही उसके लिए उचित है। इसी उचित के भाव को औचित्य कहते हैं। इस प्रकार औचित्य का अर्थ है उचित कार्य। काव्य में औचित्य का अर्थ है काव्य तत्त्वों की उचित योजना। क्षेमेन्द्र ने रस को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हुए औचित्य को उसका जीवित तत्त्व माना है। यह सत्य है कि बिना जीवन के आत्मा भी व्यवहार्य नहीं हो सकती । इस प्रकार क्षेमेन्द्र ने औचित्य को काव्य का सर्वस्व प्रतिपादित कर गुण, अलङ्कारादि को उसका अङ्गभूत बना दिया है। डॉ. चन्द्रहंस पाठक भी इस विषय में कहते हैं कि औचित्य एक ऐसा विचित्र तत्त्व है कि वह जितना उत्कृष्ट रूप में दिखाई पड़ेगा, उसी अनुपात से काव्य के अन्य अङ्ग भी उत्कृष्ट हो जायेंगे।” आचार्य क्षेमेन्द्र ने औचित्य के 27 भेदों का वर्णन किया है। ये भेद हैं
26. उचितस्थानविन्यासादलंकृतिरलंकृति ।
औचित्यादच्युता नित्यं भवन्त्येव गुणा गुणाः ।। वही, का. 6 27. कण्ठे मेखलया, नितम्बफलके तारेण हारेण वा,पाणौ नूपुरबन्धनेन, चरणे केयूरपाशेन वा ।
शौर्येण प्रणते, रिपौ करुणया, नायान्ति के हास्यतामौचित्येन बिना रुचिं प्रतनुते नालंकृति!
गुणा:।। वहीं, पृ. 5 __उचितं प्राहुराचार्यः सदृशं किल यस्य यत् ।
उचितस्य च यो भावस्तदौचित्यं प्रचक्षते ।। औ. वि. च., का. 7 29. औचित्य सम्प्रदाय का हिन्दी काव्यशास्त्र पर प्रभाव, पृ. 309
पदे वाक्ये प्रबन्धार्थे गुणेऽलंकरणे रसे । क्रियायां कारके लिङ्गे वचने च विशेषणे ।। उपसर्गे निपाते च काले देशे कुले व्रते । तत्त्वे सत्त्वेऽभिप्राये स्वभावे सारसंग्रहे ।। प्रतिभायामवस्थायां विचारे नाम्न्यथाशिषि। काव्यस्याङ्गेषु च प्राहुरौचित्यं व्यापि जीवितम् ।। वहीं, का. 8-10