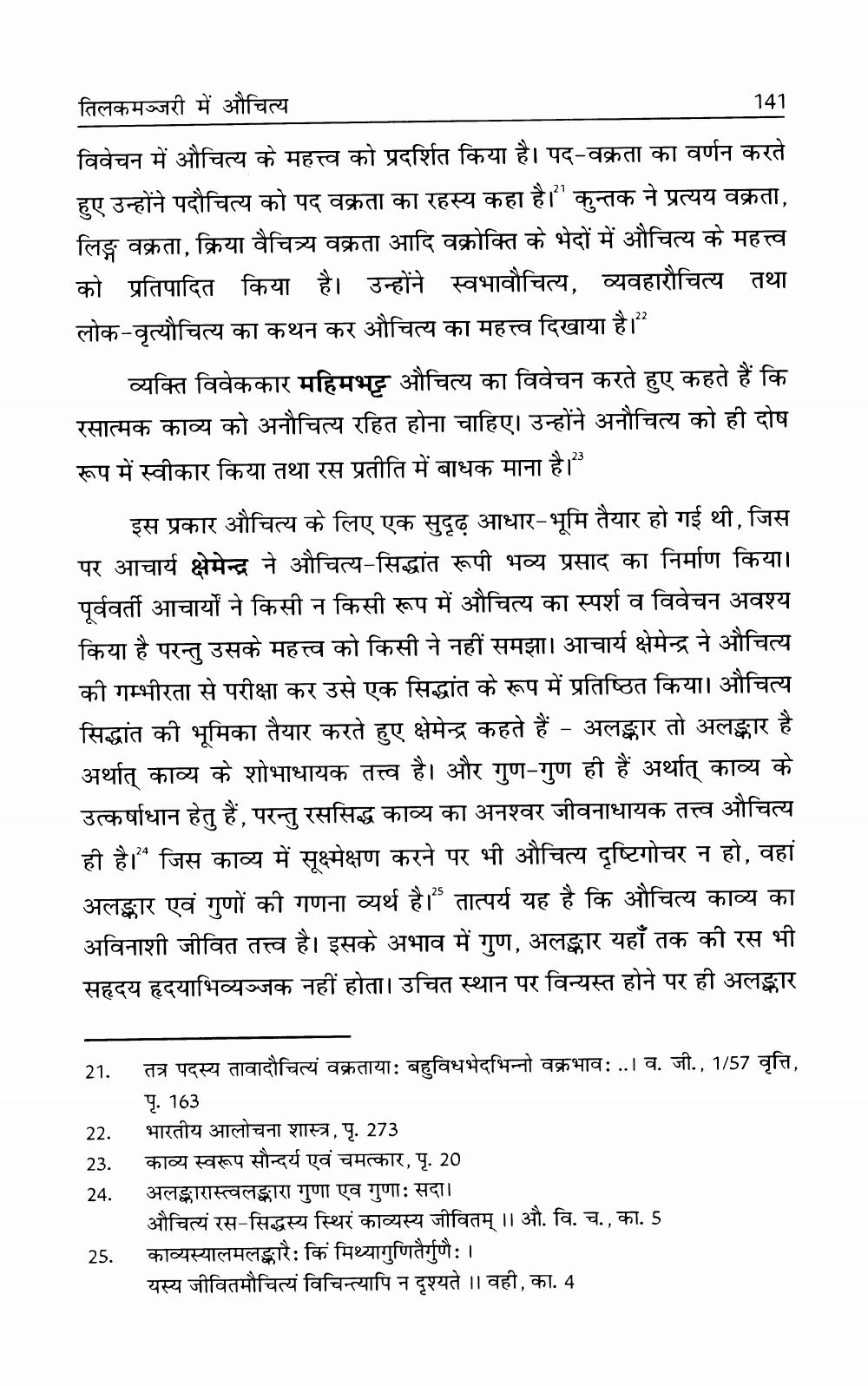________________
तिलकमञ्जरी में औचित्य
141 विवेचन में औचित्य के महत्त्व को प्रदर्शित किया है। पद-वक्रता का वर्णन करते हुए उन्होंने पदौचित्य को पद वक्रता का रहस्य कहा है।' कुन्तक ने प्रत्यय वक्रता, लिङ्ग वक्रता, क्रिया वैचित्र्य वक्रता आदि वक्रोक्ति के भेदों में औचित्य के महत्त्व को प्रतिपादित किया है। उन्होंने स्वभावौचित्य, व्यवहारौचित्य तथा लोक-वृत्यौचित्य का कथन कर औचित्य का महत्त्व दिखाया है।
व्यक्ति विवेककार महिमभट्ट औचित्य का विवेचन करते हुए कहते हैं कि रसात्मक काव्य को अनौचित्य रहित होना चाहिए। उन्होंने अनौचित्य को ही दोष रूप में स्वीकार किया तथा रस प्रतीति में बाधक माना है।
इस प्रकार औचित्य के लिए एक सुदृढ़ आधार-भूमि तैयार हो गई थी, जिस पर आचार्य क्षेमेन्द्र ने औचित्य-सिद्धांत रूपी भव्य प्रसाद का निर्माण किया। पूर्ववर्ती आचार्यों ने किसी न किसी रूप में औचित्य का स्पर्श व विवेचन अवश्य किया है परन्तु उसके महत्त्व को किसी ने नहीं समझा। आचार्य क्षेमेन्द्र ने औचित्य की गम्भीरता से परीक्षा कर उसे एक सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित किया। औचित्य सिद्धांत की भूमिका तैयार करते हुए क्षेमेन्द्र कहते हैं - अलङ्कार तो अलङ्कार है अर्थात् काव्य के शोभाधायक तत्त्व है। और गुण-गुण ही हैं अर्थात् काव्य के उत्कर्षाधान हेतु हैं, परन्तु रससिद्ध काव्य का अनश्वर जीवनाधायक तत्त्व औचित्य ही है। जिस काव्य में सूक्ष्मेक्षण करने पर भी औचित्य दृष्टिगोचर न हो, वहां अलङ्कार एवं गुणों की गणना व्यर्थ है। तात्पर्य यह है कि औचित्य काव्य का अविनाशी जीवित तत्त्व है। इसके अभाव में गुण, अलङ्कार यहाँ तक की रस भी सहृदय हृदयाभिव्यञ्जक नहीं होता। उचित स्थान पर विन्यस्त होने पर ही अलङ्कार
22.
21. तत्र पदस्य तावादौचित्यं वक्रतायाः बहुविधभेदभिन्नो वक्रभावः ..। व. जी., 1/57 वृत्ति,
पृ. 163
भारतीय आलोचना शास्त्र, पृ. 273 23. काव्य स्वरूप सौन्दर्य एवं चमत्कार, पृ. 20
अलङ्कारास्त्वलङ्कारा गुणा एव गुणा: सदा।
औचित्यं रस-सिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम् ।। औ. वि. च., का. 5 25. काव्यस्यालमलङ्कारैः किं मिथ्यागुणितैर्गुणैः।।
यस्य जीवितमौचित्यं विचिन्त्यापि न दृश्यते ।। वही, का. 4