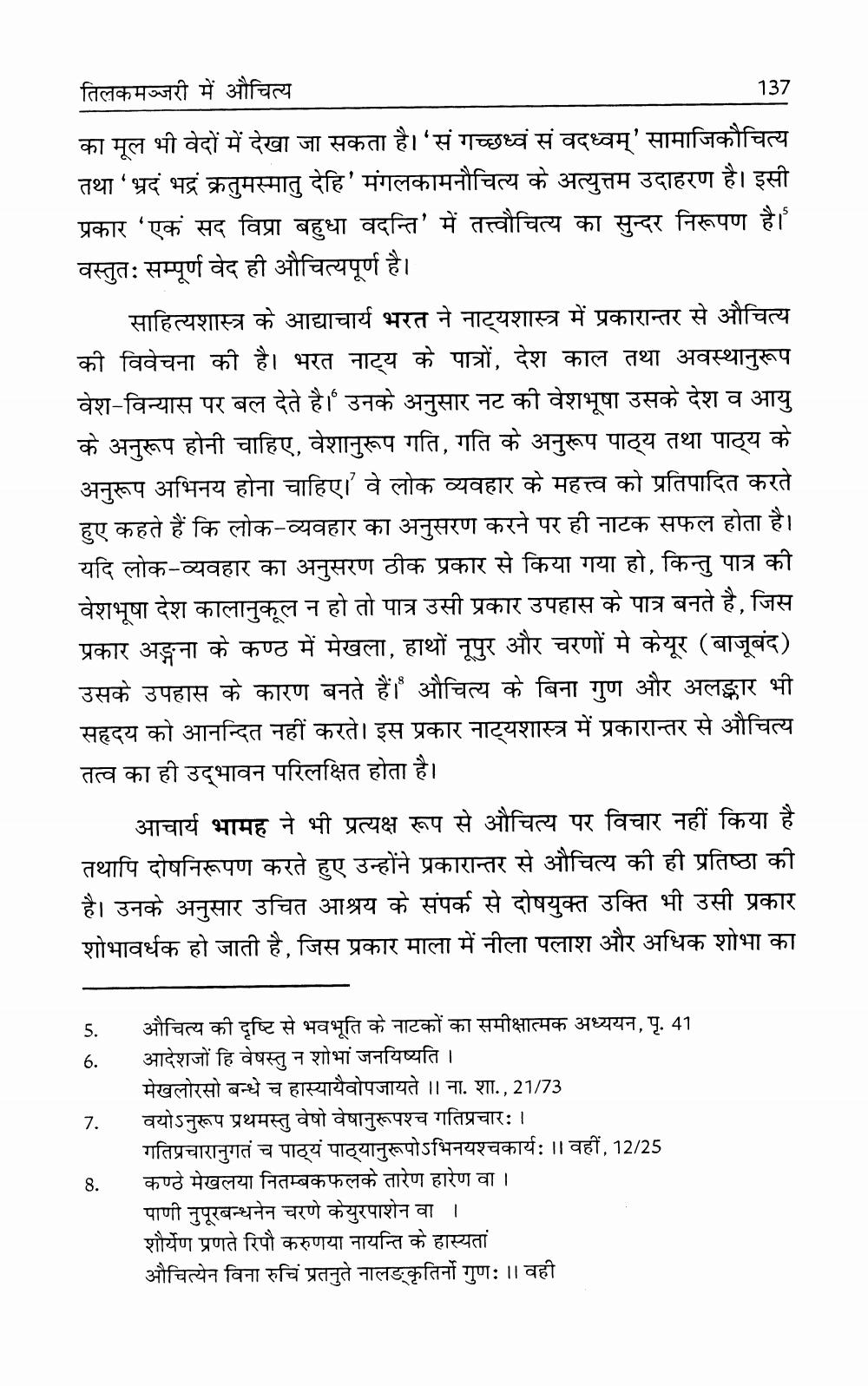________________
तिलकमञ्जरी में औचित्य
का मूल भी वेदों में देखा जा सकता है। 'सं गच्छध्वं सं वदध्वम्' सामाजिकौचित्य तथा 'भ्रदं भद्रं क्रतुमस्मातु देहि' मंगलकामनौचित्य के अत्युत्तम उदाहरण है। इसी प्रकार 'एक सद विप्रा बहुधा वदन्ति' में तत्त्वौचित्य का सुन्दर निरूपण है। वस्तुतः सम्पूर्ण वेद ही औचित्यपूर्ण है।
साहित्यशास्त्र के आद्याचार्य भरत ने नाट्यशास्त्र में प्रकारान्तर से औचित्य की विवेचना की है। भरत नाट्य के पात्रों, देश काल तथा अवस्थानुरूप वेश-विन्यास पर बल देते है।' उनके अनुसार नट की वेशभूषा उसके देश व आयु के अनुरूप होनी चाहिए, वेशानुरूप गति, गति के अनुरूप पाठ्य तथा पाठ्य के अनुरूप अभिनय होना चाहिए।' वे लोक व्यवहार के महत्त्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि लोक व्यवहार का अनुसरण करने पर ही नाटक सफल होता है। यदि लोक-व्यवहार का अनुसरण ठीक प्रकार से किया गया हो, किन्तु पात्र की वेशभूषा देश कालानुकूल न हो तो पात्र उसी प्रकार उपहास के पात्र बनते है, जिस प्रकार अङ्गना के कण्ठ में मेखला, हाथों नूपुर और चरणों मे केयूर (बाजूबंद) उसके उपहास के कारण बनते हैं ।" औचित्य के बिना गुण और अलङ्कार भी सहृदय को आनन्दित नहीं करते। इस प्रकार नाट्यशास्त्र में प्रकारान्तर से औचित्य तत्व का ही उद्भावन परिलक्षित होता है।
5.
6.
आचार्य भामह ने भी प्रत्यक्ष रूप से औचित्य पर विचार नहीं किया है तथापि दोषनिरूपण करते हुए उन्होंने प्रकारान्तर से औचित्य की ही प्रतिष्ठा की है। उनके अनुसार उचित आश्रय के संपर्क से दोषयुक्त उक्ति भी उसी प्रकार शोभावर्धक हो जाती है, जिस प्रकार माला में नीला पलाश और अधिक शोभा का
7.
-
8.
औचित्य की दृष्टि से भवभूति के नाटकों का समीक्षात्मक अध्ययन, पृ. 41
आदेशजों हि वेषस्तु न शोभां जनयिष्यति ।
मेखलोरसो बन्धे च हास्यायैवोपजायते ।। ना. शा., 21/73
137
वयोऽनुरूप प्रथमस्तु वेषो वेषानुरूपश्च गतिप्रचारः । गतिप्रचारानुगतं च पाठ्यं पाठ्यानुरूपोऽभिनयश्चकार्य: ।। वहीं, 12/25
कण्ठे मेखलया नितम्बकफलके तारेण हारेण वा । पाणी नुपूरबन्धनेन चरणे केयुरपाशेन वा । शौर्येण प्रणते रिपौ करुणया नायन्ति के हास्यतां औचित्येन विना रुचिं प्रतनुते नालङ्कृतिर्नो गुण: ।। वही