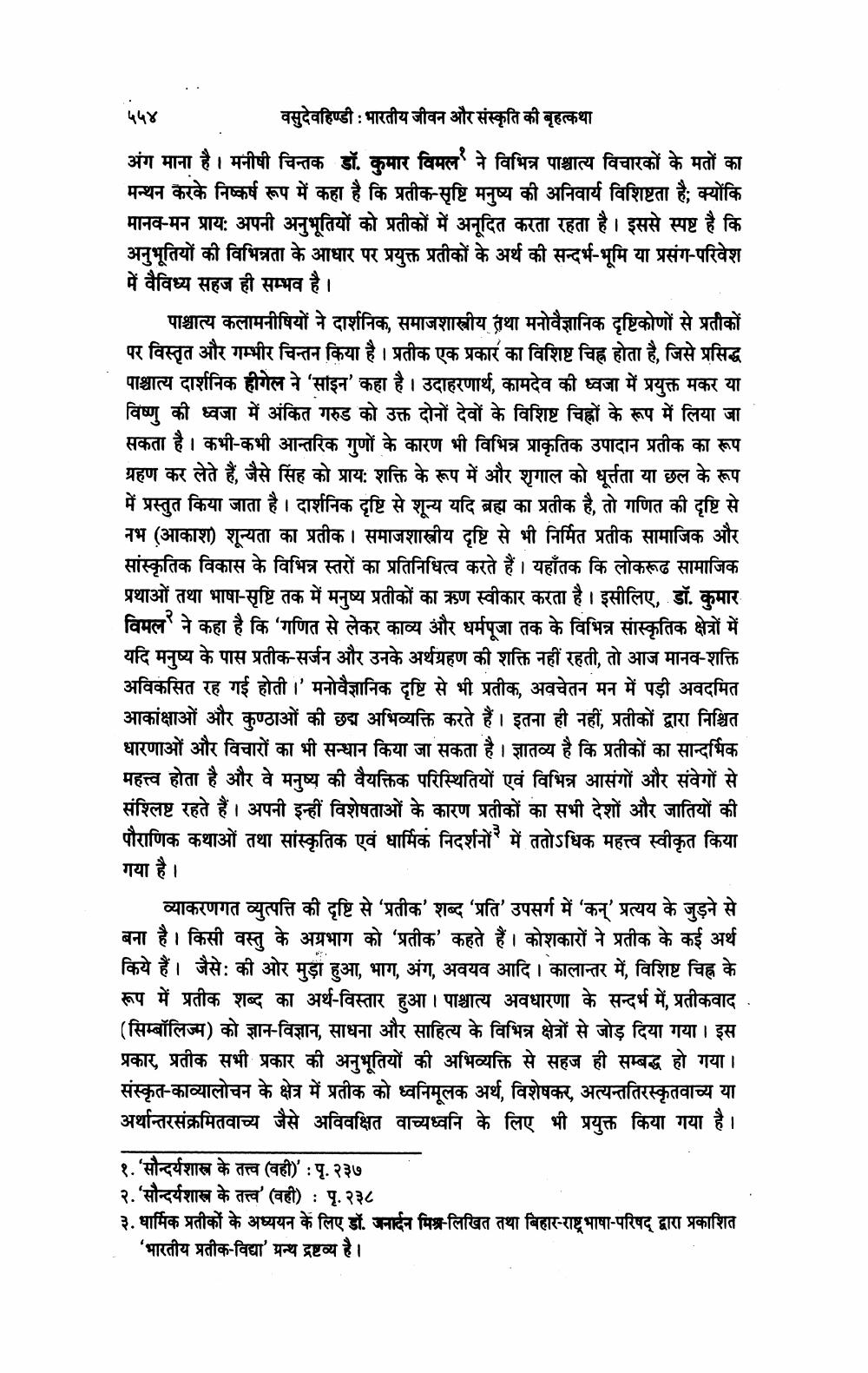________________
पं५४
वसुदेवहिण्डी : भारतीय जीवन और संस्कृति की बृहत्कथा
अंग माना है । मनीषी चिन्तक डॉ. कुमार विमल' ने विभिन्न पाश्चात्य विचारकों के मतों का मन्थन करके निष्कर्ष रूप में कहा है कि प्रतीक- सृष्टि मनुष्य की अनिवार्य विशिष्टता है; क्योंकि मानव-मन प्राय: अपनी अनुभूतियों को प्रतीकों में अनूदित करता रहता है। इससे स्पष्ट है कि अनुभूतियों की विभिन्नता के आधार पर प्रयुक्त प्रतीकों के अर्थ की सन्दर्भ- भूमि या प्रसंग- परिवेश में वैविध्य सहज ही सम्भव है ।
पाश्चात्य कलामनीषियों ने दार्शनिक, समाजशास्त्रीय तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों से प्रतीकों पर विस्तृत और गम्भीर चिन्तन किया है। प्रतीक एक प्रकार का विशिष्ट चिह्न होता है, जिसे प्रसिद्ध पाश्चात्य दार्शनिक हीगेल ने 'साइन' कहा है। उदाहरणार्थ, कामदेव की ध्वजा में प्रयुक्त मकर या विष्णु की ध्वजा में अंकित गरुड को उक्त दोनों देवों के विशिष्ट चिह्नों के रूप लिया जा सकता है। कभी-कभी आन्तरिक गुणों के कारण भी विभिन्न प्राकृतिक उपादान प्रतीक का रूप ग्रहण कर लेते हैं, जैसे सिंह को प्राय: शक्ति के रूप में और शृगाल को धूर्तता या छल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है । दार्शनिक दृष्टि से शून्य यदि ब्रह्म का प्रतीक है, तो गणित की दृष्टि से नभ (आकाश) शून्यता का प्रतीक । समाजशास्त्रीय दृष्टि से भी निर्मित प्रतीक सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं । यहाँतक कि लोकरूढ सामाजिक प्रथाओं तथा भाषा-सृष्टि तक में मनुष्य प्रतीकों का ऋण स्वीकार करता है। इसीलिए, डॉ. कुमार विमल' ने कहा है कि 'गणित से लेकर काव्य और धर्मपूजा तक के विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में यदि मनुष्य के पास प्रतीक-सर्जन और उनके अर्थग्रहण की शक्ति नहीं रहती, तो आज मानव-शक्ति अविकसित रह गई होती ।' मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी प्रतीक, अवचेतन मन में पड़ी अवदमित आकांक्षाओं और कुण्ठाओं की छद्म अभिव्यक्ति करते हैं। इतना ही नहीं, प्रतीकों द्वारा निश्चित धारणाओं और विचारों का भी सन्धान किया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि प्रतीकों का सान्दर्भिक महत्त्व होता है और वे मनुष्य की वैयक्तिक परिस्थितियों एवं विभिन्न आसंगों और संवेगों से संश्लिष्ट रहते हैं। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण प्रतीकों का सभी देशों और जातियों की पौराणिक कथाओं तथा सांस्कृतिक एवं धार्मिकं निदर्शनों में ततोऽधिक महत्त्व स्वीकृत किया गया है ।
व्याकरणगत व्युत्पत्ति की दृष्टि से 'प्रतीक' शब्द 'प्रति' उपसर्ग में 'कन्' प्रत्यय के जुड़ने से बना है। किसी वस्तु के अग्रभाग को 'प्रतीक' कहते हैं। कोशकारों ने प्रतीक के कई अर्थ किये हैं । जैसे की ओर मुड़ा हुआ, भाग, अंग, अवयव आदि । कालान्तर में, विशिष्ट चिह्न के रूप में प्रतीक शब्द का अर्थ-विस्तार हुआ । पाश्चात्य अवधारणा के सन्दर्भ में, प्रतीकवाद (सिम्बॉलिज्म) को ज्ञान-विज्ञान, साधना और साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों से जोड़ दिया गया। इस प्रकार, प्रतीक सभी प्रकार की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति से सहज ही सम्बद्ध हो गया । संस्कृत काव्यालोचन के क्षेत्र में प्रतीक को ध्वनिमूलक अर्थ, विशेषकर, अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य या अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य जैसे अविवक्षित वाच्यध्वनि के लिए भी प्रयुक्त किया गया है |
१. 'सौन्दर्यशास्त्र के तत्त्व (वही)' : पृ. २३७
२. 'सौन्दर्यशास्त्र के तत्त्व' (वही) : पृ. २३८
३. धार्मिक प्रतीकों के अध्ययन के लिए डॉ. जनार्दन मिश्र - लिखित तथा बिहार- राष्ट्र भाषा-परिषद् द्वारा प्रकाशित 'भारतीय प्रतीक - विद्या' ग्रन्थ द्रष्टव्य है ।