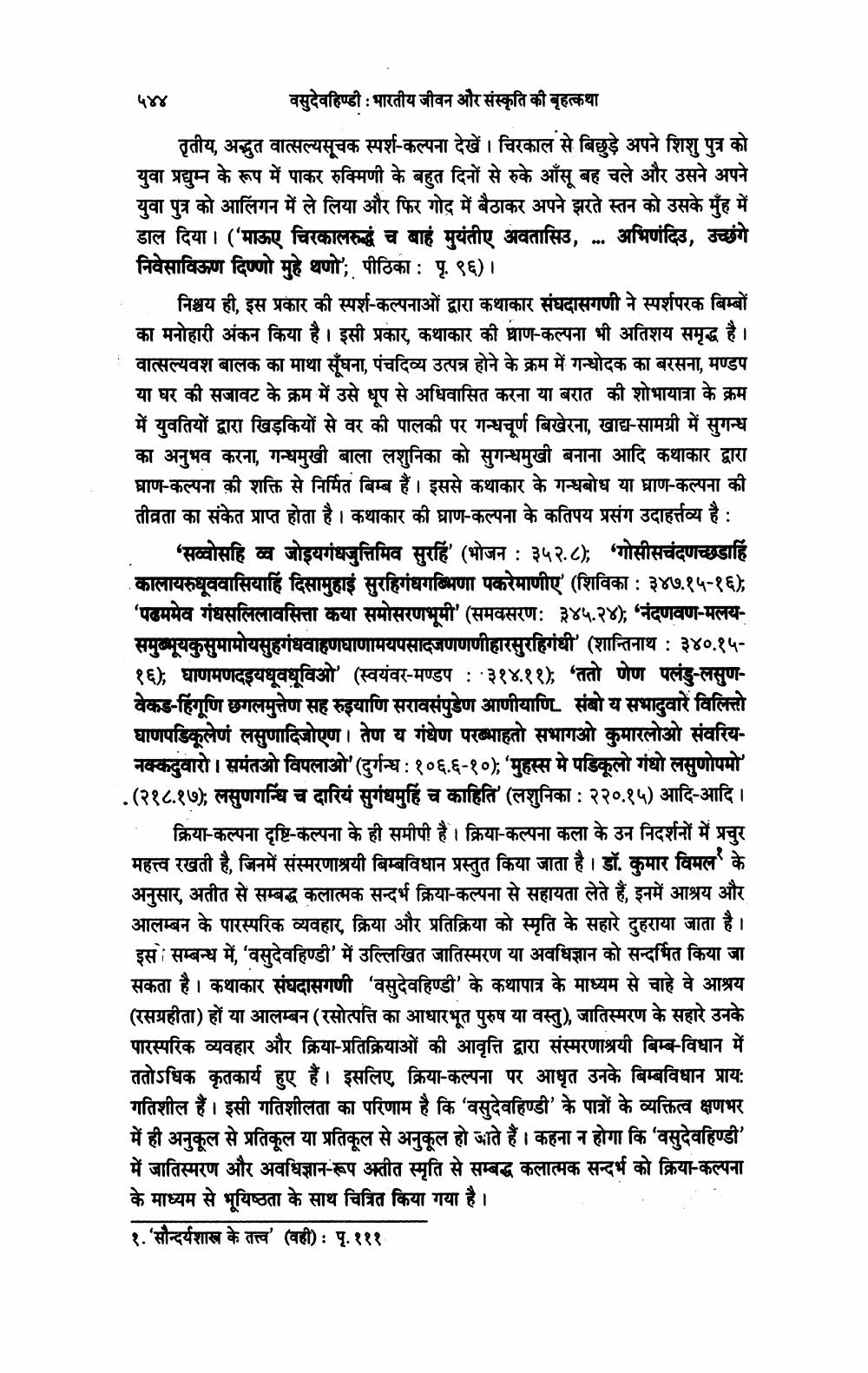________________
५४४
वसुदेवहिण्डी : भारतीय जीवन और संस्कृति की बृहत्कथा तृतीय, अद्भुत वात्सल्यसूचक स्पर्श-कल्पना देखें । चिरकाल से बिछुड़े अपने शिशु पुत्र को युवा प्रद्युम्न के रूप में पाकर रुक्मिणी के बहुत दिनों से रुके आँसू बह चले और उसने अपने युवा पुत्र को आलिंगन में ले लिया और फिर गोद में बैठाकर अपने झरते स्तन को उसके मुँह में डाल दिया। ('माऊए चिरकालरुद्धं च बाहं मुयंतीए अवतासिउ, ... अभिणंदिउ, उच्छंगे निवेसाविऊण दिण्णो मुहे थणो; पीठिका : पृ. ९६)।
निश्चय ही, इस प्रकार की स्पर्श-कल्पनाओं द्वारा कथाकार संघदासगणी ने स्पर्शपरक बिम्बों का मनोहारी अंकन किया है। इसी प्रकार, कथाकार की प्राण-कल्पना भी अतिशय समृद्ध है। वात्सल्यवश बालक का माथा सूंघना, पंचदिव्य उत्पन्न होने के क्रम में गन्धोदक का बरसना, मण्डप या घर की सजावट के क्रम में उसे धूप से अधिवासित करना या बरात की शोभायात्रा के क्रम में युवतियों द्वारा खिड़कियों से वर की पालकी पर गन्धचूर्ण बिखेरना, खाद्य-सामग्री में सुगन्ध का अनुभव करना, गन्धमुखी बाला लशुनिका को सुगन्धमुखी बनाना आदि कथाकार द्वारा घाण-कल्पना की शक्ति से निर्मित बिम्ब हैं। इससे कथाकार के गन्धबोध या घ्राण-कल्पना की तीव्रता का संकेत प्राप्त होता है । कथाकार की घाण-कल्पना के कतिपय प्रसंग उदाहर्त्तव्य है :
__'सव्वोसहि ब जोइयगंधजुत्तिमिव सुरहि' (भोजन : ३५२.८), 'गोसीसचंदणच्छडाहिं कालायरुधूववासियाहिं दिसामुहाई सुरहिगंधगब्मिणा पकरेमाणीए (शिविका : ३४७.१५-१६) 'पढममेव गंधसलिलावसित्ता कया समोसरणभूमी' (समवसरणः ३४५.२४), 'नंदणवण-मलयसमुन्भूयकुसुमामोयसुहगंधवाहणघाणामयपसादजणणणीहारसुरहिगंधी' (शान्तिनाथ : ३४०.१५१६); घाणमणदइयधूवधूविओ' (स्वयंवर-मण्डप : ३१४.११), 'ततो गेण पलंडु-लसुणवेकड-हिंगूणि छगलमुत्तेण सह रुझ्याणि सरावसंपुडेण आणीयाणि. संबो य सभाद्वारे विलितो घाणपडिकूलेणं लसुणादिजोएण। तेण य गंधेण परब्भाहतो सभागओ कुमारलोओ संवरियनक्कदुवारो। समंतओ विपलाओ' (दुर्गन्ध : १०६.६-१०); 'मुहस्स मे पडिकूलो गंधो लसुणोपमो' .(२१८.१७); लसुणगन्धिं च दारियं सुगंधमुहि च काहिति (लशुनिका : २२०.१५) आदि-आदि।
क्रिया-कल्पना दृष्टि-कल्पना के ही समीपी है। क्रिया-कल्पना कला के उन निदर्शनों में प्रचुर महत्त्व रखती है, जिनमें संस्मरणाश्रयी बिम्बविधान प्रस्तुत किया जाता है। डॉ. कुमार विमल' के अनुसार, अतीत से सम्बद्ध कलात्मक सन्दर्भ क्रिया-कल्पना से सहायता लेते हैं, इनमें आश्रय और आलम्बन के पारस्परिक व्यवहार, क्रिया और प्रतिक्रिया को स्मृति के सहारे दुहराया जाता है। इस सम्बन्ध में, 'वसुदेवहिण्डी' में उल्लिखित जातिस्मरण या अवधिज्ञान को सन्दर्मित किया जा सकता है। कथाकार संघदासगणी 'वसुदेवहिण्डी' के कथापात्र के माध्यम से चाहे वे आश्रय (रसग्रहीता) हों या आलम्बन (रसोत्पत्ति का आधारभूत पुरुष या वस्तु), जातिस्मरण के सहारे उनके पारस्परिक व्यवहार और क्रिया-प्रतिक्रियाओं की आवृत्ति द्वारा संस्मरणाश्रयी बिम्ब-विधान में ततोऽधिक कृतकार्य हुए हैं। इसलिए, क्रिया-कल्पना पर आधृत उनके बिम्बविधान प्राय: गतिशील हैं। इसी गतिशीलता का परिणाम है कि 'वसुदेवहिण्डी' के पात्रों के व्यक्तित्व क्षणभर में ही अनुकूल से प्रतिकूल या प्रतिकूल से अनुकूल हो जाते हैं। कहना न होगा कि 'वसुदेवहिण्डी' में जातिस्मरण और अवधिज्ञान-रूप अतीत स्मृति से सम्बद्ध कलात्मक सन्दर्भ को क्रिया-कल्पना के माध्यम से भूयिष्ठता के साथ चित्रित किया गया है। १. 'सौन्दर्यशास्त्र के तत्त्व' (वही) : पृ. १११