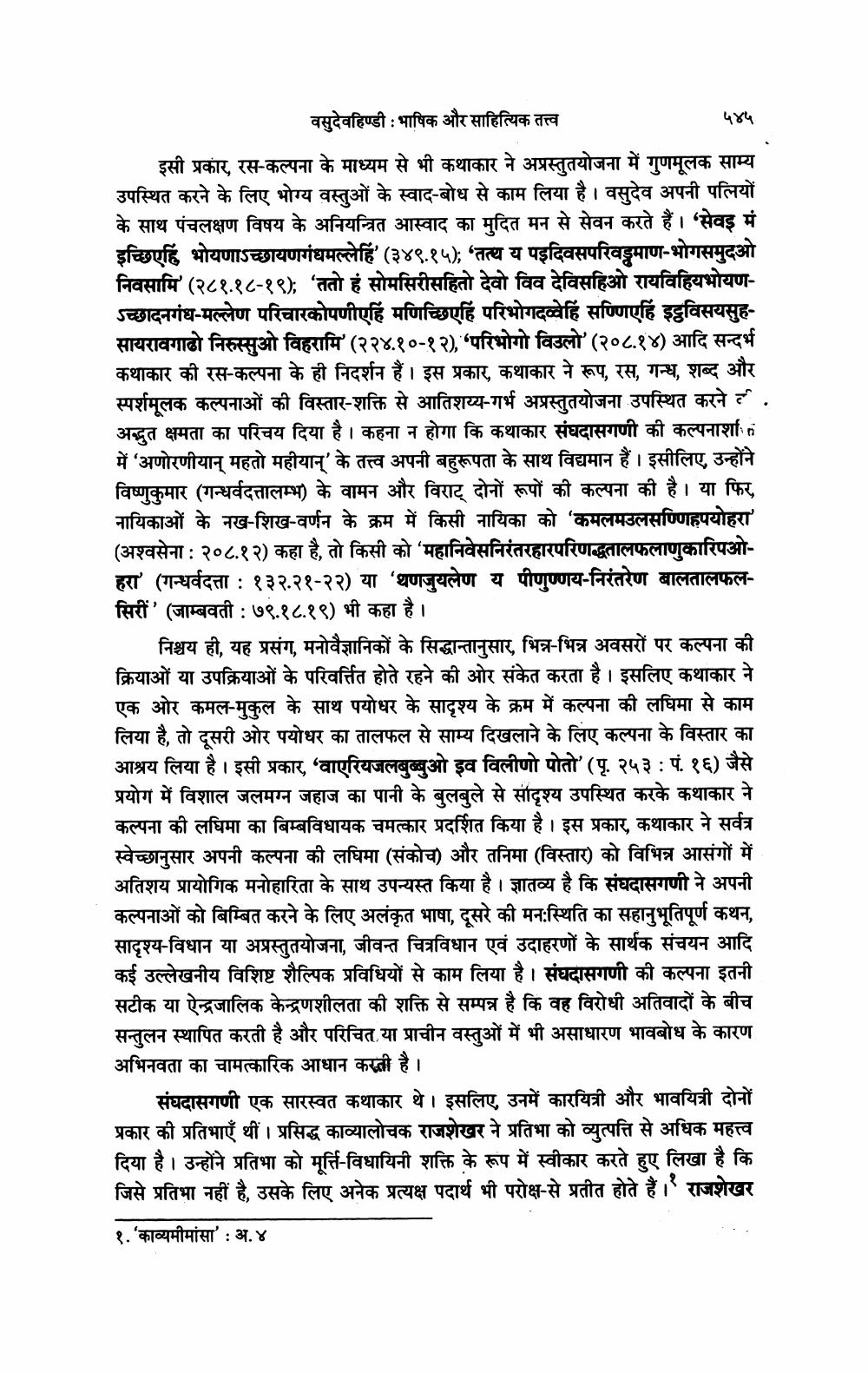________________
वसुदेवहिण्डी : भाषिक और साहित्यिक तत्त्व
५४५
इसी प्रकार, रस-कल्पना के माध्यम से भी कथाकार ने अप्रस्तुतयोजना में गुणमूलक साम्य उपस्थित करने के लिए भोग्य वस्तुओं के स्वाद - बोध से काम लिया है। वसुदेव अपनी पत्नियों के साथ पंचलक्षण विषय के अनियन्त्रित आस्वाद का मुदित मन से सेवन करते हैं । ' सेवइ मं इच्छिएहिं भोयणाऽच्छायणगंधमल्लेहिं' (३४९.१५); 'तत्य य पइदिवसपरिवड्डूमाण-भोगसमुदओ निवसामि' (२८१.१८-१९ ) ' ततो हं सोमसिरीसहितो देवो विव देविसहिओ रायविहियभोयणउच्छादनगंध मल्लेण परिचारकोपणीएहिं मणिच्छिएहिं परिभोगदव्वेहिं सपिणएहिं इट्ठविसयसुहसायरावगाढो निरुस्सुओ विहरामि (२२४.१० -१२), 'परिभोगो विउलो' (२०८.१४) आदि सन्दर्भ कथाकार की रस-कल्पना के ही निदर्शन हैं । इस प्रकार, कथाकार ने रूप, रस, गन्ध, शब्द और स्पर्शमूलक कल्पनाओं की विस्तार - शक्ति से आतिशय्य - गर्भ अप्रस्तुतयोजना उपस्थित करने अद्भुत क्षमता का परिचय दिया है। कहना न होगा कि कथाकार संघदासगणी की कल्पनाश में 'अणोरणीयान् महतो महीयान्' के तत्त्व अपनी बहुरूपता के साथ विद्यमान हैं। इसीलिए उन्होंने विष्णुकुमार (गन्धर्वदत्तालम्भ) के वामन और विराट् दोनों रूपों की कल्पना की है। या फिर, नायिकाओं के नख-शिख-वर्णन के क्रम में किसी नायिका को 'कमलमउलसण्णिहपयोहरा' (अश्वसेना : २०८.१२) कहा है, तो किसी को 'महानिवेसनिरंतरहारपरिणद्धतालफलाणुकारिपओहरा' (गन्धर्वदत्ता : १३२.२१ - २२) या 'थणजुयलेण य पीणुण्णय-निरंतरेण बालतालफलसिरीं' (जाम्बवती : ७९.१८.१९) भी कहा है ।
निश्चय ही, यह प्रसंग, मनोवैज्ञानिकों के सिद्धान्तानुसार, भिन्न-भिन्न अवसरों पर कल्पना की क्रियाओं या उपक्रियाओं के परिवर्तित होते रहने की ओर संकेत करता है । इसलिए कथाकार ने एक ओर कमल-मुकुल के साथ पयोधर के सादृश्य के क्रम में कल्पना की लघिमा से काम लिया है, तो दूसरी ओर पयोधर का तालफल से साम्य दिखलाने के लिए कल्पना के विस्तार का आश्रय लिया है। इसी प्रकार, 'वाएरियजलबुब्बुओ इव विलीणो पोतो' (पृ. २५३ : पं. १६) जैसे प्रयोग में विशाल जलमग्न जहाज का पानी के बुलबुले से सादृश्य उपस्थित करके कथाकार ने कल्पना की लघिमा का बिम्बविधायक चमत्कार प्रदर्शित किया है। इस प्रकार, कथाकार ने सर्वत्र स्वेच्छानुसार अपनी कल्पना की लघिमा (संकोच) और तनिमा (विस्तार) को विभिन्न आसंगों में अतिशय प्रायोगिक मनोहारिता के साथ उपन्यस्त किया है। ज्ञातव्य है कि संघदासगणी ने अपनी कल्पनाओं को बिम्बित करने के लिए अलंकृत भाषा, दूसरे की मन:स्थिति का सहानुभूतिपूर्ण कथन, सादृश्य-विधान या अप्रस्तुतयोजना, जीवन्त चित्रविधान एवं उदाहरणों के सार्थक संचयन आदि कई उल्लेखनीय विशिष्ट शैल्पिक प्रविधियों से काम लिया है। संघदासगणी की कल्पना इतनी सटीक या ऐन्द्रजालिक केन्द्रणशीलता की शक्ति से सम्पन्न है कि वह विरोधी अतिवादों के बीच सन्तुलन स्थापित करती है और परिचित या प्राचीन वस्तुओं में भी असाधारण भावबोध के कारण अभिनवता का चामत्कारिक आधान करती है ।
संघदासगणी एक सारस्वत कथाकार थे। इसलिए, उनमें कारयित्री और भावयित्री दोनों प्रकार की प्रतिभाएँ थीं । प्रसिद्ध काव्यालोचक राजशेखर ने प्रतिभा को व्युत्पत्ति से अधिक महत्त्व दिया है। उन्होंने प्रतिभा को मूर्ति - विधायिनी शक्ति के रूप में स्वीकार करते हुए लिखा है कि जिसे प्रतिभा नहीं है, उसके लिए अनेक प्रत्यक्ष पदार्थ भी परोक्ष से प्रतीत होते हैं। राजशेखर
१. 'काव्यमीमांसा' : अ. ४