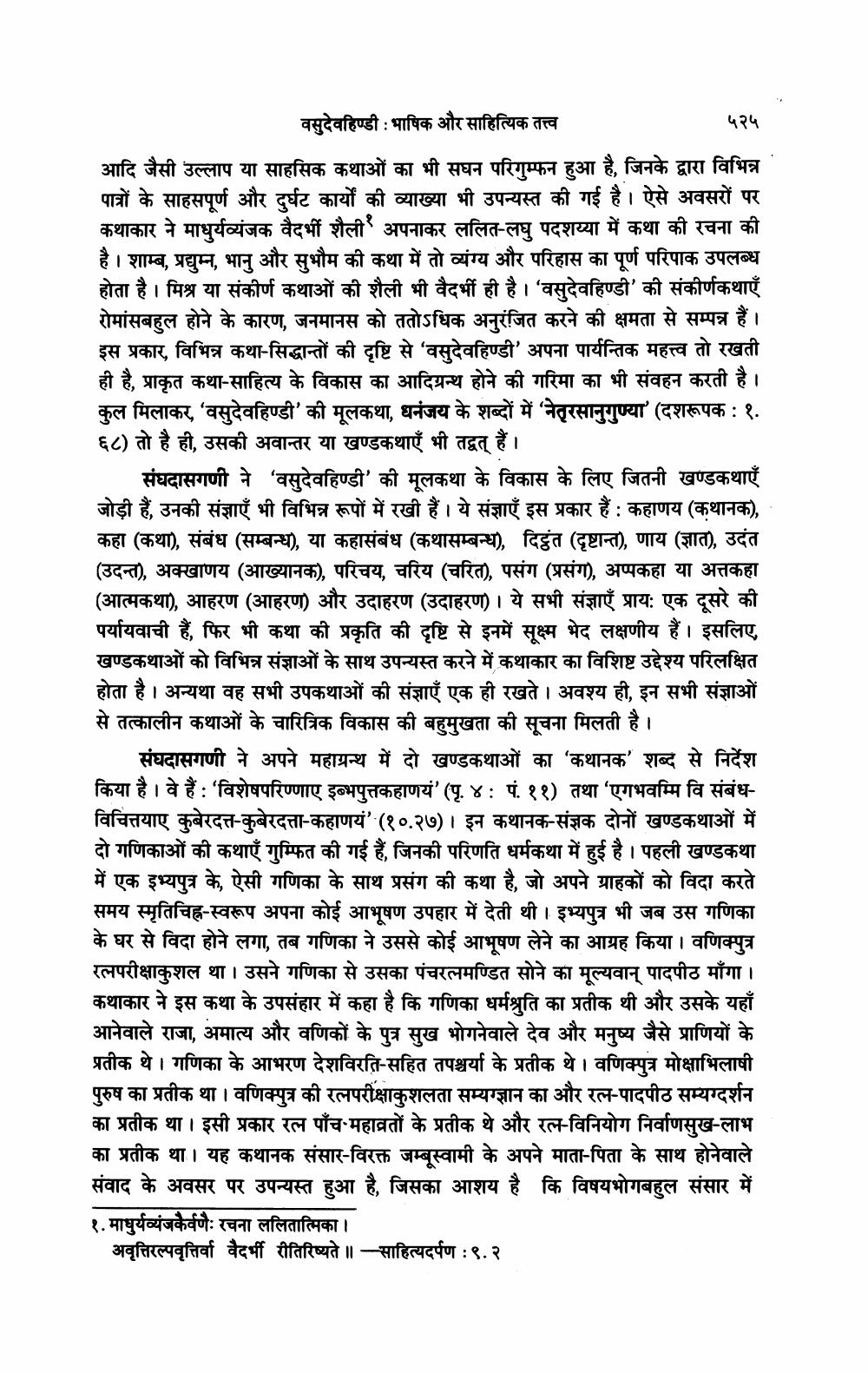________________
वसुदेवहिण्डी : भाषिक और साहित्यिक तत्त्व
५२५ आदि जैसी उल्लाप या साहसिक कथाओं का भी सघन परिगुम्फन हुआ है, जिनके द्वारा विभिन्न पात्रों के साहसपूर्ण और दुर्घट कार्यों की व्याख्या भी उपन्यस्त की गई है। ऐसे अवसरों पर कथाकार ने माधुर्यव्यंजक वैदर्भी शैली अपनाकर ललित-लघु पदशय्या में कथा की रचना की है। शाम्ब, प्रद्युम्न, भानु और सुभौम की कथा में तो व्यंग्य और परिहास का पूर्ण परिपाक उपलब्ध होता है। मिश्र या संकीर्ण कथाओं की शैली भी वैदर्भी ही है। 'वसुदेवहिण्डी' की संकीर्णकथाएँ रोमांसबहुल होने के कारण, जनमानस को ततोऽधिक अनुरंजित करने की क्षमता से सम्पन्न हैं। इस प्रकार, विभिन्न कथा-सिद्धान्तों की दृष्टि से 'वसुदेवहिण्डी' अपना पार्यन्तिक महत्त्व तो रखती ही है, प्राकृत कथा-साहित्य के विकास का आदिग्रन्थ होने की गरिमा का भी संवहन करती है। कुल मिलाकर, 'वसुदेवहिण्डी' की मूलकथा, धनंजय के शब्दों में 'नेतृरसानुगुण्या' (दशरूपक : १. ६८) तो है ही, उसकी अवान्तर या खण्डकथाएँ भी तद्वत् हैं।
संघदासगणी ने 'वसदेवहिण्डी' की मलकथा के विकास के लिए जितनी खण्डकथाएँ जोड़ी हैं, उनकी संज्ञाएँ भी विभिन्न रूपों में रखी हैं। ये संज्ञाएँ इस प्रकार हैं : कहाणय (कथानक), कहा (कथा), संबंध (सम्बन्ध), या कहासंबंध (कथासम्बन्ध), दिटुंत (दृष्टान्त), णाय (ज्ञात), उदंत (उदन्त), अक्खाणय (आख्यानक), परिचय, चरिय (चरित), पसंग (प्रसंग), अप्पकहा या अत्तकहा (आत्मकथा), आहरण (आहरण) और उदाहरण (उदाहरण)। ये सभी संज्ञाएँ प्राय: एक दूसरे की पर्यायवाची हैं, फिर भी कथा की प्रकृति की दृष्टि से इनमें सूक्ष्म भेद लक्षणीय हैं। इसलिए, खण्डकथाओं को विभिन्न संज्ञाओं के साथ उपन्यस्त करने में कथाकार का विशिष्ट उद्देश्य परिलक्षित होता है। अन्यथा वह सभी उपकथाओं की संज्ञाएँ एक ही रखते। अवश्य ही, इन सभी संज्ञाओं से तत्कालीन कथाओं के चारित्रिक विकास की बहुमुखता की सूचना मिलती है।
संघदासगणी ने अपने महाग्रन्थ में दो खण्डकथाओं का ‘कथानक' शब्द से निर्देश किया है। वे हैं : 'विशेषपरिण्णाए इब्भपुत्तकहाणयं' (पृ. ४ : पं. ११) तथा 'एगभवम्मि वि संबंधविचित्तयाए कुबेरदत्त-कुबेरदत्ता-कहाणयं' (१०.२७)। इन कथानक-संज्ञक दोनों खण्डकथाओं में दो गणिकाओं की कथाएँ गुम्फित की गई हैं, जिनकी परिणति धर्मकथा में हुई है। पहली खण्डकथा में एक इभ्यपुत्र के, ऐसी गणिका के साथ प्रसंग की कथा है, जो अपने ग्राहकों को विदा करते समय स्मृतिचिह्न-स्वरूप अपना कोई आभूषण उपहार में देती थी। इभ्यपुत्र भी जब उस गणिका के घर से विदा होने लगा, तब गणिका ने उससे कोई आभूषण लेने का आग्रह किया। वणिक्पुत्र रत्नपरीक्षाकुशल था। उसने गणिका से उसका पंचरत्नमण्डित सोने का मूल्यवान् पादपीठ माँगा। कथाकार ने इस कथा के उपसंहार में कहा है कि गणिका धर्मश्रुति का प्रतीक थी और उसके यहाँ आनेवाले राजा, अमात्य और वणिकों के पुत्र सुख भोगनेवाले देव और मनुष्य जैसे प्राणियों के प्रतीक थे। गणिका के आभरण देशविरति-सहित तपश्चर्या के प्रतीक थे। वणिक्पुत्र मोक्षाभिलाषी पुरुष का प्रतीक था। वणिक्पुत्र की रत्नपरीक्षाकुशलता सम्यग्ज्ञान का और रल-पादपीठ सम्यग्दर्शन का प्रतीक था। इसी प्रकार रत्न पाँच महाव्रतों के प्रतीक थे और रत्ल-विनियोग निर्वाणसुख-लाभ का प्रतीक था। यह कथानक संसार-विरक्त जम्बूस्वामी के अपने माता-पिता के साथ होनेवाले संवाद के अवसर पर उपन्यस्त हुआ है, जिसका आशय है कि विषयभोगबहुल संसार में १. माधुर्यव्यंजकैर्वणैः रचना ललितात्मिका।
अवृत्तिरल्पवत्तिर्वा वैदर्भी रीतिरिष्यते ॥-साहित्यदर्पण :९.२