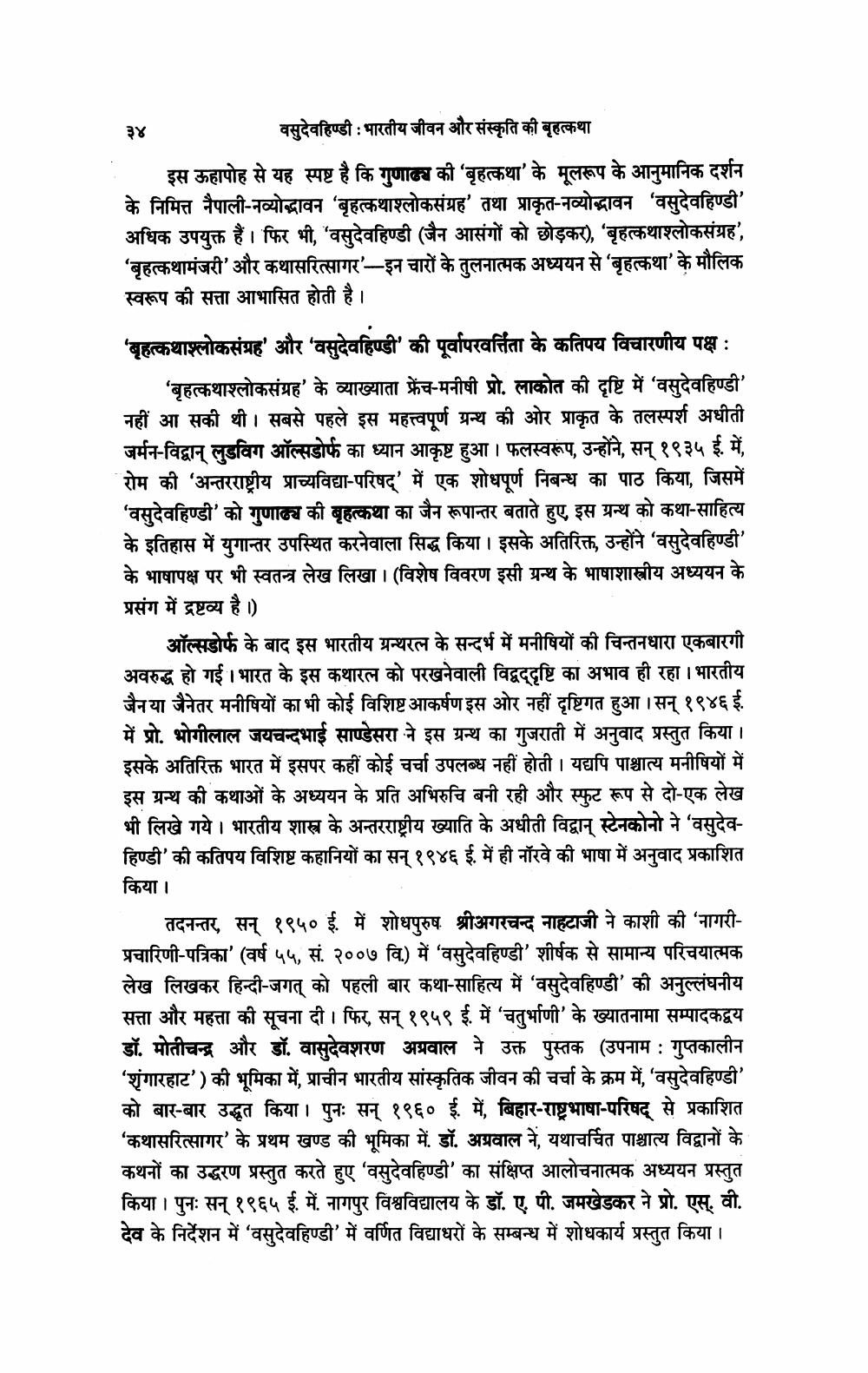________________
३४
वसुदेवहिण्डी : भारतीय जीवन और संस्कृति की बृहत्कथा ___ इस ऊहापोह से यह स्पष्ट है कि गुणान्य की 'बृहत्कथा' के मूलरूप के आनुमानिक दर्शन के निमित्त नैपाली-नव्योद्भावन 'बृहत्कथाश्लोकसंग्रह' तथा प्राकृत-नव्योद्भावन 'वसुदेवहिण्डी' अधिक उपयुक्त हैं। फिर भी, 'वसुदेवहिण्डी (जैन आसंगों को छोड़कर), 'बृहत्कथाश्लोकसंग्रह', 'बृहत्कथामंजरी' और कथासरित्सागर'-इन चारों के तुलनात्मक अध्ययन से 'बृहत्कथा' के मौलिक स्वरूप की सत्ता आभासित होती है। 'बृहत्कथाश्लोकसंग्रह' और 'वसुदेवहिण्डी' की पूर्वापरवर्त्तिता के कतिपय विचारणीय पक्ष :
'बृहत्कथाश्लोकसंग्रह' के व्याख्याता फ्रेंच-मनीषी प्रो. लाकोत की दृष्टि में 'वसुदेवहिण्डी' नहीं आ सकी थी। सबसे पहले इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ की ओर प्राकृत के तलस्पर्श अधीती जर्मन-विद्वान् लुडविग ऑल्सडोर्फ का ध्यान आकृष्ट हुआ। फलस्वरूप, उन्होंने, सन् १९३५ ई. में, रोम की 'अन्तरराष्ट्रीय प्राच्यविद्या-परिषद्' में एक शोधपूर्ण निबन्ध का पाठ किया, जिसमें 'वसुदेवहिण्डी' को गुणाढ्य की बृहत्कथा का जैन रूपान्तर बताते हुए, इस ग्रन्थ को कथा-साहित्य के इतिहास में युगान्तर उपस्थित करनेवाला सिद्ध किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने 'वसुदेवहिण्डी' के भाषापक्ष पर भी स्वतन्त्र लेख लिखा । (विशेष विवरण इसी ग्रन्थ के भाषाशास्त्रीय अध्ययन के प्रसंग में द्रष्टव्य है।) ___ ऑल्सडोर्फ के बाद इस भारतीय ग्रन्थरत्न के सन्दर्भ में मनीषियों की चिन्तनधारा एकबारगी अवरुद्ध हो गई । भारत के इस कथारन को परखनेवाली विद्वदृष्टि का अभाव ही रहा । भारतीय जैन या जैनेतर मनीषियों का भी कोई विशिष्ट आकर्षण इस ओर नहीं दृष्टिगत हुआ। सन् १९४६ ई. में प्रो. भोगीलाल जयचन्दभाई साण्डेसरा ने इस ग्रन्थ का गुजराती में अनुवाद प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त भारत में इसपर कहीं कोई चर्चा उपलब्ध नहीं होती । यद्यपि पाश्चात्य मनीषियों में इस ग्रन्थ की कथाओं के अध्ययन के प्रति अभिरुचि बनी रही और स्फुट रूप से दो-एक लेख भी लिखे गये। भारतीय शास्त्र के अन्तरराष्ट्रीय ख्याति के अधीती विद्वान् स्टेनकोनो ने 'वसुदेवहिण्डी' की कतिपय विशिष्ट कहानियों का सन् १९४६ ई. में ही नॉरवे की भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया।
तदनन्तर, सन् १९५० ई. में शोधपुरुष श्रीअगरचन्द नाहटाजी ने काशी की 'नागरीप्रचारिणी-पत्रिका' (वर्ष ५५, सं. २००७ वि) में 'वसुदेवहिण्डी' शीर्षक से सामान्य परिचयात्मक लेख लिखकर हिन्दी-जगत् को पहली बार कथा-साहित्य में 'वसुदेवहिण्डी' की अनुल्लंघनीय सत्ता और महत्ता की सूचना दी। फिर, सन् १९५९ ई. में 'चतुर्भाणी' के ख्यातनामा सम्पादकद्वय डॉ. मोतीचन्द्र और डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल ने उक्त पुस्तक (उपनाम : गुप्तकालीन 'शृंगारहाट') की भूमिका में, प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक जीवन की चर्चा के क्रम में, 'वसुदेवहिण्डी' को बार-बार उद्धृत किया। पुनः सन् १९६० ई. में, बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् से प्रकाशित 'कथासरित्सागर' के प्रथम खण्ड की भूमिका में. डॉ. अग्रवाल ने, यथाचर्चित पाश्चात्य विद्वानों के कथनों का उद्धरण प्रस्तुत करते हुए 'वसुदेवहिण्डी' का संक्षिप्त आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। पुनः सन् १९६५ ई. में. नागपुर विश्वविद्यालय के डॉ. ए. पी. जमखेडकर ने प्रो. एस्. वी. देव के निर्देशन में 'वसुदेवहिण्डी' में वर्णित विद्याधरों के सम्बन्ध में शोधकार्य प्रस्तुत किया।