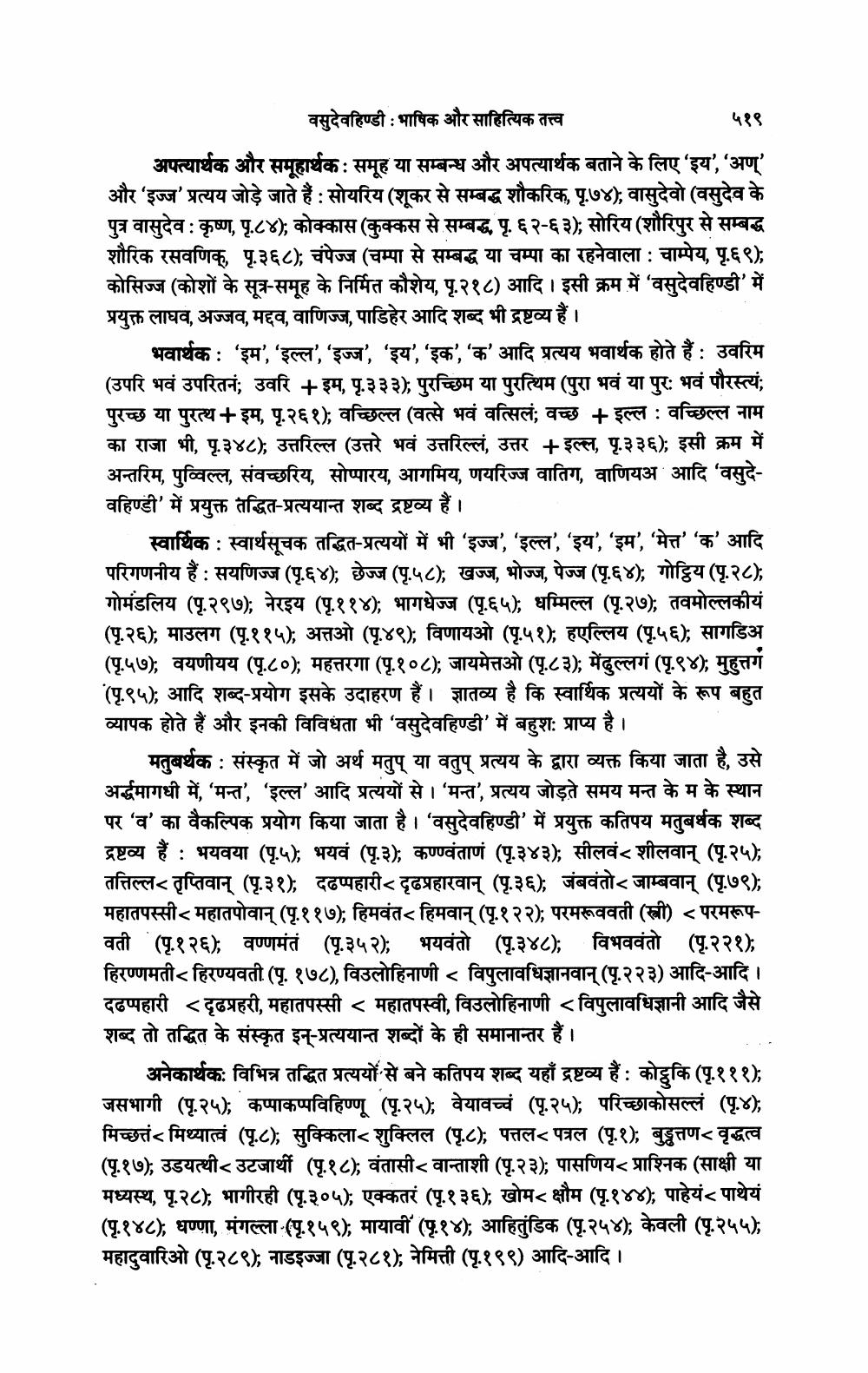________________
वसुदेवहिण्डी : भाषिक और साहित्यिक तत्त्व
५१९
अपत्यार्थक और समूहार्थक : समूह या सम्बन्ध और अपत्यार्थक बताने के लिए 'इय’, ‘अण्’ और ‘इज्ज' प्रत्यय जोड़े जाते हैं : सोयरिय (शूकर से सम्बद्ध शौकरिक, पृ.७४), वासुदेवो (वसुदेव के पुत्र वासुदेव : कृष्ण, पृ. ८४); कोक्कास (कुक्कस से सम्बद्ध, पृ. ६२-६३); सोरिय (शौरिपुर से सम्बद्ध शौरिक रसवणिक्, पृ. ३६८), चंपेज्ज (चम्पा से सम्बद्ध या चम्पा का रहनेवाला : चाम्पेय, पृ.६९); कोसिज्ज (कोशों के सूत्र - समूह के निर्मित कौशेय, पृ. २१८) आदि । इसी क्रम में 'वसुदेवहिण्डी' में प्रयुक्त लाघव, अज्जव, मद्दव, वाणिज्ज, पाडिहेर आदि शब्द भी द्रष्टव्य हैं ।
भवार्थक : 'इम', 'इल्ल', 'इज्ज', 'इय', 'इक', 'क' आदि प्रत्यय भवार्थक होते हैं : उवरिम (उपरि भवं उपरितनं; उवरि + इम, पृ. ३३३), पुरच्छिम या पुरत्थिम (पुरा भवं या पुरः भवं पौरस्त्यं; पुरच्छ या पुरत्थ + इम, पृ. २६१), वच्छिल्ल (वत्से भवं वत्सिलं; वच्छ + इल्ल : वच्छिल्ल नाम का राजा भी, पृ.३४८); उत्तरिल्ल (उत्तरे भवं उत्तरिल्लं, उत्तर + इल्ल, पृ. ३३६); इसी क्रम में अन्तरिम, पुव्विल्ल, संवच्छरिय, सोप्पारय, आगमिय, णयरिज्ज वातिग, वाणियअ आदि 'वसुदेवहिण्डी' में प्रयुक्त तद्धित-प्रत्ययान्त शब्द द्रष्टव्य हैं।
स्वार्थिक: स्वार्थसूचक तद्धित - प्रत्ययों में भी 'इज्ज', 'इल्ल', 'इय', 'इम', 'मेत्त' 'क' आदि परिगणनीय हैं : सयणिज्ज (पृ.६४); छेज्ज (पृ.५८); खज्ज, भोज्ज, पेज्ज (पृ.६४); गोट्ठिय (पृ.२८); गोमंडलिय (पृ.२९७); नेरइय (पृ. ११४); भागधेज्ज (पृ.६५); धम्मिल्ल (पृ.२७); तवमोल्लकीयं (पृ.२६), माउलग (पृ.११५ ); अत्तओ (पृ.४९); विणायओ (पृ. ५१ ); हएल्लिय (पृ. ५६), सागडिअ (पृ.५७); वयणीयय (पृ.८०); महत्तरगा (पृ. १०८); जायमेत्तओ (पृ. ८३); में दुल्लगं (पृ. ९४); मुहुत्तगं (पृ.९५); आदि शब्द-प्रयोग इसके उदाहरण हैं । ज्ञातव्य है कि स्वार्थिक प्रत्ययों के रूप बहुत व्यापक होते हैं और इनकी विविधता भी 'वसुदेवहिण्डी' में बहुशः प्राप्य है ।
मतुबर्थक : संस्कृत में जो अर्थ मतुप् या वतुप् प्रत्यय के द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसे अर्द्धमागधी में, 'मन्त', 'इल्ल' आदि प्रत्ययों से । 'मन्त' प्रत्यय जोड़ते समय मन्त के म के स्थान पर 'व' का वैकल्पिक प्रयोग किया जाता है । 'वसुदेवहिण्डी' में प्रयुक्त कतिपय मतुबर्थक शब्द द्रष्टव्य हैं : भयवया (पृ.५), भयवं (पृ.३); कण्ण्वंताणं (पृ. ३४३); सीलवं < शीलवान् (पृ.२५); तत्तिल्ल< तृप्तिवान् (पृ.३१); दढप्पहारी < दृढप्रहारवान् (पृ.३६); जंबवंतो < जाम्बवान् (पृ.७९); महातपस्सी< महातपोवान् (पृ.११७); हिमवंत < हिमवान् (पृ.१२२); परमरूववती (स्त्री) < परमरूपवती (पृ.१२६), वण्णमंतं (पृ.३५२); भयवंतो (पृ.३४८); विभववंतो (पृ.२२१); हिरण्णमती < हिरण्यवती (पृ. १७८), विउलोहिनाणी - विपुलावधिज्ञानवान् (पृ.२२३) आदि-आदि । दढप्पहारी < दृढप्रहरी, महातपस्सी < महातपस्वी, विउलोहिनाणी < विपुलावधिज्ञानी आदि जैसे शब्द तो तद्धित के संस्कृत इन्- प्रत्ययान्त शब्दों के ही समानान्तर हैं ।
<
अनेकार्थकः विभिन्न तद्धित प्रत्ययों से बने कतिपय शब्द यहाँ द्रष्टव्य हैं : कोट्टुकि (पृ. १११); जसभागी (पृ.२५); कप्पाकप्पविहिण्णू (पृ.२५), वेयावच्चं (पृ. २५); परिच्छाकोसल्लं (पृ.४); मिच्छत्तं - मिथ्यात्वं (पृ. ८), सुक्किला- शुक्लिल (पृ. ८); पत्तल < पत्रल (पृ. १); बुडुत्तण- वृद्धत्व (पृ.१७); उडयत्थी< उटजार्थी (पृ.१८), वंतासी < वान्ताशी (पृ. २३); पासणिय< प्राश्निक (साक्षी या मध्यस्थ, पृ. २८), भागीरही (पृ. ३०५), एक्कतरं (पृ. १३६), खोम - क्षौम (पृ. १४४), पाहेयं < पाथेयं (पृ. १४८), धण्णा, मंगल्ला - (पृ. १५९), मायावी (पृ. १४), आहितुंडिक (पृ. २५४); केवली (पृ.२५५), महादुवारिओ (पृ. २८९); नाडइज्जा (पृ. २८१), नेमित्ती (पृ. १९९) आदि -आदि ।