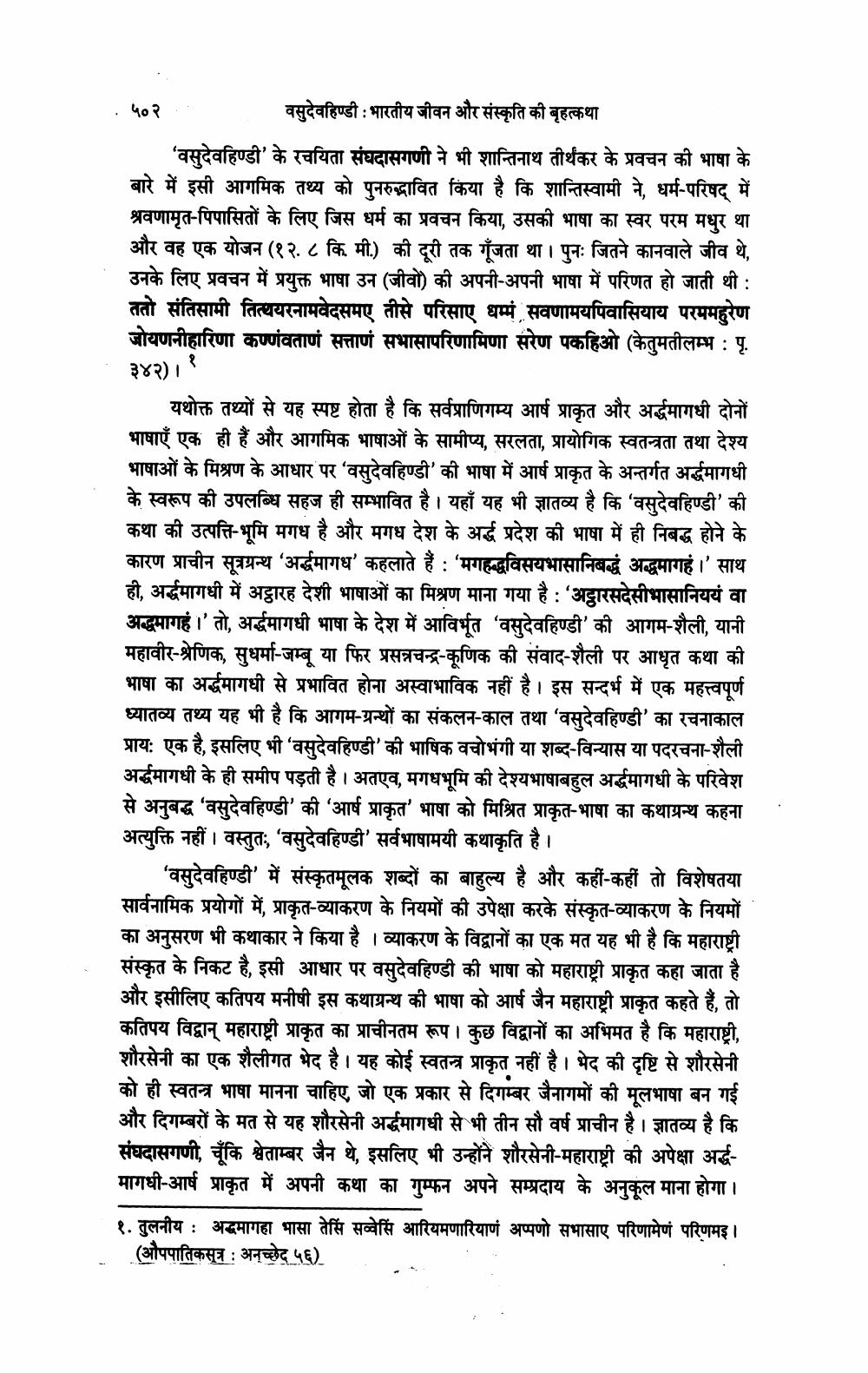________________
. ५०२ . वसुदेवहिण्डी : भारतीय जीवन और संस्कृति की बृहत्कथा
'वसुदेवहिण्डी' के रचयिता संघदासगणी ने भी शान्तिनाथ तीर्थंकर के प्रवचन की भाषा के बारे में इसी आगमिक तथ्य को पुनरुद्भावित किया है कि शान्तिस्वामी ने, धर्म-परिषद् में श्रवणामृत-पिपासितों के लिए जिस धर्म का प्रवचन किया, उसकी भाषा का स्वर परम मधुर था
और वह एक योजन (१२. ८ कि. मी.) की दूरी तक गूंजता था। पुनः जितने कानवाले जीव थे, उनके लिए प्रवचन में प्रयुक्त भाषा उन (जीवों) की अपनी-अपनी भाषा में परिणत हो जाती थी : ततो संतिसामी तित्थयरनामवेदसमए तीसे परिसाए धम्मं सवणामयपिवासियाय परममहुरेण जोयणनीहारिणा कण्णवताणं सत्ताणं सभासापरिणामिणा सरेण पकहिओ (केतमतीलम्भ : पृ.
३४२)। १
__यथोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि सर्वप्राणिगम्य आर्ष प्राकृत और अर्द्धमागधी दोनों भाषाएँ एक ही हैं और आगमिक भाषाओं के सामीप्य, सरलता, प्रायोगिक स्वतन्त्रता तथा देश्य भाषाओं के मिश्रण के आधार पर 'वसुदेवहिण्डी' की भाषा में आर्ष प्राकृत के अन्तर्गत अर्द्धमागधी के स्वरूप की उपलब्धि सहज ही सम्भावित है। यहाँ यह भी ज्ञातव्य है कि 'वसुदेवहिण्डी' की कथा की उत्पत्ति-भूमि मगध है और मगध देश के अर्द्ध प्रदेश की भाषा में ही निबद्ध होने के कारण प्राचीन सूत्रग्रन्थ 'अर्धमागध' कहलाते हैं : 'मगहद्धविसयभासानिबद्धं अद्धमागहं ।' साथ ही, अर्द्धमागधी में अट्ठारह देशी भाषाओं का मिश्रण माना गया है : अट्ठारसदेसीभासानिययं वा अद्धमागहं ।' तो, अर्धमागधी भाषा के देश में आविर्भूत 'वसुदेवहिण्डी' की आगम-शैली, यानी महावीर-श्रेणिक, सुधर्मा-जम्बू या फिर प्रसन्नचन्द्र-कूणिक की संवाद-शैली पर आधृत कथा की भाषा का अर्द्धमागधी से प्रभावित होना अस्वाभाविक नहीं है। इस सन्दर्भ में एक महत्त्वपूर्ण ध्यातव्य तथ्य यह भी है कि आगम-ग्रन्थों का संकलन-काल तथा 'वसुदेवहिण्डी' का रचनाकाल प्राय: एक है, इसलिए भी 'वसुदेवहिण्डी' की भाषिक वचोभंगी या शब्द-विन्यास या पदरचना-शैली अर्धमागधी के ही समीप पड़ती है। अतएव, मगधभूमि की देश्यभाषाबहुल अर्धमागधी के परिवेश से अनुबद्ध 'वसुदेवहिण्डी' की 'आर्ष प्राकृत' भाषा को मिश्रित प्राकृत-भाषा का कथाग्रन्थ कहना अत्युक्ति नहीं। वस्तुतः 'वसुदेवहिण्डी' सर्वभाषामयी कथाकृति है।
'वसुदेवहिण्डी' में संस्कृतमूलक शब्दों का बाहुल्य है और कहीं-कहीं तो विशेषतया सार्वनामिक प्रयोगों में, प्राकृत-व्याकरण के नियमों की उपेक्षा करके संस्कृत-व्याकरण के नियमों का अनुसरण भी कथाकार ने किया है । व्याकरण के विद्वानों का एक मत यह भी है कि महाराष्ट्री संस्कृत के निकट है, इसी आधार पर वसुदेवहिण्डी की भाषा को महाराष्ट्री प्राकृत कहा जाता है
और इसीलिए कतिपय मनीषी इस कथाग्रन्थ की भाषा को आर्ष जैन महाराष्ट्री प्राकृत कहते हैं, तो कतिपय विद्वान् महाराष्ट्री प्राकृत का प्राचीनतम रूप। कुछ विद्वानों का अभिमत है कि महाराष्ट्री, शौरसेनी का एक शैलीगत भेद है। यह कोई स्वतन्त्र प्राकृत नहीं है। भेद की दृष्टि से शौरसेनी को ही स्वतन्त्र भाषा मानना चाहिए, जो एक प्रकार से दिगम्बर जैनागमों की मूलभाषा बन गई और दिगम्बरों के मत से यह शौरसेनी अर्धमागधी से भी तीन सौ वर्ष प्राचीन है। ज्ञातव्य है कि संघदासगणी, चूँकि श्वेताम्बर जैन थे, इसलिए भी उन्होंने शौरसेनी-महाराष्ट्री की अपेक्षा अर्द्धमागधी-आर्ष प्राकृत में अपनी कथा का गुम्फन अपने सम्प्रदाय के अनुकूल माना होगा। १. तुलनीय : अदमागहा भासा तेसि सव्वेसिं आरियमणारियाणं अप्पणो सभासाए परिणामेणं परिणमइ । _ (औपपातिकसूत्र : अनुच्छेद ५६)