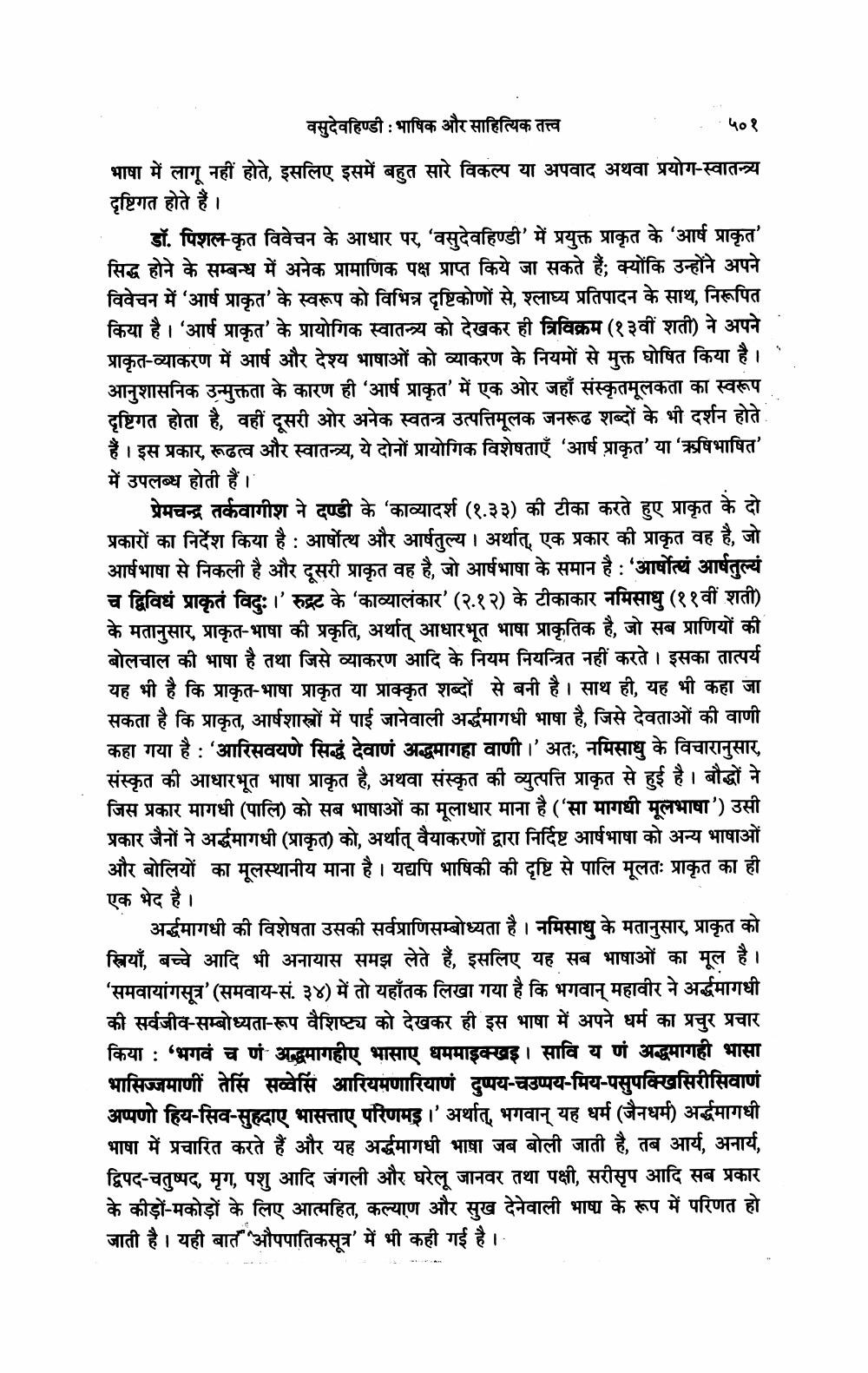________________
५०१
वसुदेवहिण्डी : भाषिक और साहित्यिक तत्त्व
५०१ भाषा में लागू नहीं होते, इसलिए इसमें बहुत सारे विकल्प या अपवाद अथवा प्रयोग-स्वातन्त्र्य दृष्टिगत होते हैं।
डॉ. पिशल-कृत विवेचन के आधार पर, 'वसुदेवहिण्डी' में प्रयुक्त प्राकृत के 'आर्ष प्राकृत' सिद्ध होने के सम्बन्ध में अनेक प्रामाणिक पक्ष प्राप्त किये जा सकते हैं; क्योंकि उन्होंने अपने विवेचन में 'आर्ष प्राकृत' के स्वरूप को विभिन्न दृष्टिकोणों से, श्लाघ्य प्रतिपादन के साथ, निरूपित किया है । 'आर्ष प्राकृत' के प्रायोगिक स्वातन्त्र्य को देखकर ही त्रिविक्रम (१३वीं शती) ने अपने प्राकृत-व्याकरण में आर्ष और देश्य भाषाओं को व्याकरण के नियमों से मुक्त घोषित किया है। " आनुशासनिक उन्मुक्तता के कारण ही 'आर्ष प्राकृत' में एक ओर जहाँ संस्कृतमूलकता का स्वरूप दृष्टिगत होता है, वहीं दूसरी ओर अनेक स्वतन्त्र उत्पत्तिमूलक जनरूढ शब्दों के भी दर्शन होते हैं । इस प्रकार, रूढत्व और स्वातन्त्र्य, ये दोनों प्रायोगिक विशेषताएँ 'आर्ष प्राकृत' या 'ऋषिभाषित' में उपलब्ध होती हैं।
प्रेमचन्द्र तर्कवागीश ने दण्डी के 'काव्यादर्श (१.३३) की टीका करते हुए प्राकृत के दो प्रकारों का निर्देश किया है : आर्षोत्थ और आर्षतुल्य । अर्थात्, एक प्रकार की प्राकृत वह है, जो आर्षभाषा से निकली है और दूसरी प्राकृत वह है, जो आर्षभाषा के समान है : 'आर्षोत्यं आर्षतुल्यं च द्विविधं प्राकृतं विदुः।' रुद्रट के 'काव्यालंकार' (२.१२) के टीकाकार नमिसाधु (११वीं शती) के मतानुसार, प्राकृत-भाषा की प्रकृति, अर्थात् आधारभूत भाषा प्राकृतिक है, जो सब प्राणियों की बोलचाल की भाषा है तथा जिसे व्याकरण आदि के नियम नियन्त्रित नहीं करते। इसका तात्पर्य यह भी है कि प्राकृत-भाषा प्राकृत या प्राक्कृत शब्दों से बनी है। साथ ही, यह भी कहा जा सकता है कि प्राकृत, आर्षशास्त्रों में पाई जानेवाली अर्द्धमागधी भाषा है, जिसे देवताओं की वाणी कहा गया है : 'आरिसवयणे सिद्धं देवाणं अद्धमागहा वाणी।' अतः नमिसाधु के विचारानुसार, संस्कृत की आधारभूत भाषा प्राकृत है, अथवा संस्कृत की व्युत्पत्ति प्राकृत से हुई है। बौद्धों ने जिस प्रकार मागधी (पालि) को सब भाषाओं का मूलाधार माना है ('सा मागधी मूलभाषा') उसी प्रकार जैनों ने अर्द्धमागधी (प्राकृत) को, अर्थात् वैयाकरणों द्वारा निर्दिष्ट आर्षभाषा को अन्य भाषाओं
और बोलियों का मूलस्थानीय माना है । यद्यपि भाषिकी की दृष्टि से पालि मूलतः प्राकृत का ही एक भेद है।
__ अर्द्धमागधी की विशेषता उसकी सर्वप्राणिसम्बोध्यता है । नमिसाधु के मतानुसार, प्राकृत को स्त्रियाँ, बच्चे आदि भी अनायास समझ लेते हैं, इसलिए यह सब भाषाओं का मूल है। 'समवायांगसूत्र' (समवाय-सं. ३४) में तो यहाँतक लिखा गया है कि भगवान् महावीर ने अर्द्धमागधी की सर्वजीव-सम्बोध्यता-रूप वैशिष्ट्य को देखकर ही इस भाषा में अपने धर्म का प्रचुर प्रचार किया : 'भगवं च णं अद्धमागहीए भासाए धममाइक्खइ। सावि य णं अद्धमागही भासा भासिज्जमाणी तेसिं सव्वेसिं आरियमणारियाणं दुष्पय-चउप्पय-मिय-पसुपक्खिसिरीसिवाणं अप्पणो हिय-सिव-सुहदाए भासत्ताए परिणमइ।' अर्थात्, भगवान् यह धर्म (जैनधर्म) अर्द्धमागधी भाषा में प्रचारित करते हैं और यह अर्द्धमागधी भाषा जब बोली जाती है, तब आर्य, अनार्य, द्विपद-चतुष्पद, मृग, पशु आदि जंगली और घरेलू जानवर तथा पक्षी, सरीसृप आदि सब प्रकार के कीड़ों-मकोड़ों के लिए आत्महित, कल्याण और सुख देनेवाली भाषा के रूप में परिणत हो जाती है। यही बात औपपातिकसूत्र' में भी कही गई है।