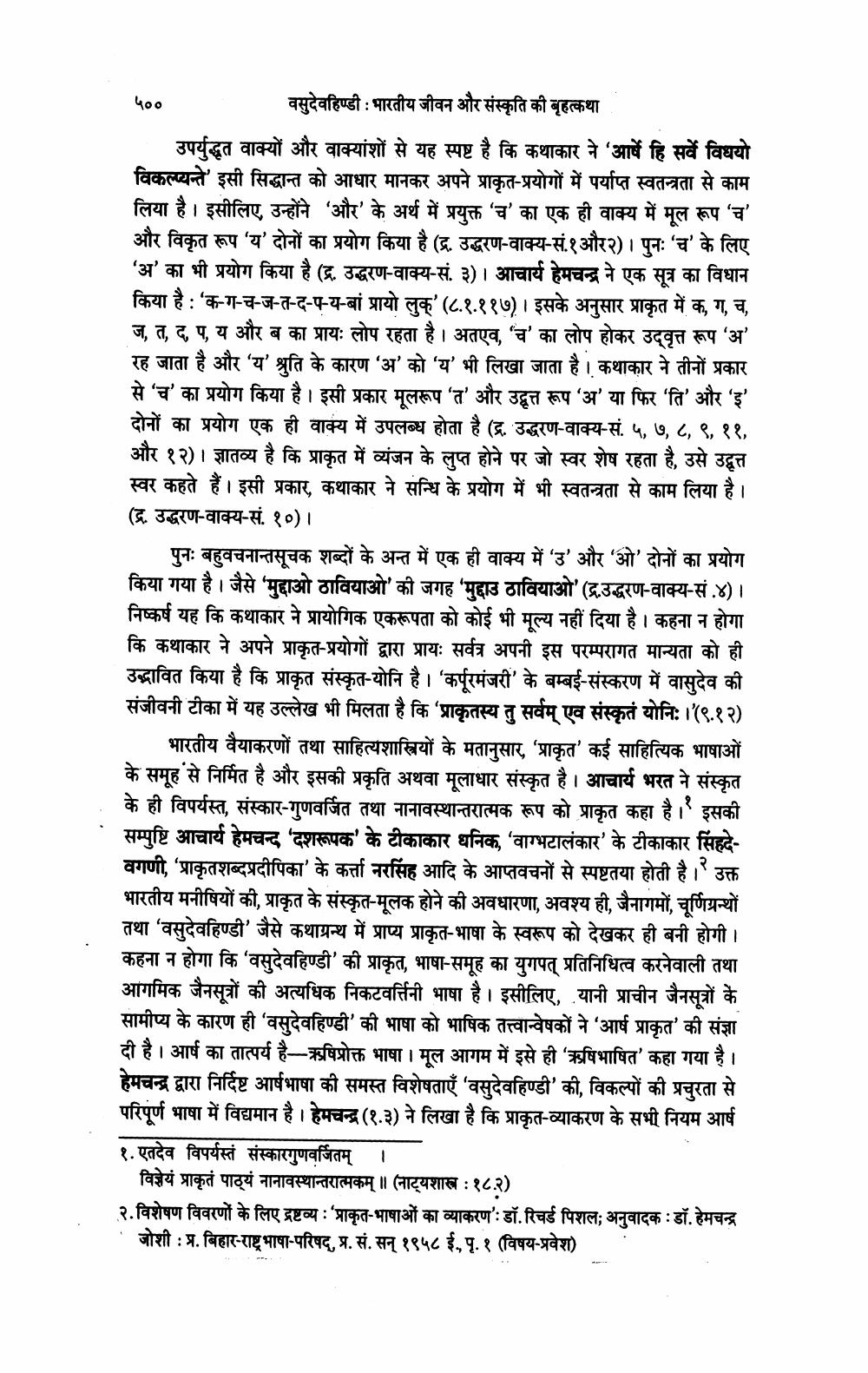________________
५०० __ वसुदेवहिण्डी : भारतीय जीवन और संस्कृति की बृहत्कथा
उपर्युद्धत वाक्यों और वाक्यांशों से यह स्पष्ट है कि कथाकार ने 'आर्षे हि सर्वे विधयो विकल्प्यन्ते' इसी सिद्धान्त को आधार मानकर अपने प्राकृत-प्रयोगों में पर्याप्त स्वतन्त्रता से काम लिया है। इसीलिए, उन्होंने 'और' के अर्थ में प्रयुक्त 'च' का एक ही वाक्य में मल रूप 'च'
और विकृत रूप 'य' दोनों का प्रयोग किया है (द्र. उद्धरण-वाक्य-सं.१और२) । पुनः 'च' के लिए 'अ' का भी प्रयोग किया है (द्र. उद्धरण-वाक्य-सं. ३)। आचार्य हेमचन्द्र ने एक सूत्र का विधान किया है : ‘क-ग-च-ज-त-द-प-य-बां प्रायो लुक्' (८.१.११७) । इसके अनुसार प्राकृत में क, ग, च, ज, त, द, प, य और ब का प्रायः लोप रहता है। अतएव, 'च' का लोप होकर उद्वृत्त रूप 'अ' रह जाता है और 'य' श्रुति के कारण 'अ' को 'य' भी लिखा जाता है। कथाकार ने तीनों प्रकार से 'च' का प्रयोग किया है। इसी प्रकार मलरूप 'त' और उदत्त रूप 'अ' या फिर 'ति' और 'इ' दोनों का प्रयोग एक ही वाक्य में उपलब्ध होता है (द्र. उद्धरण-वाक्य-सं. ५, ७, ८, ९, ११,
और १२)। ज्ञातव्य है कि प्राकृत में व्यंजन के लुप्त होने पर जो स्वर शेष रहता है, उसे उद्वृत्त स्वर कहते हैं। इसी प्रकार, कथाकार ने सन्धि के प्रयोग में भी स्वतन्त्रता से काम लिया है। (द्र. उद्धरण-वाक्य-सं. १०)।
पुनः बहुवचनान्तसूचक शब्दों के अन्त में एक ही वाक्य में 'उ' और 'ओ' दोनों का प्रयोग किया गया है। जैसे 'मुद्दाओ ठावियाओ' की जगह 'मुद्दाउ ठावियाओ' (द्र.उद्धरण-वाक्य-सं.४)। निष्कर्ष यह कि कथाकार ने प्रायोगिक एकरूपता को कोई भी मूल्य नहीं दिया है। कहना न होगा कि कथाकार ने अपने प्राकृत-प्रयोगों द्वारा प्रायः सर्वत्र अपनी इस परम्परागत मान्यता को ही उद्भावित किया है कि प्राकृत संस्कृत-योनि है। 'कर्पूरमंजरी' के बम्बई-संस्करण में वासुदेव की संजीवनी टीका में यह उल्लेख भी मिलता है कि 'प्राकृतस्य तु सर्वम् एव संस्कृतं योनिः । ९.१२)
भारतीय वैयाकरणों तथा साहित्यशास्त्रियों के मतानुसार, 'प्राकृत' कई साहित्यिक भाषाओं के समूह से निर्मित है और इसकी प्रकृति अथवा मूलाधार संस्कृत है। आचार्य भरत ने संस्कृत के ही विपर्यस्त, संस्कार-गुणवर्जित तथा नानावस्थान्तरात्मक रूप को प्राकृत कहा है। इसकी सम्पुष्टि आचार्य हेमचन्द 'दशरूपक' के टीकाकार धनिक, 'वाग्भटालंकार' के टीकाकार सिंहदेवगणी, ‘प्राकृतशब्दप्रदीपिका' के कर्ता नरसिंह आदि के आप्तवचनों से स्पष्टतया होती है। उक्त भारतीय मनीषियों की, प्राकृत के संस्कृत-मूलक होने की अवधारणा, अवश्य ही, जैनागमों, चूर्णिग्रन्थों तथा 'वसुदेवहिण्डी' जैसे कथाग्रन्थ में प्राप्य प्राकृत-भाषा के स्वरूप को देखकर ही बनी होगी। कहना न होगा कि 'वसुदेवहिण्डी' की प्राकृत, भाषा-समूह का युगपत् प्रतिनिधित्व करनेवाली तथा आगमिक जैनसूत्रों की अत्यधिक निकटवर्तिनी भाषा है। इसीलिए, यानी प्राचीन जैनसूत्रों के सामीप्य के कारण ही 'वसुदेवहिण्डी' की भाषा को भाषिक तत्त्वान्वेषकों ने 'आर्ष प्राकृत' की संज्ञा दी है। आर्ष का तात्पर्य है-ऋषिप्रोक्त भाषा । मूल आगम में इसे ही 'ऋषिभाषित' कहा गया है। हेमचन्द्र द्वारा निर्दिष्ट आर्षभाषा की समस्त विशेषताएँ 'वसुदेवहिण्डी' की, विकल्पों की प्रचुरता से परिपूर्ण भाषा में विद्यमान है। हेमचन्द्र (१.३) ने लिखा है कि प्राकृत-व्याकरण के सभी नियम आर्ष १. एतदेव विपर्यस्तं संस्कारगुणवर्जितम् ।
विज्ञेयं प्राकृतं पाठ्यं नानावस्थान्तरात्मकम् ॥ (नाट्यशास्त्र : १८.२) २.विशेषण विवरणों के लिए द्रष्टव्य : 'प्राकृत-भाषाओं का व्याकरण':डॉ.रिचर्ड पिशल; अनुवादक : डॉ. हेमचन्द्र
जोशी : प्र. बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्, प्र. सं. सन् १९५८ ई, पृ. १ (विषय-प्रवेश) ।