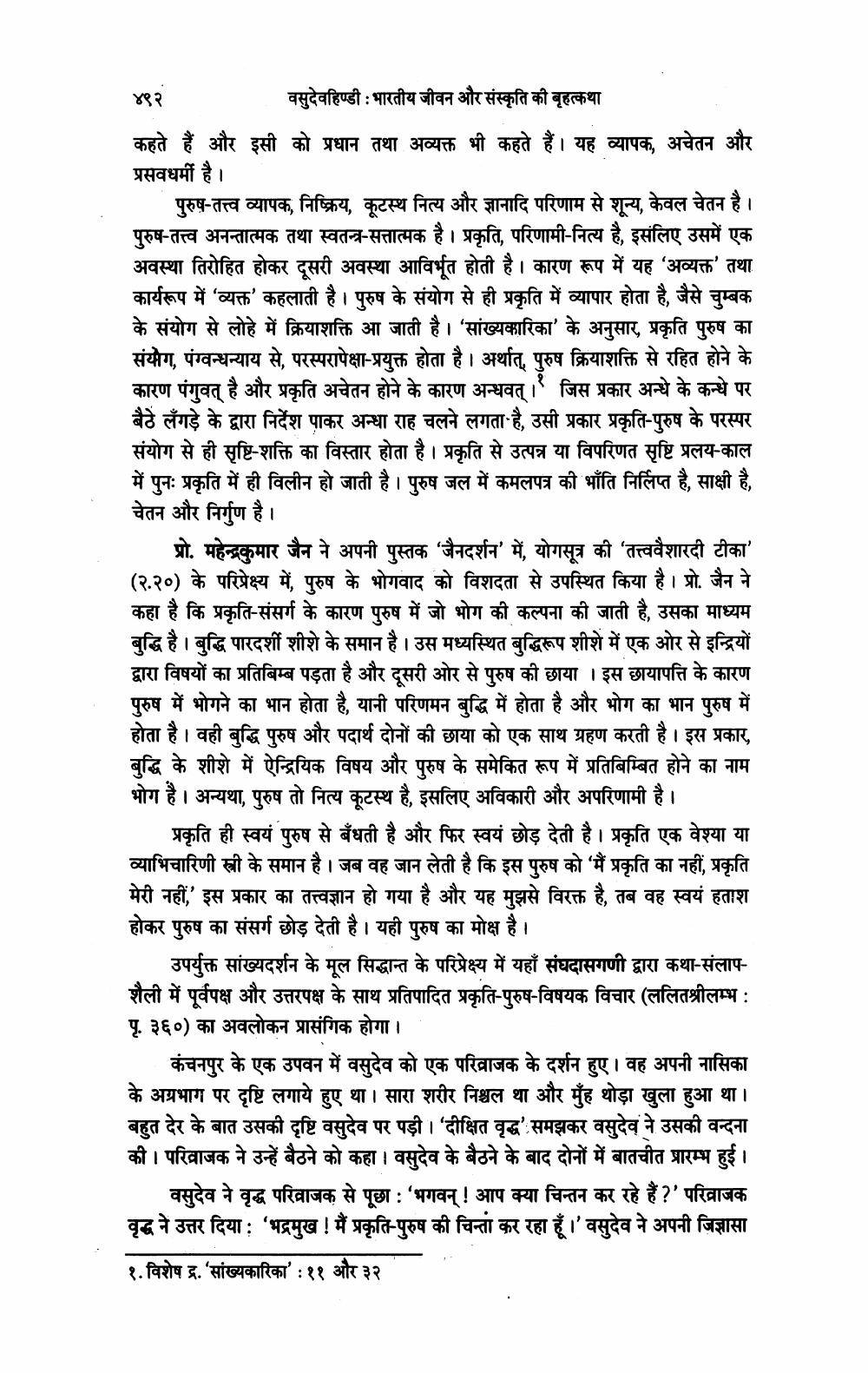________________
४९२
वसुदेवहिण्डी : भारतीय जीवन और संस्कृति की बृहत्कथा
कहते हैं और इसी को प्रधान तथा अव्यक्त भी कहते हैं । यह व्यापक, अचेतन और प्रसवधर्मी है।
पुरुष-तत्त्व व्यापक, निष्क्रिय, कूटस्थ नित्य और ज्ञानादि परिणाम से शून्य, केवल चेतन है । पुरुष-तत्त्व अनन्तात्मक तथा स्वतन्त्र - सत्तात्मक है । प्रकृति, परिणामी - नित्य है, इसलिए उसमें एक अवस्था तिरोहित होकर दूसरी अवस्था आविर्भूत होती है। कारण रूप में यह 'अव्यक्त' तथा कार्यरूप में ‘व्यक्त’ कहलाती है। पुरुष के संयोग से ही प्रकृति में व्यापार होता है, जैसे चुम्बक के संयोग से लोहे में क्रियाशक्ति आ जाती है । 'सांख्यकारिका' के अनुसार, प्रकृति पुरुष का संयोग, पंग्वन्धन्याय से, परस्परापेक्षा प्रयुक्त होता है । अर्थात्, पुरुष क्रियाशक्ति से रहित होने कारण पंगुवत् है और प्रकृति अचेतन होने के कारण अन्धवत् । ' जिस प्रकार अन्धे के कन्धे पर बैठे लँगड़े के द्वारा निर्देश पाकर अन्धा राह चलने लगता है, उसी प्रकार प्रकृति-पुरुष के परस्पर संयोग से ही सृष्टि शक्ति का विस्तार होता है । प्रकृति से उत्पन्न या विपरिणत सृष्टि प्रलय-काल पुनः प्रकृति में ही विलीन हो जाती है। पुरुष जल में कमलपत्र की भाँति निर्लिप्त है, साक्षी है, चेतन और निर्गुण है ।
प्रो. महेन्द्रकुमार जैन ने अपनी पुस्तक 'जैनदर्शन' में, योगसूत्र की 'तत्त्ववैशारदी टीका' (२.२० ) के परिप्रेक्ष्य में, पुरुष के भोगवाद को विशदता से उपस्थित किया है। प्रो. जैन ने कहा है कि प्रकृति-संसर्ग के कारण पुरुष में जो भोग की कल्पना की जाती है, उसका माध्य बुद्धि है। बुद्धि पारदर्शी शीशे के समान है। उस मध्यस्थित बुद्धिरूप शीशे में एक ओर से इन्द्रियों द्वारा विषयों का प्रतिबिम्ब पड़ता है और दूसरी ओर से पुरुष की छाया । इस छायापत्ति के कारण पुरुष में भोगने का भान होता है, यानी परिणमन बुद्धि में होता है और भोग का भान पुरुष होता है । वही बुद्धि पुरुष और पदार्थ दोनों की छाया को एक साथ ग्रहण करती है । इस प्रकार, बुद्धि के शीशे में ऐन्द्रियक विषय और पुरुष के समेकित रूप में प्रतिबिम्बित होने का नाम भोग है । अन्यथा, पुरुष तो नित्य कूटस्थ है, इसलिए अविकारी और अपरिणामी है।
प्रकृति ही स्वयं पुरुष से बँधती है और फिर स्वयं छोड़ देती है । प्रकृति एक वेश्या या व्याभिचारिणी स्त्री के समान है। जब वह जान लेती है कि इस पुरुष को 'मैं प्रकृति का नहीं, प्रकृति मेरी नहीं,' इस प्रकार का तत्त्वज्ञान हो गया है और यह मुझसे विरक्त है, तब वह स्वयं हताश होकर पुरुष का संसर्ग छोड़ देती है। यही पुरुष का मोक्ष है ।
उपर्युक्त सांख्यदर्शन के मूल सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में यहाँ संघदासगणी द्वारा कथा-संलापशैली में पूर्वपक्ष और उत्तरपक्ष के साथ प्रतिपादित प्रकृति-पुरुष-विषयक विचार (ललितश्रीलम्भ : पृ. ३६०) का अवलोकन प्रासंगिक होगा ।
कंचनपुर के एक उपवन में वसुदेव को एक परिव्राजक के दर्शन हुए। वह अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि लगाये हुए था। सारा शरीर निश्चल था और मुँह थोड़ा खुला हुआ था । बहुत देर के बात उसकी दृष्टि वसुदेव पर पड़ी। 'दीक्षित वृद्ध' समझकर वसुदेव ने उसकी वन्दना की । परिव्राजक ने उन्हें बैठने को कहा । वसुदेव के बैठने के बाद दोनों में बातचीत प्रारम्भ हुई।
वसुदेव ने वृद्ध परिव्राजक से पूछा : 'भगवन् ! आप क्या चिन्तन कर रहे हैं ?' परिव्राजक वृद्ध ने उत्तर दिया : 'भद्रमुख ! मैं प्रकृति-पुरुष की चिन्तां कर रहा हूँ।' वसुदेव ने अपनी जिज्ञासा १. विशेष द्र. 'सांख्यकारिका' : ११ और ३२