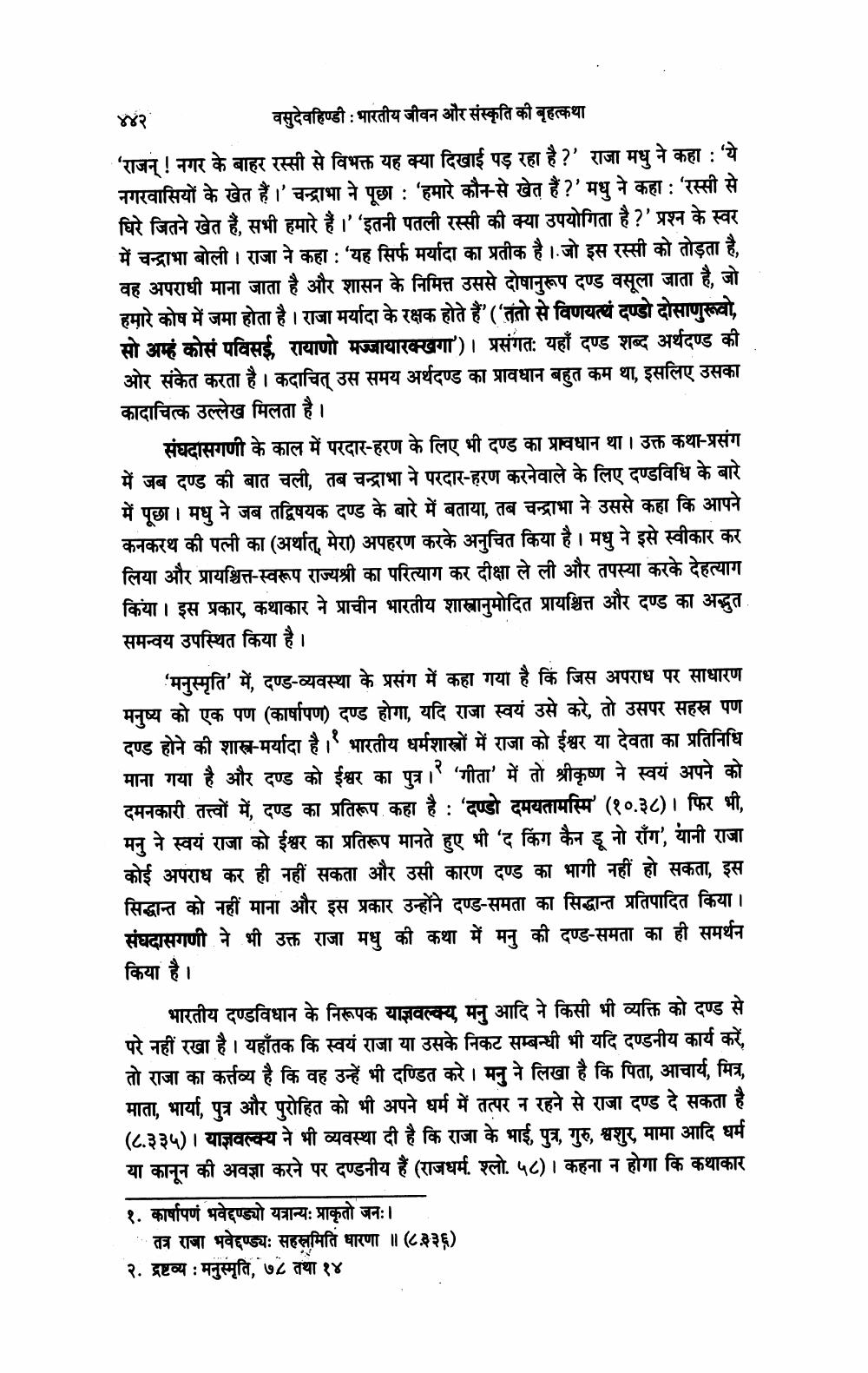________________
४४२
वसुदेवहिण्डी : भारतीय जीवन और संस्कृति की बृहत्कथा 'राजन् ! नगर के बाहर रस्सी से विभक्त यह क्या दिखाई पड़ रहा है?' राजा मधु ने कहा : 'ये नगरवासियों के खेत हैं।' चन्द्राभा ने पूछा : 'हमारे कौन-से खेत हैं?' मधु ने कहा : 'रस्सी से घिरे जितने खेत हैं, सभी हमारे हैं ।' 'इतनी पतली रस्सी की क्या उपयोगिता है ?' प्रश्न के स्वर में चन्द्राभा बोली। राजा ने कहा : 'यह सिर्फ मर्यादा का प्रतीक है। जो इस रस्सी को तोड़ता है, वह अपराधी माना जाता है और शासन के निमित्त उससे दोषानुरूप दण्ड वसूला जाता है, जो हमारे कोष में जमा होता है। राजा मर्यादा के रक्षक होते हैं' ('ततो से विणयत्यं दण्डो दोसाणुरूवो, सो अम्हं कोसं पविसई रायाणो मज्जायारक्खगा')। प्रसंगत: यहाँ दण्ड शब्द अर्थदण्ड की
ओर संकेत करता है। कदाचित् उस समय अर्थदण्ड का प्रावधान बहुत कम था, इसलिए उसका कादाचित्क उल्लेख मिलता है।
संघदासगणी के काल में परदार-हरण के लिए भी दण्ड का प्रावधान था। उक्त कथा-प्रसंग में जब दण्ड की बात चली, तब चन्द्राभा ने परदार-हरण करनेवाले के लिए दण्डविधि के बारे में पूछा। मधु ने जब तद्विषयक दण्ड के बारे में बताया, तब चन्द्राभा ने उससे कहा कि आपने कनकरथ की पत्नी का (अर्थात्, मेरा) अपहरण करके अनुचित किया है। मधु ने इसे स्वीकार कर लिया और प्रायश्चित्त-स्वरूप राज्यश्री का परित्याग कर दीक्षा ले ली और तपस्या करके देहत्याग किया। इस प्रकार, कथाकार ने प्राचीन भारतीय शास्त्रानुमोदित प्रायश्चित्त और दण्ड का अद्भुत समन्वय उपस्थित किया है।
'मनुस्मृति' में, दण्ड-व्यवस्था के प्रसंग में कहा गया है कि जिस अपराध पर साधारण मनुष्य को एक पण (कार्षापण) दण्ड होगा, यदि राजा स्वयं उसे करे, तो उसपर सहस्र पण दण्ड होने की शास्त्र-मर्यादा है। भारतीय धर्मशास्त्रों में राजा को ईश्वर या देवता का प्रतिनिधि माना गया है और दण्ड को ईश्वर का पुत्र ।२ 'गीता' में तो श्रीकृष्ण ने स्वयं अपने को दमनकारी तत्त्वों में, दण्ड का प्रतिरूप कहा है : 'दण्डो दमयतामस्मि' (१०.३८)। फिर भी, मनु ने स्वयं राजा को ईश्वर का प्रतिरूप मानते हुए भी 'द किंग कैन डू नो राँग', यानी राजा कोई अपराध कर ही नहीं सकता और उसी कारण दण्ड का भागी नहीं हो सकता, इस सिद्धान्त को नहीं माना और इस प्रकार उन्होंने दण्ड-समता का सिद्धान्त प्रतिपादित किया। संघदासगणी ने भी उक्त राजा मधु की कथा में मनु की दण्ड-समता का ही समर्थन किया है।
भारतीय दण्डविधान के निरूपक याज्ञवल्क्य मनु आदि ने किसी भी व्यक्ति को दण्ड से परे नहीं रखा है। यहाँतक कि स्वयं राजा या उसके निकट सम्बन्धी भी यदि दण्डनीय कार्य करें, तो राजा का कर्तव्य है कि वह उन्हें भी दण्डित करे । मनु ने लिखा है कि पिता, आचार्य, मित्र, माता, भार्या, पुत्र और पुरोहित को भी अपने धर्म में तत्पर न रहने से राजा दण्ड दे सकता है (८.३३५) । याज्ञवल्क्य ने भी व्यवस्था दी है कि राजा के भाई, पुत्र, गुरु, श्वशुर, मामा आदि धर्म या कानून की अवज्ञा करने पर दण्डनीय हैं (राजधर्म, श्लो. ५८)। कहना न होगा कि कथाकार १. कार्षापणं भवेद्दण्ड्यो यत्रान्यः प्राकृतो जनः।
तत्र राजा भवेद्दण्ड्यः सहस्रमिति धारणा ॥ (८.३३६) २. द्रष्टव्य : मनुस्मृति, ७८ तथा १४