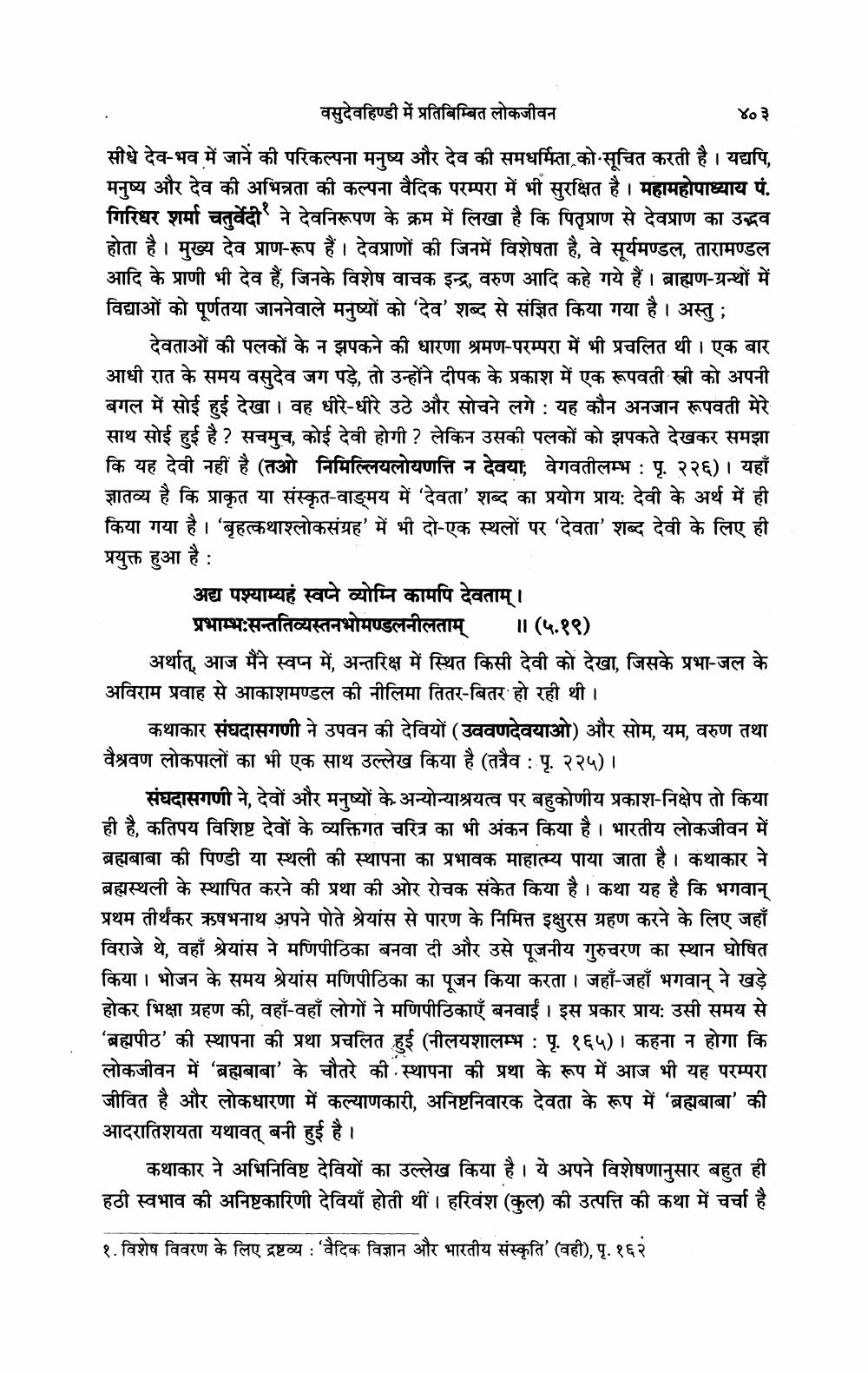________________
वसुदेवहिण्डी में प्रतिबिम्बित लोकजीवन
४०३ सीधे देव-भव में जाने की परिकल्पना मनुष्य और देव की समधर्मिता को सूचित करती है। यद्यपि, मनुष्य और देव की अभिन्नता की कल्पना वैदिक परम्परा में भी सुरक्षित है। महामहोपाध्याय पं. गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ने देवनिरूपण के क्रम में लिखा है कि पितृप्राण से देवप्राण का उद्भव होता है। मुख्य देव प्राण-रूप हैं। देवप्राणों की जिनमें विशेषता है, वे सूर्यमण्डल, तारामण्डल
आदि के प्राणी भी देव हैं, जिनके विशेष वाचक इन्द्र, वरुण आदि कहे गये हैं। ब्राह्मण-ग्रन्थों में विद्याओं को पूर्णतया जाननेवाले मनुष्यों को 'देव' शब्द से संज्ञित किया गया है। अस्तु ;
देवताओं की पलकों के न झपकने की धारणा श्रमण-परम्परा में भी प्रचलित थी। एक बार आधी रात के समय वसुदेव जग पड़े, तो उन्होंने दीपक के प्रकाश में एक रूपवती स्त्री को अपनी बगल में सोई हुई देखा। वह धीरे-धीरे उठे और सोचने लगे : यह कौन अनजान रूपवती मेरे साथ सोई हुई है? सचमुच, कोई देवी होगी? लेकिन उसकी पलकों को झपकते देखकर समझा कि यह देवी नहीं है (तओ निमिल्लियलोयणत्ति न देवया, वेगवतीलम्भ : पृ. २२६)। यहाँ ज्ञातव्य है कि प्राकृत या संस्कृत-वाङ्मय में 'देवता' शब्द का प्रयोग प्राय: देवी के अर्थ में ही किया गया है। 'बृहत्कथाश्लोकसंग्रह' में भी दो-एक स्थलों पर 'देवता' शब्द देवी के लिए ही प्रयुक्त हुआ है :
अद्य पश्याम्यहं स्वप्ने व्योम्नि कामपि देवताम्।
प्रभाम्भःसन्ततिव्यस्तनभोमण्डलनीलताम् ॥ (५.१९) अर्थात्, आज मैंने स्वप्न में, अन्तरिक्ष में स्थित किसी देवी को देखा, जिसके प्रभा-जल के अविराम प्रवाह से आकाशमण्डल की नीलिमा तितर-बितर हो रही थी। ___ कथाकार संघदासगणी ने उपवन की देवियों (उववणदेवयाओ) और सोम, यम, वरुण तथा वैश्रवण लोकपालों का भी एक साथ उल्लेख किया है (तत्रैव : पृ. २२५)।
संघदासगणी ने, देवों और मनुष्यों के अन्योन्याश्रयत्व पर बहुकोणीय प्रकाश-निक्षेप तो किया ही है, कतिपय विशिष्ट देवों के व्यक्तिगत चरित्र का भी अंकन किया है। भारतीय लोकजीवन में ब्रह्मबाबा की पिण्डी या स्थली की स्थापना का प्रभावक माहात्म्य पाया जाता है। कथाकार ने ब्रह्मस्थली के स्थापित करने की प्रथा की ओर रोचक संकेत किया है। कथा यह है कि भगवान् प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ अपने पोते श्रेयांस से पारण के निमित्त इक्षुरस ग्रहण करने के लिए जहाँ विराजे थे, वहाँ श्रेयांस ने मणिपीठिका बनवा दी और उसे पूजनीय गुरुचरण का स्थान घोषित किया। भोजन के समय श्रेयांस मणिपीठिका का पूजन किया करता । जहाँ-जहाँ भगवान् ने खड़े होकर भिक्षा ग्रहण की, वहाँ-वहाँ लोगों ने मणिपीठिकाएँ बनवाईं। इस प्रकार प्राय: उसी समय से 'ब्रह्मपीठ' की स्थापना की प्रथा प्रचलित हुई (नीलयशालम्भ : पृ. १६५)। कहना न होगा कि लोकजीवन में 'ब्रह्मबाबा' के चौतरे की स्थापना की प्रथा के रूप में आज भी यह परम्परा जीवित है और लोकधारणा में कल्याणकारी, अनिष्टनिवारक देवता के रूप में 'ब्रह्मबाबा' की आदरातिशयता यथावत बनी हई है।
कथाकार ने अभिनिविष्ट देवियों का उल्लेख किया है। ये अपने विशेषणानुसार बहुत ही हठी स्वभाव की अनिष्टकारिणी देवियाँ होती थीं। हरिवंश (कुल) की उत्पत्ति की कथा में चर्चा है
१. विशेष विवरण के लिए द्रष्टव्य : 'वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति' (वही), पृ. १६२