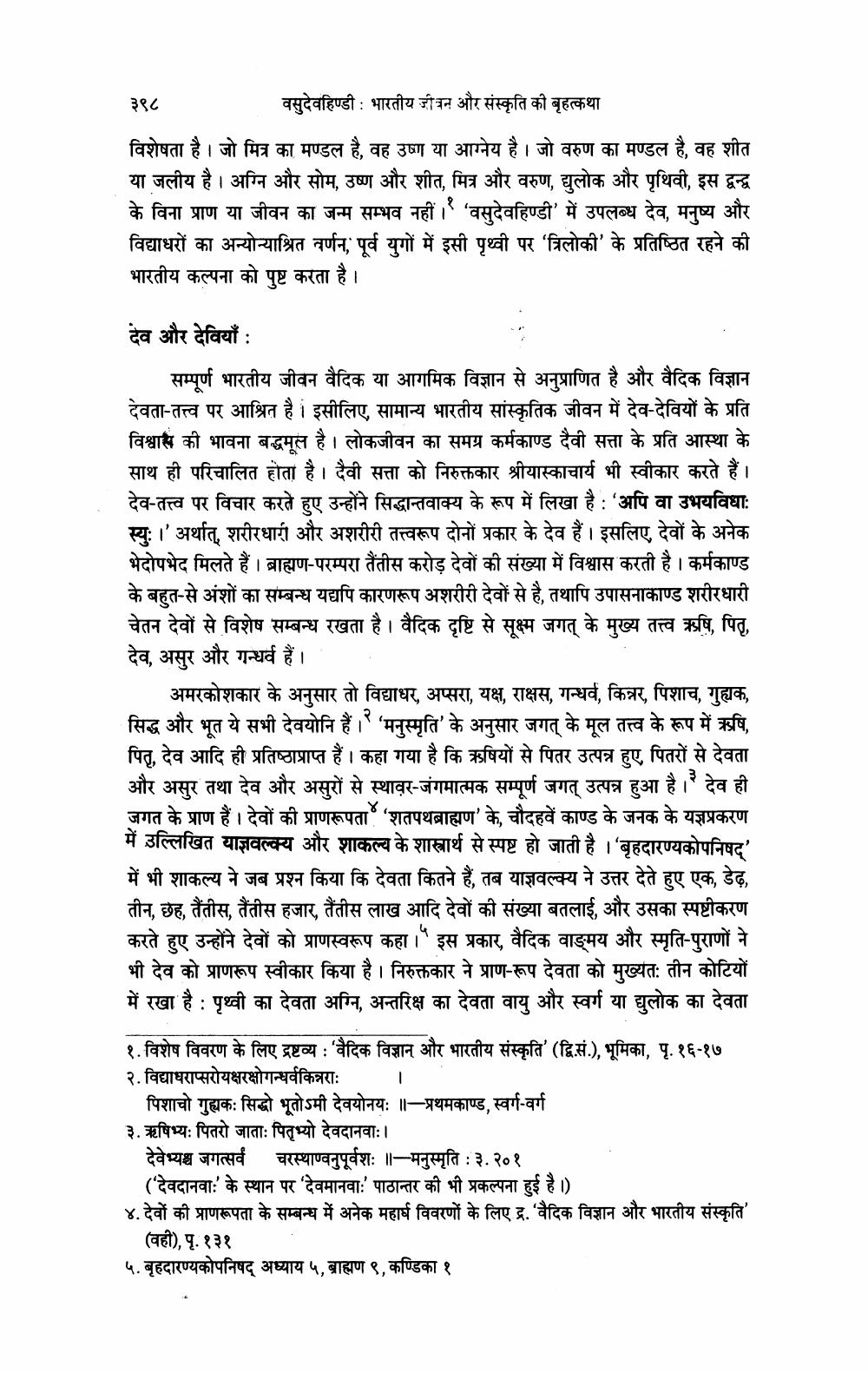________________
३९८
वसुदेवहिण्डी : भारतीय जीवन और संस्कृति की बृहत्कथा
विशेषता है। जो मित्र का मण्डल है, वह उष्ण या आग्नेय है। जो वरुण का मण्डल है, वह शीत या जलीय है । अग्नि और सोम, उष्ण और शीत, मित्र और वरुण, द्युलोक और पृथिवी, इस द्वन्द्व के विना प्राण या जीवन का जन्म सम्भव नहीं । ' 'वसुदेवहिण्डी' में उपलब्ध देव, मनुष्य और विद्याधरों का अन्योन्याश्रित वर्णन, पूर्व युगों में इसी पृथ्वी पर 'त्रिलोकी' के प्रतिष्ठित रहने की भारतीय कल्पना को पुष्ट करता है ।
देव और देवियाँ :
सम्पूर्ण भारतीय जीवन वैदिक या आगमिक विज्ञान से अनुप्राणित है और वैदिक विज्ञान देवता - तत्त्व पर आश्रित है । इसीलिए, सामान्य भारतीय सांस्कृतिक जीवन में देव - देवियों के प्रति विश्वास की भावना बद्धमूल है। लोकजीवन का समग्र कर्मकाण्ड दैवी सत्ता के प्रति आस्था के साथ ही परिचालित होता है। दैवी सत्ता को निरुक्तकार श्रीयास्काचार्य भी स्वीकार करते हैं । देव-तत्त्व पर विचार करते हुए उन्होंने सिद्धान्तवाक्य के रूप में लिखा है : 'अपि वा उभयविधा: स्युः ।' अर्थात्, शरीरधारी और अशरीरी तत्त्वरूप दोनों प्रकार के देव हैं। इसलिए, देवों के अनेक भेदोपभेद मिलते हैं । ब्राह्मण-परम्परा तैंतीस करोड़ देवों की संख्या में विश्वास करती है । कर्मकाण्ड के बहुत-से अंशों का सम्बन्ध यद्यपि कारणरूप अशरीरी देवों से है, तथापि उपासनाकाण्ड शरीरधारी चेतन देवों से विशेष सम्बन्ध रखता है। वैदिक दृष्टि से सूक्ष्म जगत् के मुख्य तत्त्व ऋषि, पितृ, देव, असुर और गन्धर्व हैं ।
अमरकोशकार के अनुसार तो विद्याधर, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, गन्धर्व, किन्नर, पिशाच, गुह्यक, सिद्ध और भूत ये सभी देवयोनि हैं। 'मनुस्मृति' के अनुसार जगत् के मूल तत्त्व के रूप में ऋषि, पितृ, देव आदि ही प्रतिष्ठाप्राप्त हैं। कहा गया है कि ऋषियों से पितर उत्पन्न हुए, पितरों से देवता और असुर तथा देव और असुरों से स्थावर-जंगमात्मक सम्पूर्ण जगत् उत्पन्न हुआ है। देव ही जगत के प्राण हैं । देवों की प्राणरूपता 'शतपथब्राह्मण' के, चौदहवें काण्ड के जनक के यज्ञप्रकरण में उल्लिखित याज्ञवल्क्य और शाकल्य के शास्त्रार्थ से स्पष्ट हो जाती है । 'बृहदारण्यकोपनिषद्' में भी शाकल्य ने जब प्रश्न किया कि देवता कितने हैं, तब याज्ञवल्क्य ने उत्तर देते हुए एक, डेढ़, तीन, छह, तैंतीस, तैंतीस हजार, तैंतीस लाख आदि देवों की संख्या बतलाई, और उसका स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने देवों को प्राणस्वरूप कहा । " इस प्रकार, वैदिक वाङ्मय और स्मृति-पुराणों ने भी देव को प्राणरूप स्वीकार किया है । निरुक्तकार ने प्राण-रूप देवता को मुख्यत: तीन कोटियों में रखा है : पृथ्वी का देवता अग्नि, अन्तरिक्ष का देवता वायु और स्वर्ग या द्युलोक का देवता
१. विशेष विवरण के लिए द्रष्टव्य : 'वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति' (द्वि.सं.), भूमिका, पृ. १६-१७
२. विद्याधराप्सरोयक्षरक्षोगन्धर्वकिन्नराः
1
पिशाचो गुह्यकः सिद्धो भूतोऽमी देवयोनयः ॥ - प्रथमकाण्ड, स् ३. ऋषिभ्यः पितरो जाताः पितृभ्यो देवदानवाः ।
देवेभ्यश्च जगत्सर्वं चरस्थाण्वनुपूर्वशः ॥ - मनुस्मृति : ३. २०१
('देवदानवाः' के स्थान पर 'देवमानवा:' पाठान्तर की भी प्रकल्पना हुई है ।)
४. देवों की प्राणरूपता के सम्बन्ध में अनेक महार्ष विवरणों के लिए द्र. 'वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति'
(वही), पृ. १३१
५.
. बृहदारण्यकोपनिषद् अध्याय ५, ब्राह्मण ९, कण्डिका १
स्वर्ग-वर्ग