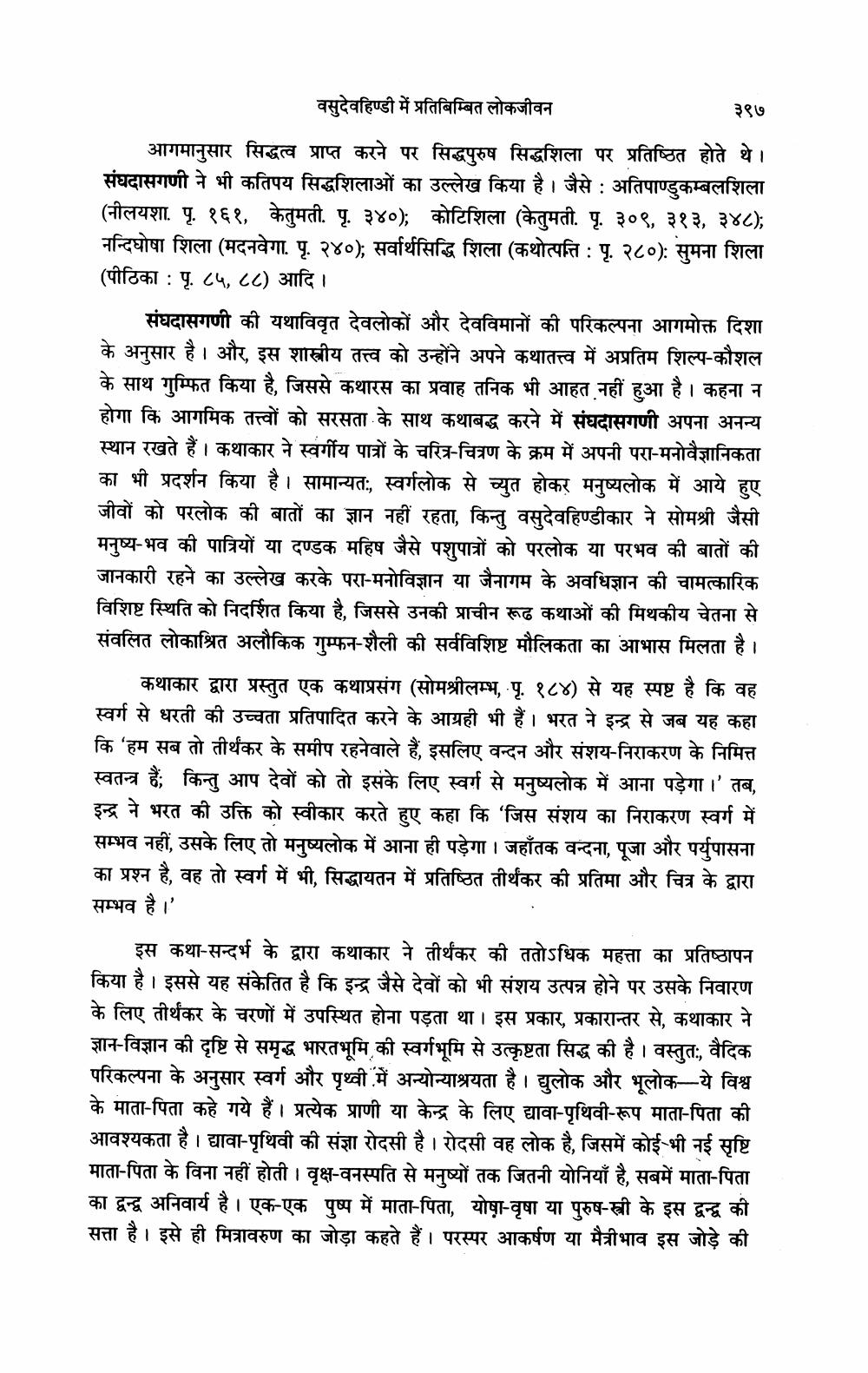________________
वसुदेवहिण्डी में प्रतिबिम्बित लोकजीवन
३९७ आगमानुसार सिद्धत्व प्राप्त करने पर सिद्धपुरुष सिद्धशिला पर प्रतिष्ठित होते थे। संघदासगणी ने भी कतिपय सिद्धशिलाओं का उल्लेख किया है। जैसे : अतिपाण्डुकम्बलशिला (नीलयशा. पृ. १६१, केतुमती. पृ. ३४०); कोटिशिला (केतुमती. पृ. ३०९, ३१३, ३४८), नन्दिघोषा शिला (मदनवेगा. पृ. २४०); सर्वार्थसिद्धि शिला (कथोत्पत्ति : पृ. २८०): सुमना शिला (पीठिका : पृ. ८५, ८८) आदि।
संघदासगणी की यथाविवृत देवलोकों और देवविमानों की परिकल्पना आगमोक्त दिशा के अनुसार है। और, इस शास्त्रीय तत्त्व को उन्होंने अपने कथातत्त्व में अप्रतिम शिल्प-कौशल के साथ गुम्फित किया है, जिससे कथारस का प्रवाह तनिक भी आहत नहीं हुआ है। कहना न होगा कि आगमिक तत्त्वों को सरसता के साथ कथाबद्ध करने में संघदासगणी अपना अनन्य स्थान रखते हैं। कथाकार ने स्वर्गीय पात्रों के चरित्र-चित्रण के क्रम में अपनी परा-मनोवैज्ञानिकता का भी प्रदर्शन किया है। सामान्यत:, स्वर्गलोक से च्युत होकर मनुष्यलोक में आये हुए जीवों को परलोक की बातों का ज्ञान नहीं रहता, किन्तु वसुदेवहिण्डीकार ने सोमश्री जैसी मनुष्य-भव की पात्रियों या दण्डक महिष जैसे पशुपात्रों को परलोक या परभव की बातों की जानकारी रहने का उल्लेख करके परा-मनोविज्ञान या जैनागम के अवधिज्ञान की चामत्कारिक विशिष्ट स्थिति को निदर्शित किया है, जिससे उनकी प्राचीन रूढ कथाओं की मिथकीय चेतना से संवलित लोकाश्रित अलौकिक गुम्फन-शैली की सर्वविशिष्ट मौलिकता का आभास मिलता है।
कथाकार द्वारा प्रस्तुत एक कथाप्रसंग (सोमश्रीलम्भ, पृ. १८४) से यह स्पष्ट है कि वह स्वर्ग से धरती की उच्चता प्रतिपादित करने के आग्रही भी हैं। भरत ने इन्द्र से जब यह कहा कि 'हम सब तो तीर्थंकर के समीप रहनेवाले हैं, इसलिए वन्दन और संशय-निराकरण के निमित्त स्वतन्त्र हैं; किन्तु आप देवों को तो इसके लिए स्वर्ग से मनुष्यलोक में आना पड़ेगा।' तब, इन्द्र ने भरत की उक्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि 'जिस संशय का निराकरण स्वर्ग में सम्भव नहीं, उसके लिए तो मनुष्यलोक में आना ही पड़ेगा । जहाँतक वन्दना, पूजा और पर्युपासना का प्रश्न है, वह तो स्वर्ग में भी, सिद्धायतन में प्रतिष्ठित तीर्थंकर की प्रतिमा और चित्र के द्वारा सम्भव है।'
इस कथा-सन्दर्भ के द्वारा कथाकार ने तीर्थंकर की ततोऽधिक महत्ता का प्रतिष्ठापन किया है। इससे यह संकेतित है कि इन्द्र जैसे देवों को भी संशय उत्पन्न होने पर उसके निवारण के लिए तीर्थंकर के चरणों में उपस्थित होना पड़ता था। इस प्रकार, प्रकारान्तर से, कथाकार ने ज्ञान-विज्ञान की दृष्टि से समृद्ध भारतभूमि की स्वर्गभूमि से उत्कृष्टता सिद्ध की है। वस्तुतः, वैदिक परिकल्पना के अनुसार स्वर्ग और पृथ्वी में अन्योन्याश्रयता है । धुलोक और भूलोक-ये विश्व के माता-पिता कहे गये हैं। प्रत्येक प्राणी या केन्द्र के लिए द्यावा-पृथिवी-रूप माता-पिता की आवश्यकता है। द्यावा-पृथिवी की संज्ञा रोदसी है । रोदसी वह लोक है, जिसमें कोई भी नई सृष्टि माता-पिता के विना नहीं होती। वृक्ष-वनस्पति से मनुष्यों तक जितनी योनियाँ है, सबमें माता-पिता का द्वन्द्व अनिवार्य है। एक-एक पुष्प में माता-पिता, योषा-वृषा या पुरुष-स्त्री के इस द्वन्द्व की सत्ता है। इसे ही मित्रावरुण का जोड़ा कहते हैं। परस्पर आकर्षण या मैत्रीभाव इस जोड़े की