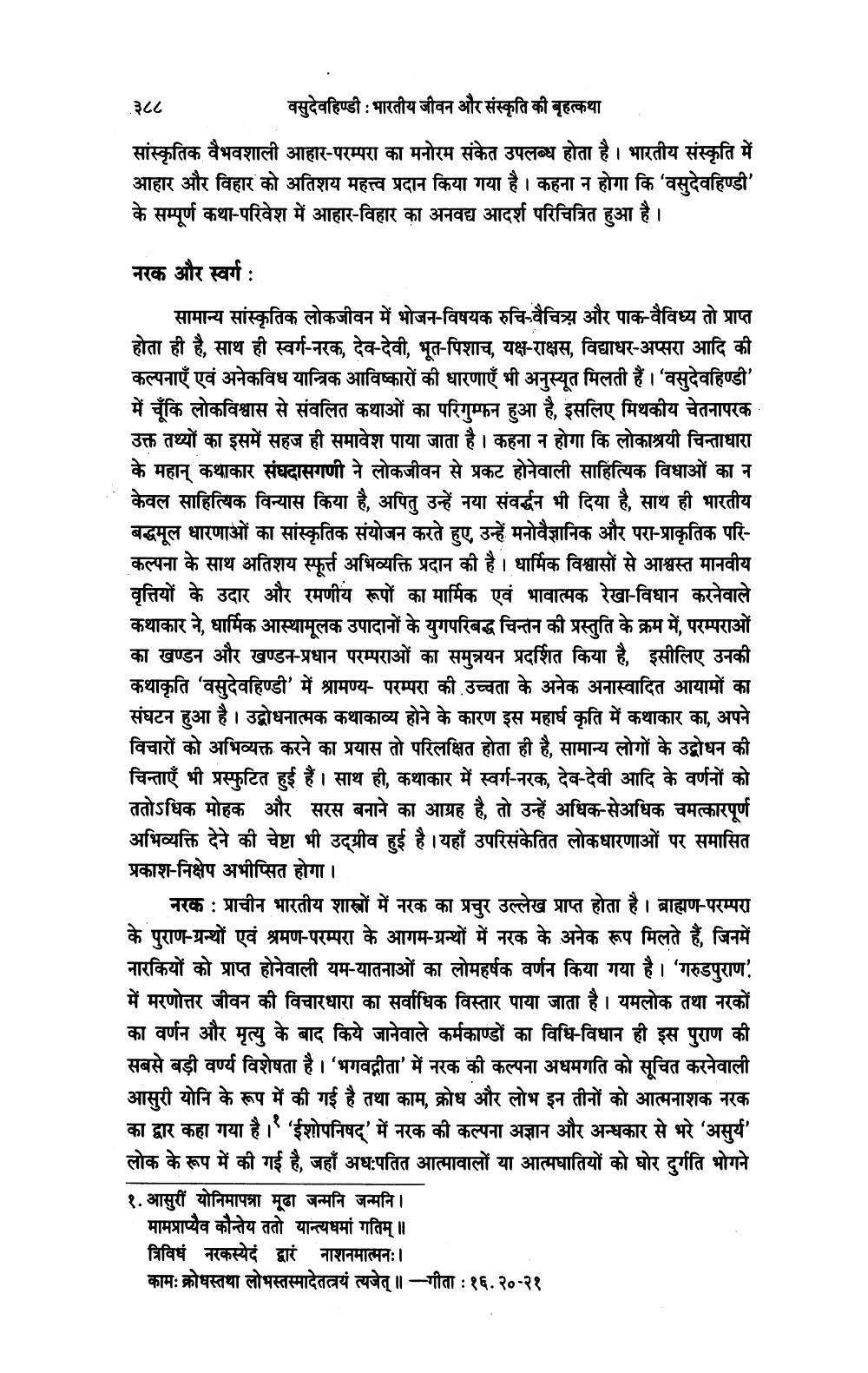________________
वसुदेवहिण्डी : भारतीय जीवन और संस्कृति की बृहत्कथा
सांस्कृतिक वैभवशाली आहार - परम्परा का मनोरम संकेत उपलब्ध होता है। भारतीय संस्कृति में आहार और विहार को अतिशय महत्त्व प्रदान किया गया है । कहना न होगा कि 'वसुदेवहिण्डी' के सम्पूर्ण कथा-परिवेश में आहार-विहार का अनवद्य आदर्श परिचित्रित हुआ है।
. ३८८
नरक और स्वर्ग :
सामान्य सांस्कृतिक लोकजीवन में भोजन-विषयक रुचि वैचित्र्य और पाक - वैविध्य तो प्राप्त होता ही है, साथ ही स्वर्ग-नरक, देव-देवी, भूत-पिशाच, यक्ष-राक्षस, विद्याधर - अप्सरा आदि की कल्पनाएँ एवं अनेकविध यान्त्रिक आविष्कारों की धारणाएँ भी अनुस्यूत मिलती हैं। 'वसुदेवहिण्डी' में चूँकि लोकविश्वास से संवलित कथाओं का परिगुम्फन हुआ है, इसलिए मिथकीय चेतनापरक - उक्त तथ्यों का इसमें सहज ही समावेश पाया जाता है । कहना न होगा कि लोकाश्रयी चिन्ताधारा के महान् कथाकार संघदासगणी ने लोकजीवन से प्रकट होनेवाली साहित्यिक विधाओं का न केवल साहित्यिक विन्यास किया है, अपितु उन्हें नया संवर्द्धन भी दिया है, साथ ही भारतीय बद्धमूल धारणाओं का सांस्कृतिक संयोजन करते हुए, उन्हें मनोवैज्ञानिक और परा- प्राकृतिक परिकल्पना के साथ अतिशय स्फूर्त अभिव्यक्ति प्रदान की है। धार्मिक विश्वासों से आश्वस्त मानवीय वृत्तियों के उदार और रमणीय रूपों का मार्मिक एवं भावात्मक रेखा -विधान करनेवाले कथाकार ने, धार्मिक आस्थामूलक उपादानों के युगपरिबद्ध चिन्तन की प्रस्तुति के क्रम में, परम्पराओं का खण्डन और खण्डन-प्रधान परम्पराओं का समुन्नयन प्रदर्शित किया है, इसीलिए उनकी कथाकृति 'वसुदेवहिण्डी' में श्रामण्य- परम्परा की उच्चता के अनेक अनास्वादित आयामों का संघटन हुआ है । उद्बोधनात्मक कथाकाव्य होने के कारण इस महार्घ कृति में कथाकार का, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का प्रयास तो परिलक्षित होता ही है, सामान्य लोगों के उद्बोधन की चिन्ताएँ भी प्रस्फुटित हुई हैं। साथ ही, कथाकार में स्वर्ग-नरक, देव-देवी आदि के वर्णनों को ततोऽधिक मोहक और सरस बनाने का आग्रह है, तो उन्हें अधिक से अधिक चमत्कारपूर्ण अभिव्यक्ति देने की चेष्टा भी उद्ग्रीव हुई है । यहाँ उपरिसंकेतित लोकधारणाओं पर समाति प्रकाश-निक्षेप अभीप्सित होगा ।
नरक : प्राचीन भारतीय शास्त्रों में नरक का प्रचुर उल्लेख प्राप्त होता है । ब्राह्मण - परम्परा के पुराण-ग्रन्थों एवं श्रमण-परम्परा के आगम-ग्रन्थों में नरक के अनेक रूप मिलते हैं, जिनमें नारकियों को प्राप्त होनेवाली यम यातनाओं का लोमहर्षक वर्णन किया गया है । 'गरुडपुराण' में मरणोत्तर जीवन की विचारधारा का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। यमलोक तथा नरकों का वर्णन और मृत्यु के बाद किये जानेवाले कर्मकाण्डों का विधि-विधान ही इस पुराण की सबसे बड़ी वर्ण्य विशेषता है। 'भगवद्गीता' में नरक की कल्पना अधमगति को सूचित करनेवाली आसुरी योनि के रूप में की गई है तथा काम, क्रोध और लोभ इन तीनों को आत्मनाशक नरक का द्वार कहा गया है।' 'ईशोपनिषद्' में नरक की कल्पना अज्ञान और अन्धकार से भरे 'असुर्य' लोक के रूप की गई है, जहाँ अध:पतित आत्मावालों या आत्मघातियों को घोर दुर्गति भोगने १. आसुरीं योनिमापत्रा मूढा जन्मनि जन्मनि ।
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् ॥
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ॥ - गीता : १६. २०-२१