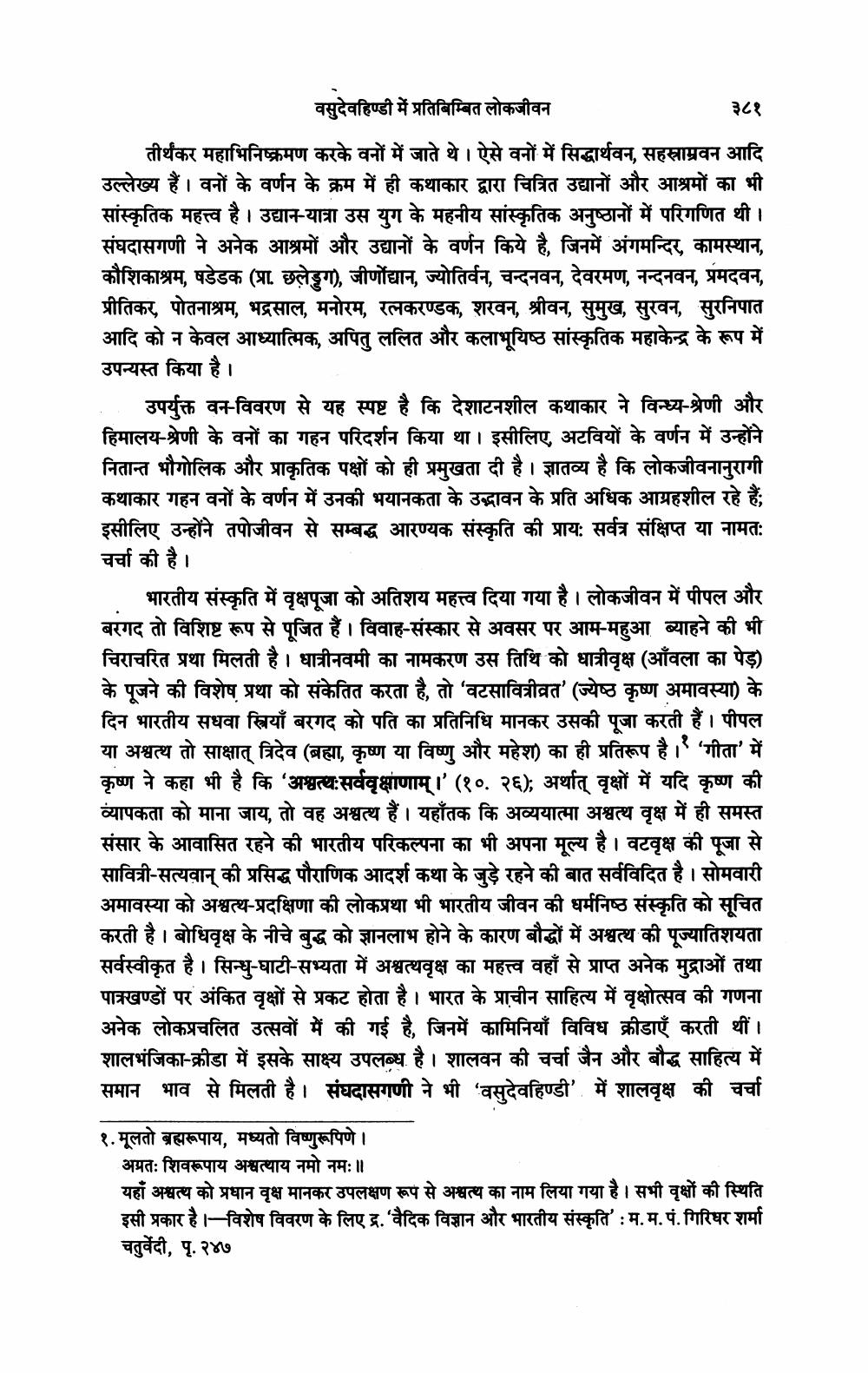________________
३८१
वसुदेवहिण्डी में प्रतिबिम्बित लोकजीवन तीर्थंकर महाभिनिष्क्रमण करके वनों में जाते थे। ऐसे वनों में सिद्धार्थवन, सहस्राम्रवन आदि उल्लेख्य हैं। वनों के वर्णन के क्रम में ही कथाकार द्वारा चित्रित उद्यानों और आश्रमों का भी सांस्कृतिक महत्त्व है। उद्यान-यात्रा उस युग के महनीय सांस्कृतिक अनुष्ठानों में परिगणित थी। संघदासगणी ने अनेक आश्रमों और उद्यानों के वर्णन किये है, जिनमें अंगमन्दिर, कामस्थान, कौशिकाश्रम, षडेडक (प्रा. छलेड्डग), जीर्णोद्यान, ज्योतिर्वन, चन्दनवन, देवरमण, नन्दनवन, प्रमदवन, प्रीतिकर, पोतनाश्रम, भद्रसाल, मनोरम, रत्नकरण्डक, शरवन, श्रीवन, सुमुख, सुरवन, सुरनिपात आदि को न केवल आध्यात्मिक, अपितु ललित और कलाभूयिष्ठ सांस्कृतिक महाकेन्द्र के रूप में उपन्यस्त किया है।
. उपर्युक्त वन-विवरण से यह स्पष्ट है कि देशाटनशील कथाकार ने विन्ध्य-श्रेणी और हिमालय-श्रेणी के वनों का गहन परिदर्शन किया था। इसीलिए, अटवियों के वर्णन में उन्होंने नितान्त भौगोलिक और प्राकृतिक पक्षों को ही प्रमुखता दी है। ज्ञातव्य है कि लोकजीवनानुरागी कथाकार गहन वनों के वर्णन में उनकी भयानकता के उद्भावन के प्रति अधिक आग्रहशील रहे हैं; इसीलिए उन्होंने तपोजीवन से सम्बद्ध आरण्यक संस्कृति की प्राय: सर्वत्र संक्षिप्त या नामत: चर्चा की है।
भारतीय संस्कृति में वृक्षपूजा को अतिशय महत्त्व दिया गया है । लोकजीवन में पीपल और बरगद तो विशिष्ट रूप से पूजित हैं। विवाह-संस्कार से अवसर पर आम-महुआ ब्याहने की भी चिराचरित प्रथा मिलती है। धात्रीनवमी का नामकरण उस तिथि को धात्रीवृक्ष (आँवला का पेड़) के पूजने की विशेष प्रथा को संकेतित करता है, तो 'वटसावित्रीव्रत' (ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या) के दिन भारतीय सधवा स्त्रियाँ बरगद को पति का प्रतिनिधि मानकर उसकी पूजा करती हैं। पीपल या अश्वत्थ तो साक्षात् त्रिदेव (ब्रह्मा, कृष्ण या विष्णु और महेश) का ही प्रतिरूप है।' 'गीता' में कृष्ण ने कहा भी है कि 'अश्वत्थःसर्ववृक्षाणाम्।' (१०. २६); अर्थात् वृक्षों में यदि कृष्ण की व्यापकता को माना जाय, तो वह अश्वत्थ हैं। यहाँतक कि अव्ययात्मा अश्वत्थ वृक्ष में ही समस्त संसार के आवासित रहने की भारतीय परिकल्पना का भी अपना मूल्य है। वटवृक्ष की पूजा से सावित्री-सत्यवान् की प्रसिद्ध पौराणिक आदर्श कथा के जुड़े रहने की बात सर्वविदित है। सोमवारी अमावस्या को अश्वत्थ-प्रदक्षिणा की लोकप्रथा भी भारतीय जीवन की धर्मनिष्ठ संस्कृति को सूचित करती है । बोधिवृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञानलाभ होने के कारण बौद्धों में अश्वत्थ की पूज्यातिशयता सर्वस्वीकत है। सिन्ध-घाटी-सभ्यता में अश्वत्थवक्ष का महत्त्व वहाँ से प्राप्त अनेक मद्राओं तथा पात्रखण्डों पर अंकित वृक्षों से प्रकट होता है। भारत के प्राचीन साहित्य में वृक्षोत्सव की गणना अनेक लोकप्रचलित उत्सवों में की गई है, जिनमें कामिनियाँ विविध क्रीडाएँ करती थीं। शालभंजिका-क्रीडा में इसके साक्ष्य उपलब्ध है। शालवन की चर्चा जैन और बौद्ध साहित्य में समान भाव से मिलती है। संघदासगणी ने भी 'वसुदेवहिण्डी' में शालवृक्ष की चर्चा
१. मूलतो ब्रह्मरूपाय, मध्यतो विष्णुरूपिणे।
अग्रत: शिवरूपाय अश्वत्थाय नमो नमः॥ यहाँ अश्वत्थ को प्रधान वृक्ष मानकर उपलक्षण रूप से अश्वत्थ का नाम लिया गया है। सभी वृक्षों की स्थिति इसी प्रकार है। विशेष विवरण के लिए द्र. वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति' : म.म.पं.गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, पृ. २४७