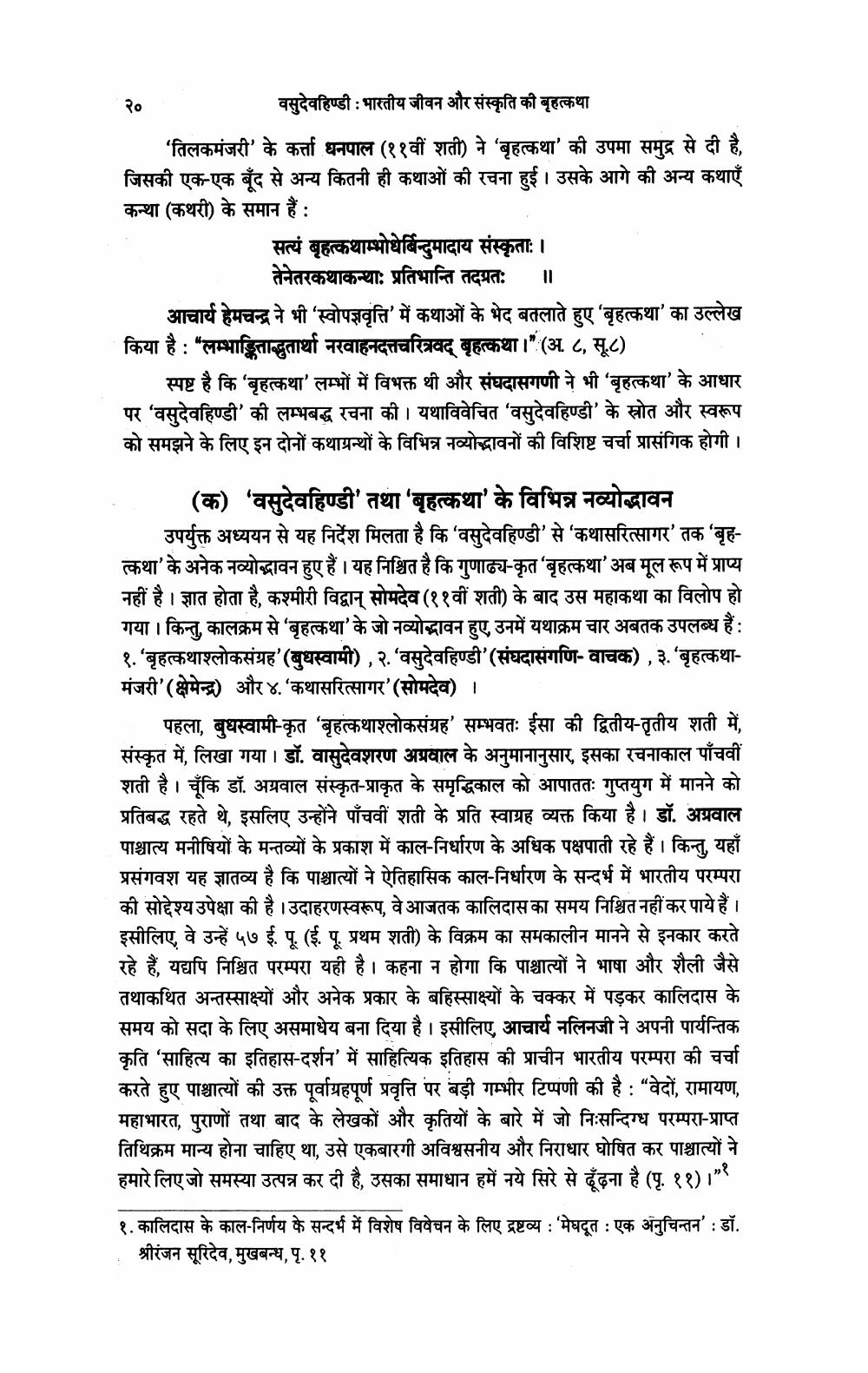________________
वसुदेवहिण्डी : भारतीय जीवन और संस्कृति की बृहत्कथा
'तिलकमंजरी' के कर्त्ता धनपाल (११वीं शती) ने 'बृहत्कथा' की उपमा समुद्र से दी है, जिसकी एक-एक बूँद से अन्य कितनी ही कथाओं की रचना हुई। उसके आगे की अन्य कथाएँ कन्था (कथरी) के समान हैं :
२०
सत्यं बृहत्कथाम्भोधेर्बिन्दुमादाय संस्कृताः । तेनेतरकथाकन्थाः प्रतिभान्ति तदग्रतः ॥
आचार्य हेमचन्द्र ने भी 'स्वोपज्ञवृत्ति' में कथाओं के भेद बतलाते हुए 'बृहत्कथा' का उल्लेख किया है : “लम्भाङ्किताद्भुतार्था नरवाहनदत्तचरित्रवद् बृहत्कथा ।" (अ. ८, सू.८)
स्पष्ट है कि 'बृहत्कथा' लम्भों में विभक्त थी और संघदासगणी ने भी 'बृहत्कथा' के आधार पर 'वसुदेवहिण्डी' की लम्भबद्ध रचना की । यथाविवेचित 'वसुदेवहिण्डी' के स्रोत और स्वरूप को समझने के लिए इन दोनों कथाग्रन्थों के विभिन्न नव्योद्भावनों की विशिष्ट चर्चा प्रासंगिक होगी ।
(क) 'वसुदेवहिण्डी' तथा 'बृहत्कथा' के विभिन्न नव्योद्भावन
उपर्युक्त अध्ययन से यह निर्देश मिलता है कि 'वसुदेवहिण्डी' से 'कथासरित्सागर' तक 'बृहत्कथा' के अनेक नव्योद्भावन हुए हैं। यह निश्चित है कि गुणाढ्य - कृत 'बृहत्कथा' अब मूल रूप में प्राप्य नहीं है । ज्ञात होता है, कश्मीरी विद्वान् सोमदेव (११वीं शती) के बाद उस महाकथा का विलोप हो गया । किन्तु कालक्रम से 'बृहत्कथा' के जो नव्योद्भावन हुए, उनमें यथाक्रम चार अबतक उपलब्ध हैं: १. 'बृहत्कथाश्लोकसंग्रह' (बुधस्वामी), २. 'वसुदेवहिण्डी' (संघदासंगणि- वाचक), ३. 'बृहत्कथामंजरी' (क्षेमेन्द्र) और ४. 'कथासरित्सागर' (सोमदेव) ।
पहला, बुधस्वामी - कृत 'बृहत्कथाश्लोकसंग्रह ' सम्भवतः ईसा की द्वितीय - तृतीय शती में, संस्कृत में, लिखा गया। डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल के अनुमानानुसार, इसका रचनाकाल पाँचवीं शती है। चूँकि डॉ. अग्रवाल संस्कृत - प्राकृत के समृद्धिकाल को आपाततः गुप्तयुग में मानने को प्रतिबद्ध रहते थे, इसलिए उन्होंने पाँचवीं शती के प्रति स्वाग्रह व्यक्त किया है। डॉ. अग्रवाल पाश्चात्य मनीषियों के मन्तव्यों के प्रकाश में काल-निर्धारण के अधिक पक्षपाती रहे हैं । किन्तु, यहाँ प्रसंगवश यह ज्ञातव्य है कि पाश्चात्यों ने ऐतिहासिक काल-निर्धारण के सन्दर्भ में भारतीय परम्परा की सोद्देश्य उपेक्षा की है । उदाहरणस्वरूप, वे आजतक कालिदास का समय निश्चित नहीं कर पाये हैं । इसीलिए वे उन्हें ५७ ई. पू. ( ई. पू. प्रथम शती) के विक्रम का समकालीन मानने से इनकार करते रहे हैं, यद्यपि निश्चित परम्परा यही है । कहना न होगा कि पाश्चात्यों ने भाषा और शैली जैसे तथाकथित अन्तस्साक्ष्यों और अनेक प्रकार के बहिस्साक्ष्यों के चक्कर में पड़कर कालिदास के समय को सदा के लिए असमाधेय बना दिया है। इसीलिए, आचार्य नलिनजी ने अपनी पार्यन्तिक कृति 'साहित्य का इतिहास - दर्शन' में साहित्यिक इतिहास की प्राचीन भारतीय परम्परा की चर्चा करते हुए पाश्चात्यों की उक्त पूर्वाग्रहपूर्ण प्रवृत्ति पर बड़ी गम्भीर टिप्पणी की है : "वेदों, रामायण, महाभारत, पुराणों तथा बाद के लेखकों और कृतियों के बारे में जो निःसन्दिग्ध परम्परा - प्राप्त तिथिक्रम मान्य होना चाहिए था, उसे एकबारगी अविश्वसनीय और निराधार घोषित कर पाश्चात्यों ने हमारे लिए जो समस्या उत्पन्न कर दी है, उसका समाधान हमें नये सिरे से ढूँढ़ना है (पृ. ११) । १
१. कालिदास के काल-निर्णय के सन्दर्भ में विशेष विवेचन के लिए द्रष्टव्य : 'मेघदूत : एक अनुचिन्तन' : डॉ. श्रीरंजन सूरिदेव, मुखबन्ध, पृ. ११