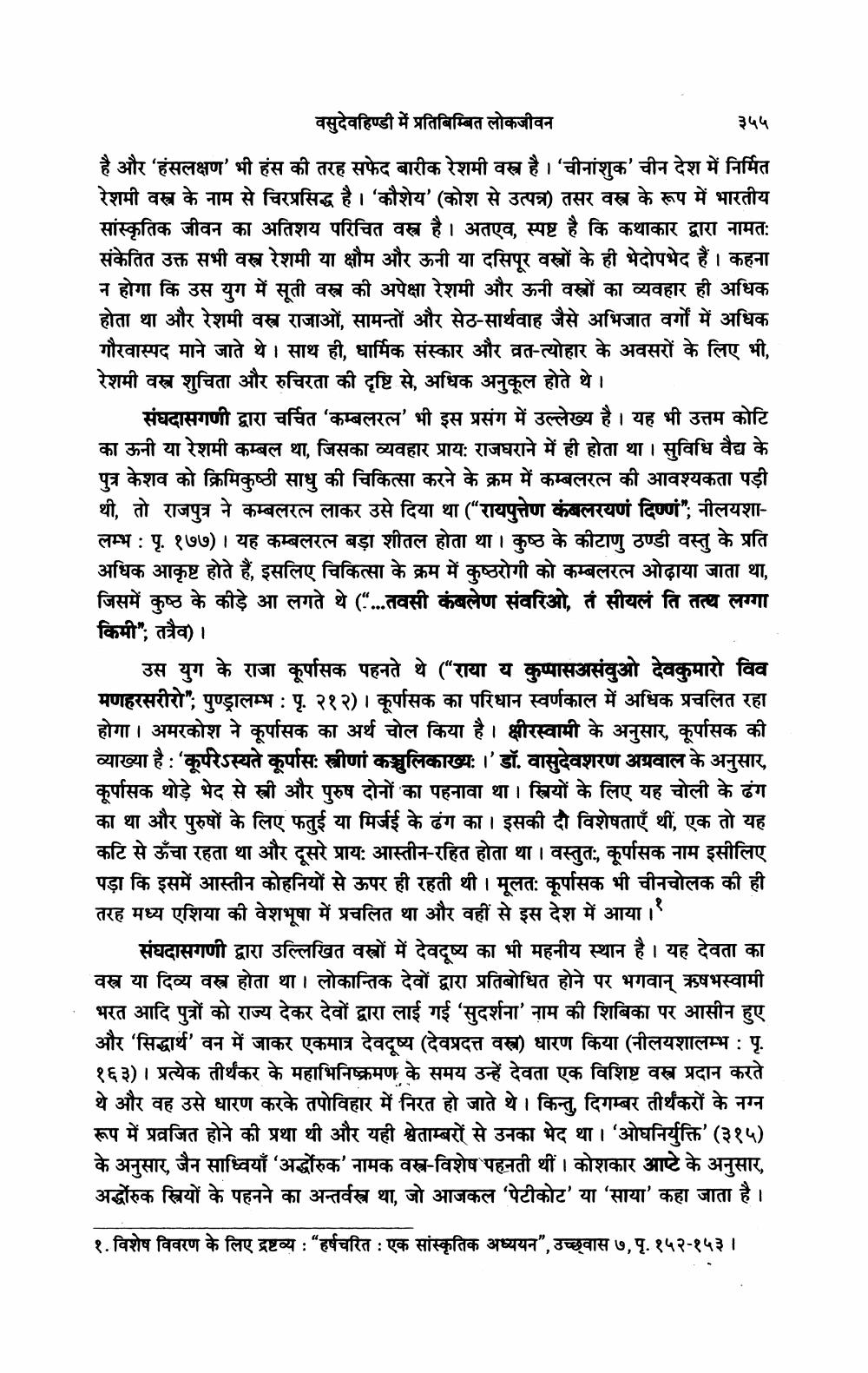________________
वसुदेवहिण्डी में प्रतिबिम्बित लोकजीवन
है और 'हंसलक्षण' भी हंस की तरह सफेद बारीक रेशमी वस्त्र है । 'चीनांशुक' चीन देश में निर्मित रेशमी वस्त्र के नाम से चिरप्रसिद्ध है । 'कौशेय' (कोश से उत्पन्न) तसर वस्त्र के रूप में भारतीय सांस्कृतिक जीवन का अतिशय परिचित वस्त्र है । अतएव, स्पष्ट है कि कथाकार द्वारा नामतः संकेतित उक्त सभी वस्त्र रेशमी या क्षौम और ऊनी या दसिपूर वस्त्रों के ही भेदोपभेद हैं । कहना
होगा कि उस युग में सूती वस्त्र की अपेक्षा रेशमी और ऊनी वस्त्रों का व्यवहार ही अधिक होता था और रेशमी वस्त्र राजाओं, सामन्तों और सेठ-सार्थवाह जैसे अभिजात वर्गों में अधिक गौरवास्पद माने जाते थे। साथ ही, धार्मिक संस्कार और व्रत-त्योहार के अवसरों के लिए भी, रेशमी वस्त्र शुचिता और रुचिरता की दृष्टि से, अधिक अनुकूल होते थे
1
३५५
संघदासगणी द्वारा चर्चित 'कम्बलरल' भी इस प्रसंग में उल्लेख्य है । यह भी उत्तम कोटि का ऊनी या रेशमी कम्बल था, जिसका व्यवहार प्राय: राजघराने में ही होता था । सुविधि वैद्य के पुत्र केशव को क्रिमिकुष्ठी साधु की चिकित्सा करने के क्रम में कम्बलरत्न की आवश्यकता पड़ी थी, तो राजपुत्र ने कम्बलरल लाकर उसे दिया था (" रायपुत्तेण कंबलरयणं दिण्णं "; नीलयशालम्भ : पृ. १७७)। यह कम्बलरत्न बड़ा शीतल होता था । कुष्ठ के कीटाणु ठण्डी वस्तु अधिक आकृष्ट होते हैं, इसलिए चिकित्सा के क्रम में कुष्ठरोगी को कम्बलरत्न ओढ़ाया जाता था, जिसमें कुष्ठ के कीड़े आ लगते थे (...तवसी कंबलेण संवरिओ, तं सीयलं ति तत्थ लग्गा किमी ; तत्रैव) ।
उस युग के राजा कूर्पासक पहनते थे ("राया य कुप्पासअसंवुओ देवकुमारो विव मणहरसरीरो",; पुण्ड्रालम्भ: पृ. २१२) । कूर्पासक का परिधान स्वर्णकाल में अधिक प्रचलित रहा होगा। अमरकोश ने कूर्पासक का अर्थ चोल किया है। क्षीरस्वामी के अनुसार, कूर्पासक की व्याख्या है : 'कूर्परेऽस्यते कूर्पासः स्त्रीणां कञ्चलिकाख्यः ।' डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल के अनुसार, कूर्पासक थोड़े भेद से स्त्री और पुरुष दोनों का पहनावा था । स्त्रियों के लिए यह चोली के ढंग का था और पुरुषों के लिए फतुई या मिर्जई के ढंग का । इसकी दो विशेषताएँ थीं, एक तो यह कटि से ऊँचा रहता था और दूसरे प्रायः आस्तीन - रहित होता था । वस्तुतः कूर्पासक नाम इसीलिए पड़ा कि इसमें आस्तीन कोहनियों से ऊपर ही रहती थी । मूलतः कूर्पासक भी चीनचोलक की ही तरह मध्य एशिया की वेशभूषा में प्रचलित था और वहीं से इस देश में आया । '
संघदासगणी द्वारा उल्लिखित वस्त्रों में देवदूष्य का भी महनीय स्थान है । यह देवता क वस्त्र या दिव्य वस्त्र होता था । लोकान्तिक देवों द्वारा प्रतिबोधित होने पर भगवान् ऋषभस्वामी भरत आदि पुत्रों को राज्य देकर देवों द्वारा लाई गई 'सुदर्शना' नाम की शिबिका पर आसीन हुए और 'सिद्धार्थ' वन में जाकर एकमात्र देवदूष्य (देवप्रदत्त वस्त्र धारण किया (नीलयशालम्भ : पृ. १६३)। प्रत्येक तीर्थंकर के महाभिनिष्क्रमण के समय उन्हें देवता एक विशिष्ट वस्त्र प्रदान करते थे और वह उसे धारण करके तपोविहार में निरत हो जाते थे । किन्तु, दिगम्बर तीर्थंकरों के नग्न रूप में प्रव्रजित होने की प्रथा थी और यही श्वेताम्बरों से उनका भेद था । 'ओघनिर्युक्ति' (३१५) के अनुसार, जैन साध्वियाँ 'अद्धरुक' नामक वस्त्र-विशेष पहनती थीं। कोशकार आप्टे के अनुसार, अर्द्धांरुक स्त्रियों के पहनने का अन्तर्वस्त्र था, जो आजकल 'पेटीकोट' या 'साया' कहा जाता है ।
१. विशेष विवरण के लिए द्रष्टव्य : " हर्षचरित : एक सांस्कृतिक अध्ययन”, उच्छ्वास ७, पृ. १५२-१५३ |