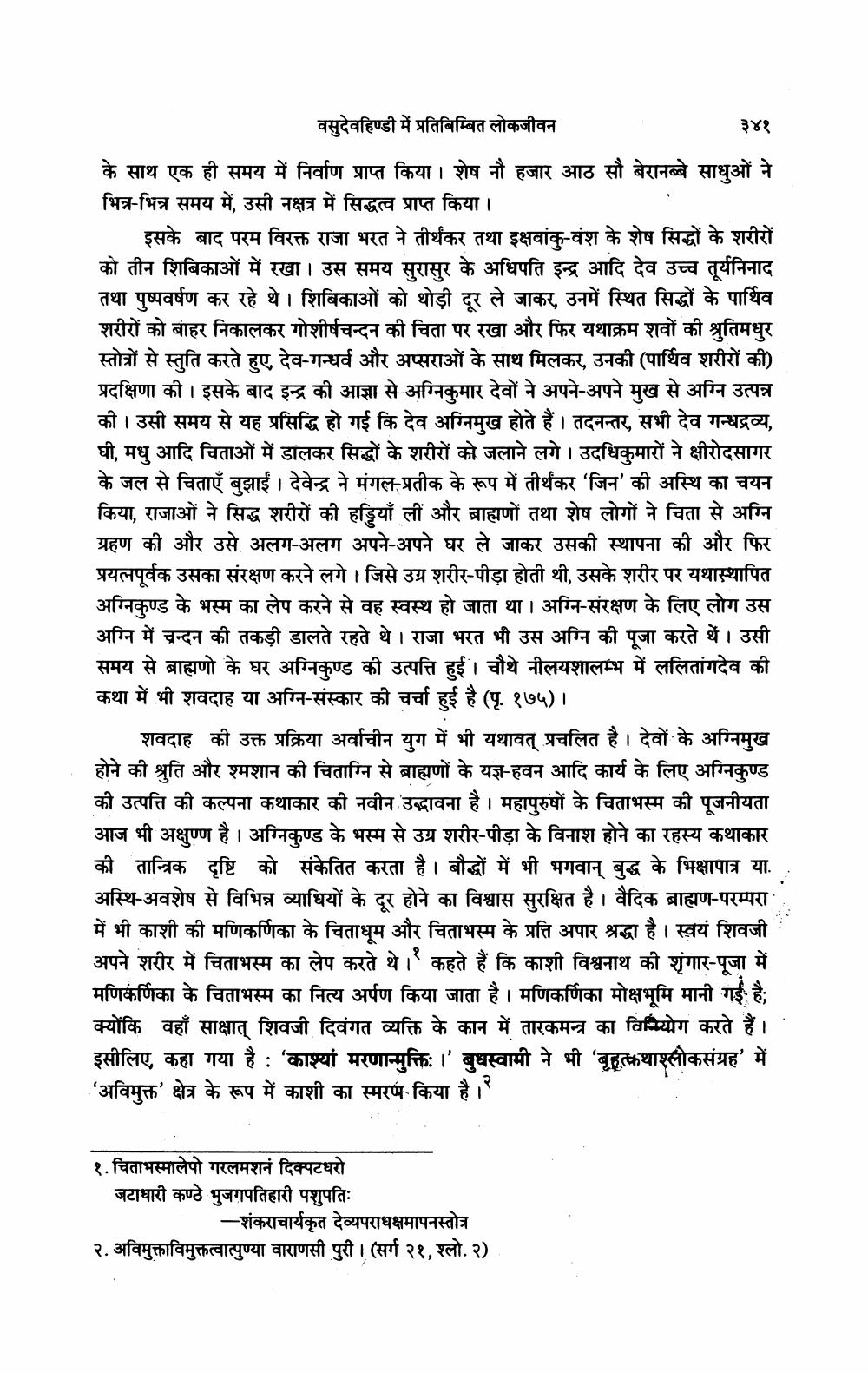________________
वसुदेवहिण्डी में प्रतिबिम्बित लोकजीवन
३४१
के साथ एक ही समय में निर्वाण प्राप्त किया। शेष नौ हजार आठ सौ बेरानब्बे साधुओं ने भिन्न-भिन्न समय में, उसी नक्षत्र में सिद्धत्व प्राप्त किया।
इसके बाद परम विरक्त राजा भरत ने तीर्थंकर तथा इक्षवांकु-वंश के शेष सिद्धों के शरीरों को तीन शिबिकाओं में रखा। उस समय सुरासुर के अधिपति इन्द्र आदि देव उच्च तूर्यनिनाद तथा पुष्पवर्षण कर रहे थे। शिबिकाओं को थोड़ी दूर ले जाकर, उनमें स्थित सिद्धों के पार्थिव शरीरों को बाहर निकालकर गोशीर्षचन्दन की चिता पर रखा और फिर यथाक्रम शवों की श्रुतिमधुर स्तोत्रों से स्तुति करते हुए, देव-गन्धर्व और अप्सराओं के साथ मिलकर, उनकी (पार्थिव शरीरों की) प्रदक्षिणा की। इसके बाद इन्द्र की आज्ञा से अग्निकुमार देवों ने अपने-अपने मुख से अग्नि उत्पन्न की। उसी समय से यह प्रसिद्धि हो गई कि देव अग्निमुख होते हैं। तदनन्तर, सभी देव गन्धद्रव्य, घी, मधु आदि चिताओं में डालकर सिद्धों के शरीरों को जलाने लगे। उदधिकुमारों ने क्षीरोदसागर के जल से चिताएँ बुझाईं। देवेन्द्र ने मंगल-प्रतीक के रूप में तीर्थंकर 'जिन' की अस्थि का चयन किया, राजाओं ने सिद्ध शरीरों की हड्डियाँ लीं और ब्राह्मणों तथा शेष लोगों ने चिता से अग्नि ग्रहण की और उसे. अलग-अलग अपने-अपने घर ले जाकर उसकी स्थापना की और फिर प्रयत्नपूर्वक उसका संरक्षण करने लगे। जिसे उग्र शरीर-पीड़ा होती थी, उसके शरीर पर यथास्थापित अग्निकुण्ड के भस्म का लेप करने से वह स्वस्थ हो जाता था। अग्नि-संरक्षण के लिए लोग उस अग्नि में चन्दन की तकड़ी डालते रहते थे। राजा भरत भी उस अग्नि की पूजा करते थे। उसी समय से ब्राह्मणो के घर अग्निकुण्ड की उत्पत्ति हुई। चौथे नीलयशालम्भ में ललितांगदेव की कथा में भी शवदाह या अग्नि-संस्कार की चर्चा हुई है (पृ. १७५) ।
शवदाह की उक्त प्रक्रिया अर्वाचीन युग में भी यथावत् प्रचलित है। देवों के अग्निमुख होने की श्रुति और श्मशान की चिताग्नि से ब्राह्मणों के यज्ञ-हवन आदि कार्य के लिए अग्निकुण्ड की उत्पत्ति की कल्पना कथाकार की नवीन उद्भावना है। महापुरुषों के चिताभस्म की पूजनीयता आज भी अक्षुण्ण है । अग्निकुण्ड के भस्म से उग्र शरीर-पीड़ा के विनाश होने का रहस्य कथाकार की तान्त्रिक दृष्टि को संकेतित करता है। बौद्धों में भी भगवान् बुद्ध के भिक्षापात्र या. अस्थि-अवशेष से विभिन्न व्याधियों के दूर होने का विश्वास सुरक्षित है। वैदिक ब्राह्मण-परम्परा में भी काशी की मणिकर्णिका के चिताधूम और चिताभस्म के प्रति अपार श्रद्धा है। स्वयं शिवजी अपने शरीर में चिताभस्म का लेप करते थे। कहते हैं कि काशी विश्वनाथ की शृंगार-पूजा में मणिकर्णिका के चिताभस्म का नित्य अर्पण किया जाता है। मणिकर्णिका मोक्षभूमि मानी गई है; क्योंकि वहाँ साक्षात् शिवजी दिवंगत व्यक्ति के कान में तारकमन्त्र का विडियोग करते हैं। इसीलिए, कहा गया है : 'काश्यां मरणान्मुक्तिः ।' बुधस्वामी ने भी 'बृहत्कथाश्लोकसंग्रह' में 'अविमुक्त' क्षेत्र के रूप में काशी का स्मरण किया है।
१.चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपतिः
-शंकराचार्यकृत देव्यपराधक्षमापनस्तोत्र २. अविमुक्ताविमुक्तत्वात्पुण्या वाराणसी पुरी । (सर्ग २१, श्लो. २)