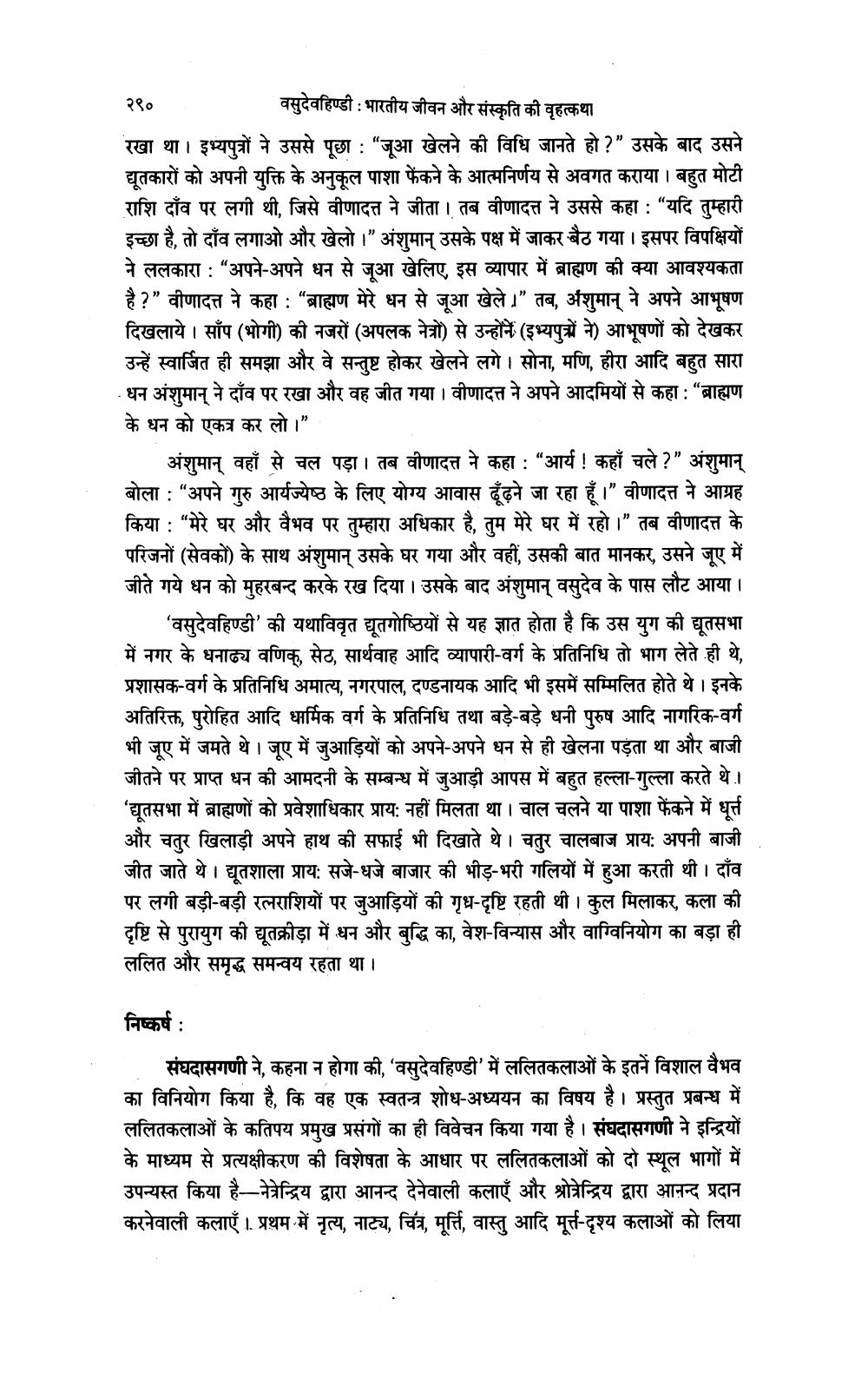________________
२९०
वसुदेवहिण्डी : भारतीय जीवन और संस्कृति की वृहत्कथा रखा था। इभ्यपुत्रों ने उससे पूछा : “जूआ खेलने की विधि जानते हो?" उसके बाद उसने द्यूतकारों को अपनी युक्ति के अनुकूल पाशा फेंकने के आत्मनिर्णय से अवगत कराया। बहुत मोटी राशि दाँव पर लगी थी, जिसे वीणादत्त ने जीता । तब वीणादत्त ने उससे कहा : “यदि तुम्हारी इच्छा है, तो दाँव लगाओ और खेलो।" अंशुमान् उसके पक्ष में जाकर बैठ गया। इसपर विपक्षियों ने ललकारा : “अपने-अपने धन से जुआ खेलिए, इस व्यापार में ब्राह्मण की क्या आवश्यकता है ?" वीणादत्त ने कहा : "ब्राह्मण मेरे धन से जूआ खेले।” तब, अंशुमान् ने अपने आभूषण दिखलाये। साँप (भोगी) की नजरों (अपलक नेत्रों) से उन्होंने (इभ्यपुत्रों ने) आभूषणों को देखकर उन्हें स्वार्जित ही समझा और वे सन्तुष्ट होकर खेलने लगे। सोना, मणि, हीरा आदि बहुत सारा धन अंशुमान् ने दाँव पर रखा और वह जीत गया। वीणादत्त ने अपने आदमियों से कहा : “ब्राह्मण के धन को एकत्र कर लो।" ____ अंशुमान् वहाँ से चल पड़ा। तब वीणादत्त ने कहा : “आर्य ! कहाँ चले?" अंशुमान् बोला : “अपने गुरु आर्यज्येष्ठ के लिए योग्य आवास ढूँढ़ने जा रहा हूँ।” वीणादत्त ने आग्रह किया : “मेरे घर और वैभव पर तुम्हारा अधिकार है, तुम मेरे घर में रहो।” तब वीणादत्त के परिजनों (सेवकों) के साथ अंशुमान् उसके घर गया और वहीं, उसकी बात मानकर, उसने जूए में जीते गये धन को मुहरबन्द करके रख दिया। उसके बाद अंशुमान् वसुदेव के पास लौट आया ।
'वसुदेवहिण्डी' की यथाविवृत द्यूतगोष्ठियों से यह ज्ञात होता है कि उस युग की द्यूतसभा में नगर के धनाढ्य वणिक्, सेठ, सार्थवाह आदि व्यापारी-वर्ग के प्रतिनिधि तो भाग लेते ही थे, प्रशासक-वर्ग के प्रतिनिधि अमात्य, नगरपाल, दण्डनायक आदि भी इसमें सम्मिलित होते थे। इनके अतिरिक्त, पुरोहित आदि धार्मिक वर्ग के प्रतिनिधि तथा बड़े-बड़े धनी पुरुष आदि नागरिक-वर्ग भी जूए में जमते थे। जूए में जुआड़ियों को अपने-अपने धन से ही खेलना पड़ता था और बाजी जीतने पर प्राप्त धन की आमदनी के सम्बन्ध में जुआड़ी आपस में बहुत हल्ला-गुल्ला करते थे। 'द्यूतसभा में ब्राह्मणों को प्रवेशाधिकार प्राय: नहीं मिलता था। चाल चलने या पाशा फेंकने में धूर्त
और चतुर खिलाड़ी अपने हाथ की सफाई भी दिखाते थे। चतुर चालबाज प्राय: अपनी बाजी जीत जाते थे। द्यूतशाला प्राय: सजे-धजे बाजार की भीड़-भरी गलियों में हुआ करती थी। दाँव पर लगी बड़ी-बड़ी रत्नराशियों पर जुआड़ियों की गृध्र-दृष्टि रहती थी। कुल मिलाकर, कला की दृष्टि से पुरायुग की द्यूतक्रीड़ा में धन और बुद्धि का, वेश-विन्यास और वाग्विनियोग का बड़ा ही ललित और समृद्ध समन्वय रहता था।
निष्कर्ष :
संघदासगणी ने, कहना न होगा की, 'वसुदेवहिण्डी' में ललितकलाओं के इतने विशाल वैभव का विनियोग किया है, कि वह एक स्वतन्त्र शोध-अध्ययन का विषय है। प्रस्तुत प्रबन्ध में ललितकलाओं के कतिपय प्रमुख प्रसंगों का ही विवेचन किया गया है। संघदासगणी ने इन्द्रियों के माध्यम से प्रत्यक्षीकरण की विशेषता के आधार पर ललितकलाओं को दो स्थूल भागों में उपन्यस्त किया है—नेत्रेन्द्रिय द्वारा आनन्द देनेवाली कलाएँ और श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा आनन्द प्रदान करनेवाली कलाएँ । प्रथम में नृत्य, नाट्य, चित्र, मूर्ति, वास्तु आदि मूर्त-दृश्य कलाओं को लिया