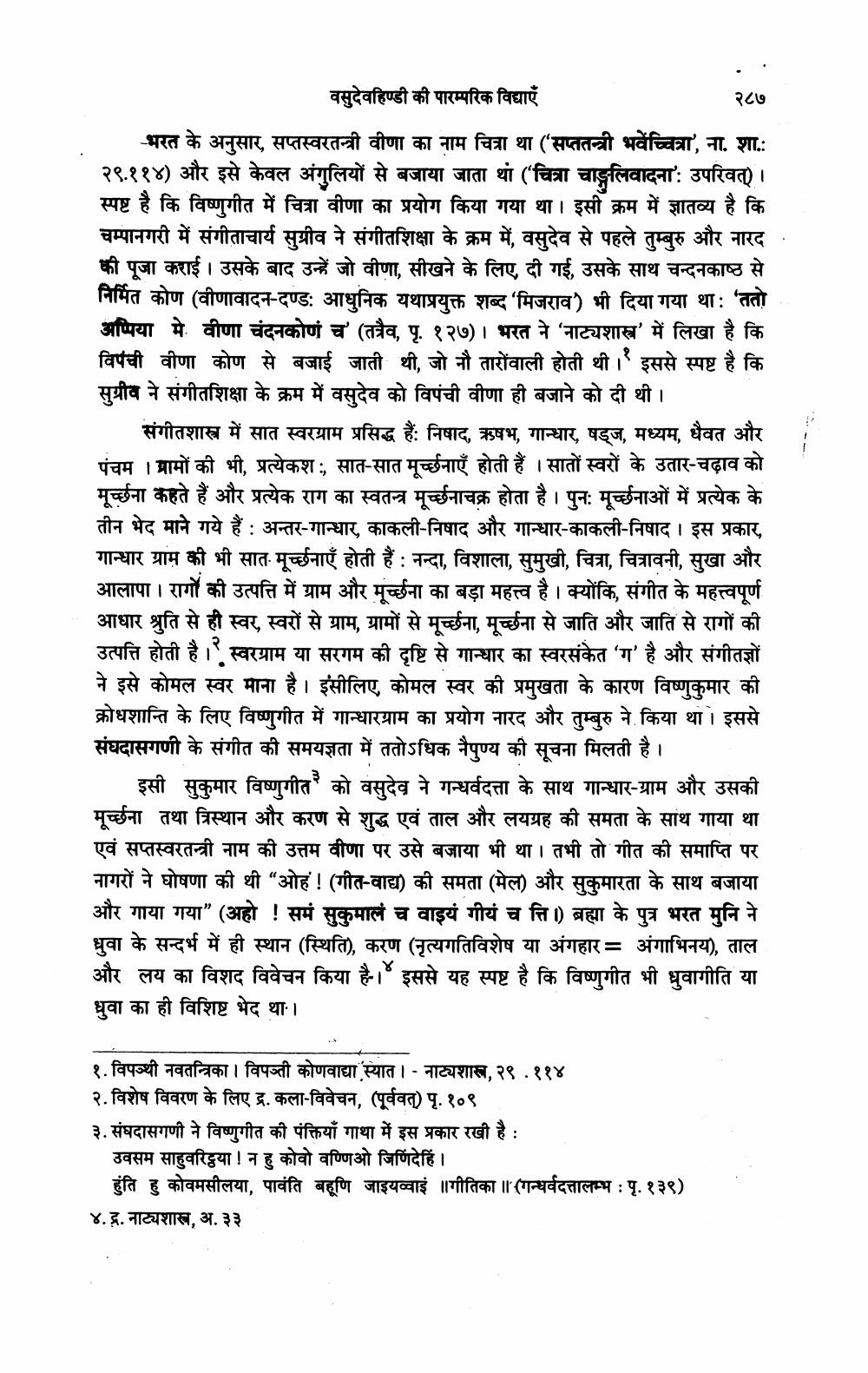________________
वसुदेवहिण्डी की पारम्परिक विद्याएँ
२८७
-भरत के अनुसार, सप्तस्वरतन्त्री वीणा का नाम चित्रा था ('सप्ततन्त्री भवेंच्चित्रा, ना. शा.: २९.११४) और इसे केवल अंगुलियों से बजाया जाता थां (चित्रा चाङ्गुलिवादना': उपरिवत्) । स्पष्ट है कि विष्णुगीत में चित्रा वीणा का प्रयोग किया गया था। इसी क्रम में ज्ञातव्य है कि चम्पानगरी में संगीताचार्य सुग्रीव ने संगीतशिक्षा के क्रम में, वसुदेव से पहले तुम्बुरु और नारद की पूजा कराई। उसके बाद उन्हें जो वीणा, सीखने के लिए, दी गई, उसके साथ चन्दनकाष्ठ से निर्मित कोण (वीणावादन-दण्डः आधुनिक यथाप्रयुक्त शब्द 'मिजराव ) भी दिया गया था : 'ततो अप्पिया मे वीणा चंदनकोणं च (तत्रैव, पृ. १२७) । भरत ने 'नाट्यशास्त्र' में लिखा है कि विपची वीणा कोण से बजाई जाती थी, जो नौ तारोंवाली होती थी । इससे स्पष्ट है कि सुग्रीव ने संगीतशिक्षा के क्रम में वसुदेव को विपंची वीणा ही बजाने को दी थी ।
संगीतशास्त्र में सात स्वरग्राम प्रसिद्ध हैं: निषाद, ऋषभ, गान्धार, षड्ज, मध्यम, धैवत और पंचम । ग्रामों की भी, प्रत्येकशः, सात-सात मूर्च्छनाएँ होती हैं । सातों स्वरों के उतार-चढ़ाव को मूर्च्छना कहते हैं और प्रत्येक राग का स्वतन्त्र मूर्च्छनाचक्र होता है । पुनः मूर्च्छनाओं में प्रत्येक तीन भेद माने गये हैं: अन्तर- गान्धार, काकली - निषाद और गान्धार- काकली - निषाद । इस प्रकार, गान्धार ग्राम की भी सात मूर्च्छनाएँ होती हैं : नन्दा, विशाला, सुमुखी, चित्रा, चित्रावनी, सुखा और आलापा । राग की उत्पत्ति में ग्राम और मूर्च्छना का बड़ा महत्त्व है। क्योंकि, संगीत के महत्त्वपूर्ण आधार श्रुति से ही स्वर, स्वरों से ग्राम, ग्रामों से मूर्च्छना, मूर्च्छना से जाति और जाति से रागों की उत्पत्ति होती है । स्वरग्राम या सरगम की दृष्टि से गान्धार का स्वरसंकेत 'ग' है और संगीतज्ञों ने इसे कोमल स्वर माना है। इसीलिए कोमल स्वर की प्रमुखता के कारण विष्णुकुमार की
•
शान्ति के लिए विष्णुगीत में गान्धारग्राम का प्रयोग नारद और तुम्बुरु ने किया था । इससे संघदासगणी के संगीत की समयज्ञता में ततोऽधिक नैपुण्य की सूचना मिलती है ।
इसी सुकुमार विष्णुगीत को वसुदेव ने गन्धर्वदत्ता के साथ गान्धार-ग्राम और उसकी मूर्च्छना तथा त्रिस्थान और करण से शुद्ध एवं ताल और लयग्रह की समता के साथ गाया था एवं सप्तस्वरतन्त्री नाम की उत्तम वीणा पर उसे बजाया भी था। तभी तो गीत की समाप्ति पर नागरों ने घोषणा की थी "ओहं ! (गीत-वाद्य) की समता (मेल) और सुकुमारता के साथ बजाया और गाया गया” (अहो ! समं सुकुमालं च वाइयं गीयं च त्ति ।) ब्रह्मा के पुत्र भरत मुनि ने ध्रुवा के सन्दर्भ में ही स्थान (स्थिति), करण (नृत्यगतिविशेष या अंगहार = अंगाभिनय), ताल और लय का विशद विवेचन किया है। इससे यह स्पष्ट है कि विष्णुगीत भी ध्रुवागीति या ध्रुवा का ही विशिष्ट भेद था ।
१. विपञ्थी नवतन्त्रिका । विपती कोणवाद्या स्यात । नाट्यशास्त्र, २९. ११४
२. विशेष विवरण के लिए द्र. कला - विवेचन, (पूर्ववत्) पृ. १०९
३. संघदासगणी ने विष्णुगीत की पंक्तियाँ गाथा में इस प्रकार रखी है :
उवसम साहुवरिट्ठया ! न हु कोवो वण्णिओ जिणिदेहिं ।
हुति हु कोवमसीलया, पावंति बहूणि जाइयव्वाई ॥ गीतिका ॥ (गन्धर्वदत्तालम्भ : पृ. १३९)
४.द्र. नाट्यशास्त्र, अ. ३३