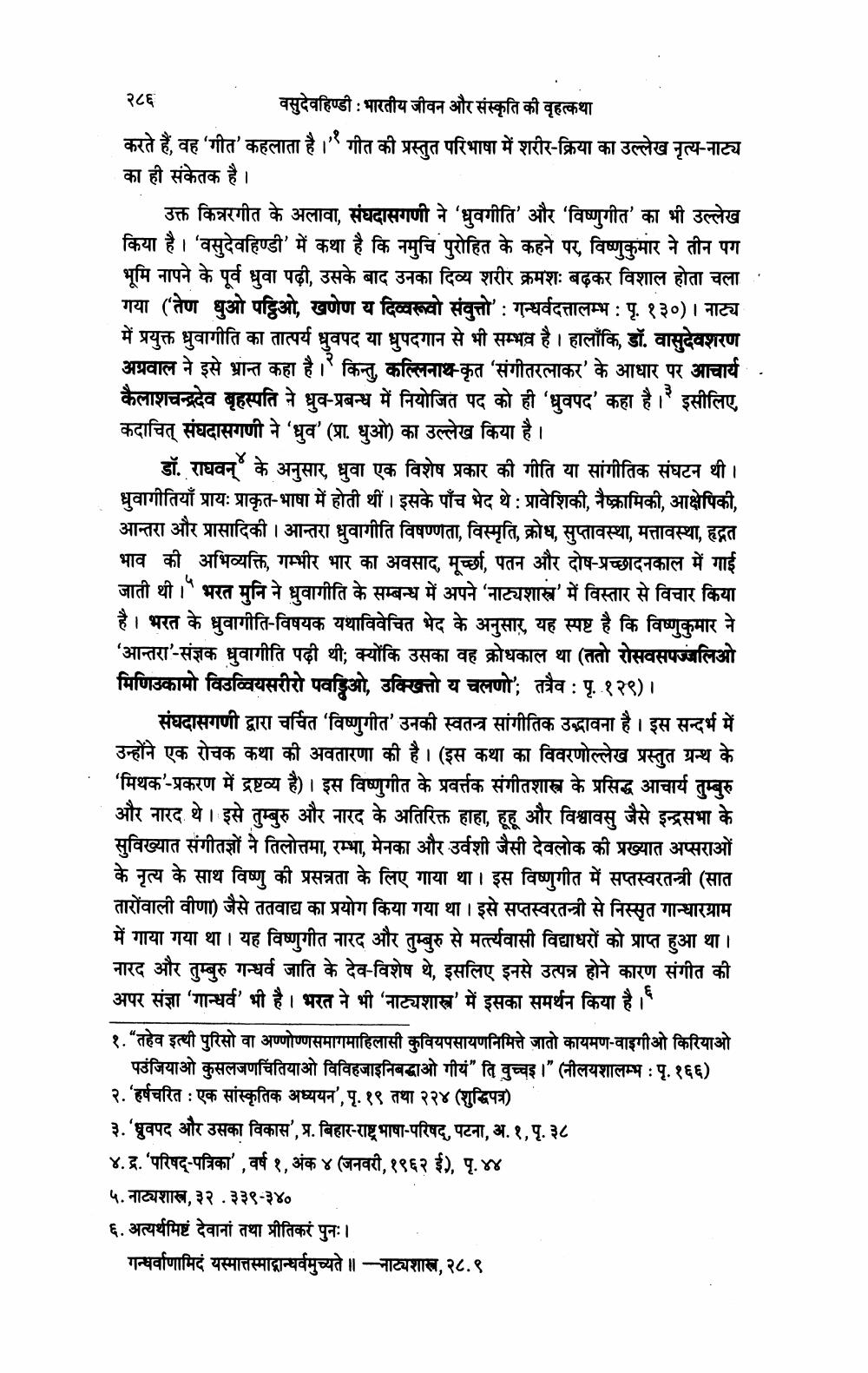________________
२८६
वसुदेवहिण्डी : भारतीय जीवन और संस्कृति की वृहत्कथा
करते हैं, वह ‘गीत' कहलाता है ।" गीत की प्रस्तुत परिभाषा में शरीर क्रिया का उल्लेख नृत्य-नाट्य का ही संकेतक है ।
उक्त किन्नरगीत के अलावा, संघदासगणी ने 'ध्रुवगीति' और 'विष्णुगीत' का भी उल्लेख किया है। 'वसुदेवहिण्डी' में कथा है कि नमुचि पुरोहित के कहने पर, विष्णुकुमार ने तीन पग भूमि नापने के पूर्व धुवा पढ़ी, उसके बाद उनका दिव्य शरीर क्रमशः बढ़कर विशाल होता चला गया ('तेण धुओ पट्टिओ, खणेण य दिव्वरूवो संवुत्तो' : गन्धर्वदत्तालम्भ: पृ. १३० ) । नाट्य में प्रयुक्त ध्रुवागीति का तात्पर्य ध्रुवपद या ध्रुपदगान से भी सम्भव है। हालाँकि, डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल ने इसे भ्रान्त कहा है। किन्तु कल्लिनाथ - कृत 'संगीतरत्नाकर' के आधार पर आचार्य कैलाशचन्द्रदेव बृहस्पति ने ध्रुव-प्रबन्ध में नियोजित पद को ही 'ध्रुवपद' कहा है। इसीलिए, कदाचित् संघदासगणी ने 'ध्रुव' (प्रा. धुओ) का उल्लेख किया है।
डॉ. राघवन् के अनुसार, ध्रुवा एक विशेष प्रकार की गीति या सांगीतिक संघटन थी। ध्रुवगीतियाँ प्रायः प्राकृत भाषा में होती थीं। इसके पाँच भेद थे : प्रावेशिकी, नैष्क्रामिकी, आक्षेपिकी, आन्तरा और प्रासादिकी । आन्तरा धुवागीति विषण्णता, विस्मृति, क्रोध, सुप्तावस्था, मत्तावस्था, भाव की अभिव्यक्ति, गम्भीर भार का अवसाद, मूर्च्छा, पतन और दोष- प्रच्छादनकाल में गाई थी। भरत मुनि धुवागीति के सम्बन्ध में अपने 'नाट्यशास्त्र' में विस्तार से विचार किया 14 है। भरत के ध्रुवागीति-विषयक यथाविवेचित भेद के अनुसार, यह स्पष्ट है कि विष्णुकुमार ने 'आन्तरा' - संज्ञक ध्रुवागीति पढ़ी थी; क्योंकि उसका वह क्रोधकाल था (ततो रोसवसपज्जलिओ मिणिउकामो विउव्वियसरीरो पवडिओ, उक्खित्तो य चलणो; तत्रैव : पृ. १२९) ।
संघदासगणी द्वारा चर्चित 'विष्णुगीत ' उनकी स्वतन्त्र सांगीतिक उद्भावना है। इस सन्दर्भ में उन्होंने एक रोचक कथा की अवतारणा की है। (इस कथा का विवरणोल्लेख प्रस्तुत ग्रन्थ के 'मिथक'- प्रकरण में द्रष्टव्य है)। इस विष्णुगीत के प्रवर्तक संगीतशास्त्र के प्रसिद्ध आचार्य तुम्बुरु और नारद थे । इसे तुम्बुरु और नारद के अतिरिक्त हाहा, हूहू और विश्वावसु जैसे इन्द्रसभा के सुविख्यात संगीतज्ञों ने तिलोत्तमा, रम्भा, मेनका और उर्वशी जैसी देवलोक की प्रख्यात अप्सराओं के नृत्य के साथ विष्णु की प्रसन्नता के लिए गाया था। इस विष्णुगीत में सप्तस्वरतन्त्री (सात तारोंवाली वीणा) जैसे ततवाद्य का प्रयोग किया गया था। इसे सप्तस्वरतन्त्री से निस्सृत गान्धारग्राम में गाया गया था । यह विष्णुगीत नारद और तुम्बुरु से मर्त्यवासी विद्याधरों को प्राप्त हुआ था । नारद और तुम्बुरु गन्धर्व जाति के देव-विशेष थे, इसलिए इनसे उत्पन्न होने कारण संगीत की अपर संज्ञा 'गान्धर्व' भी है। भरत ने भी 'नाट्यशास्त्र' में इसका समर्थन किया है।
१. “ तहेव इत्थी पुरिसो वा अण्णोष्णसमागमाहिलासी कुवियपसायणनिमित्ते जातो कायमण - वाइगीओ किरियाओ पउंजियाओ कुसलजणचिंतियाओ विविहजाइनिबद्धाओ गीयं” ति वुच्चइ ।” (नीलयशालम्भ: पृ. १६६)
२. 'हर्षचरित : एक सांस्कृतिक अध्ययन', पृ. १९ तथा २२४ (शुद्धिपत्र )
३. 'ध्रुवपद और उसका विकास', प्र. बिहार- राष्ट्र भाषा परिषद्, पटना, अ. १, पृ. ३८
४. द्र. 'परिषद्-पत्रिका', वर्ष १, अंक ४ (जनवरी, १९६२ ई), पृ. ४४
५. नाट्यशास्त्र, ३२.३३९-३४०
६. अत्यर्थमिष्टं देवानां तथा प्रीतिकरं पुनः ।
गन्धर्वाणामिदं यस्मात्तस्माद्गान्धर्वमुच्यते ॥ - नाट्यशास्त्र, २८.९