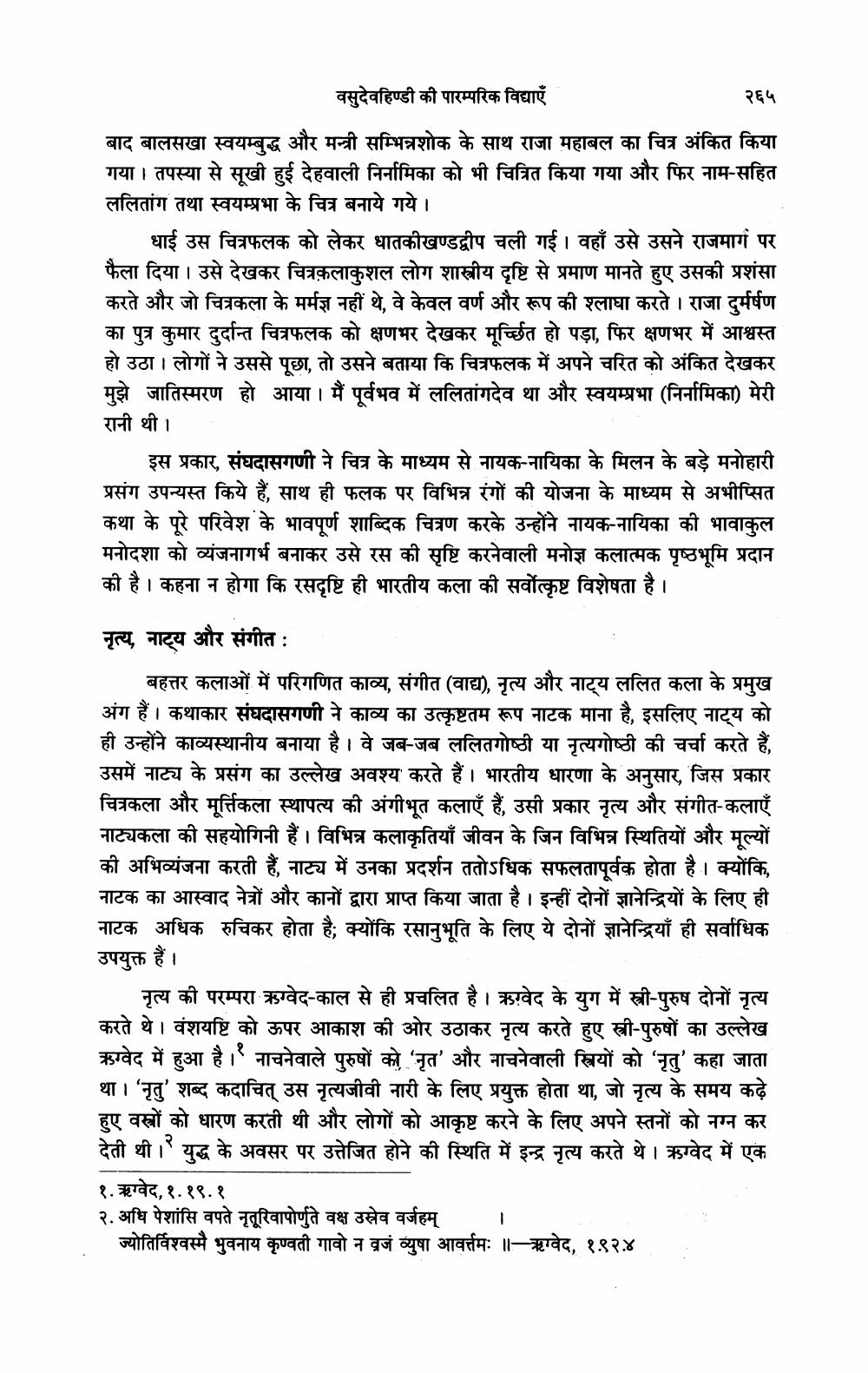________________
वसुदेवहिण्डी की पारम्परिक विद्याएँ
२६५
बाद बालसखा स्वयम्बुद्ध और मन्त्री सम्भिन्नशोक के साथ राजा महाबल का चित्र अंकित किया गया। तपस्या से सूखी हुई देहवाली निर्नामिका को भी चित्रित किया गया और फिर नाम- सहित ललितांग तथा स्वयम्प्रभा के चित्र बनाये गये ।
I
धाई उस चित्रफलक को लेकर धातकीखण्डद्वीप चली गई । वहाँ उसे उसने राजमार्ग पर फैला दिया । उसे देखकर चित्रकलाकुशल लोग शास्त्रीय दृष्टि से प्रमाण मानते हुए उसकी प्रशंसा करते और जो चित्रकला के मर्मज्ञ नहीं थे, वे केवल वर्ण और रूप की श्लाघा करते । राजा दुर्मर्षण का पुत्र कुमार दुर्दान्त चित्रफलक को क्षणभर देखकर मूर्च्छित हो पड़ा, फिर क्षणभर में आश्वस्त हो उठा। लोगों ने उससे पूछा, तो उसने बताया कि चित्रफलक में अपने चरित को अंकित देखकर मुझे जातिस्मरण हो आया। मैं पूर्वभव में ललितांगदेव था और स्वयम्प्रभा (निर्नामिका) मेरी रानी थी।
इस प्रकार, संघदासगणी ने चित्र के माध्यम से नायक-नायिका के मिलन के बड़े मनोहारी प्रसंग उपन्यस्त किये हैं, साथ ही फलक पर विभिन्न रंगों की योजना के माध्यम से अभीप्सित कथा के पूरे परिवेश के भावपूर्ण शाब्दिक चित्रण करके उन्होंने नायक-नायिका की भावाकुल मनोदशा को व्यंजनागर्भ बनाकर उसे रस की सृष्टि करनेवाली मनोज्ञ कलात्मक पृष्ठभूमि प्रदान की है । कहना न होगा कि रसदृष्टि ही भारतीय कला की सर्वोत्कृष्ट विशेषता है ।
नृत्य, नाट्य और संगीत :
बहत्तर कलाओं में परिगणित काव्य, संगीत (वाद्य), नृत्य और नाट्य ललित कला प्रमुख अंग हैं । कथाकार संघदासगणी ने काव्य का उत्कृष्टतम रूप नाटक माना है, इसलिए नाट्य को ही उन्होंने काव्यस्थानीय बनाया है । वे जब-जब ललितगोष्ठी या नृत्यगोष्ठी की चर्चा करते हैं, उसमें नाट्य के प्रसंग का उल्लेख अवश्य करते हैं । भारतीय धारणा के अनुसार, जिस प्रकार चित्रकला और मूर्त्तिकला स्थापत्य की अंगीभूत कलाएँ हैं, उसी प्रकार नृत्य और संगीत-कलाएँ नाट्यकला की सहयोगिनी हैं। विभिन्न कलाकृतियाँ जीवन के जिन विभिन्न स्थितियों और मूल्यों की अभिव्यंजना करती हैं, नाट्य में उनका प्रदर्शन ततोऽधिक सफलतापूर्वक होता है । क्योंकि, नाटक का आस्वाद नेत्रों और कानों द्वारा प्राप्त किया जाता है। इन्हीं दोनों ज्ञानेन्द्रियों के लिए ही नाटक अधिक रुचिकर होता है; क्योंकि रसानुभूति के लिए ये दोनों ज्ञानेन्द्रियाँ ही सर्वाधिक उपयुक्त हैं।
नृत्य की परम्परा ऋग्वेद काल से ही प्रचलित है। ऋग्वेद के युग में स्त्री-पुरुष दोनों नृत्य करते थे। वंशयष्टि को ऊपर आकाश की ओर उठाकर नृत्य करते हुए स्त्री-पुरुषों का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है । ' नाचनेवाले पुरुषों को 'नृत' और नाचनेवाली स्त्रियों को 'नृतु' कहा जाता था । 'नृतु' शब्द कदाचित् उस नृत्यजीवी नारी के लिए प्रयुक्त होता था, जो नृत्य के समय कढ़े हुए वस्त्रों को धारण करती थी और लोगों को आकृष्ट करने के लिए अपने स्तनों को नग्न कर देती थी। युद्ध के अवसर पर उत्तेजित होने की स्थिति में इन्द्र नृत्य करते थे । ऋग्वेद में एक
१. ऋग्वेद,१.१९.१
२. अधि पेशांसि वपते नृतुरिवापोर्णुते वक्ष उस्रेव वर्जहम्
I
ज्योतिर्विश्वस्मै भुवनाय कृण्वती गावो न व्रजं व्युषा आवर्त्तमः ॥ ऋग्वेद, १९२.४