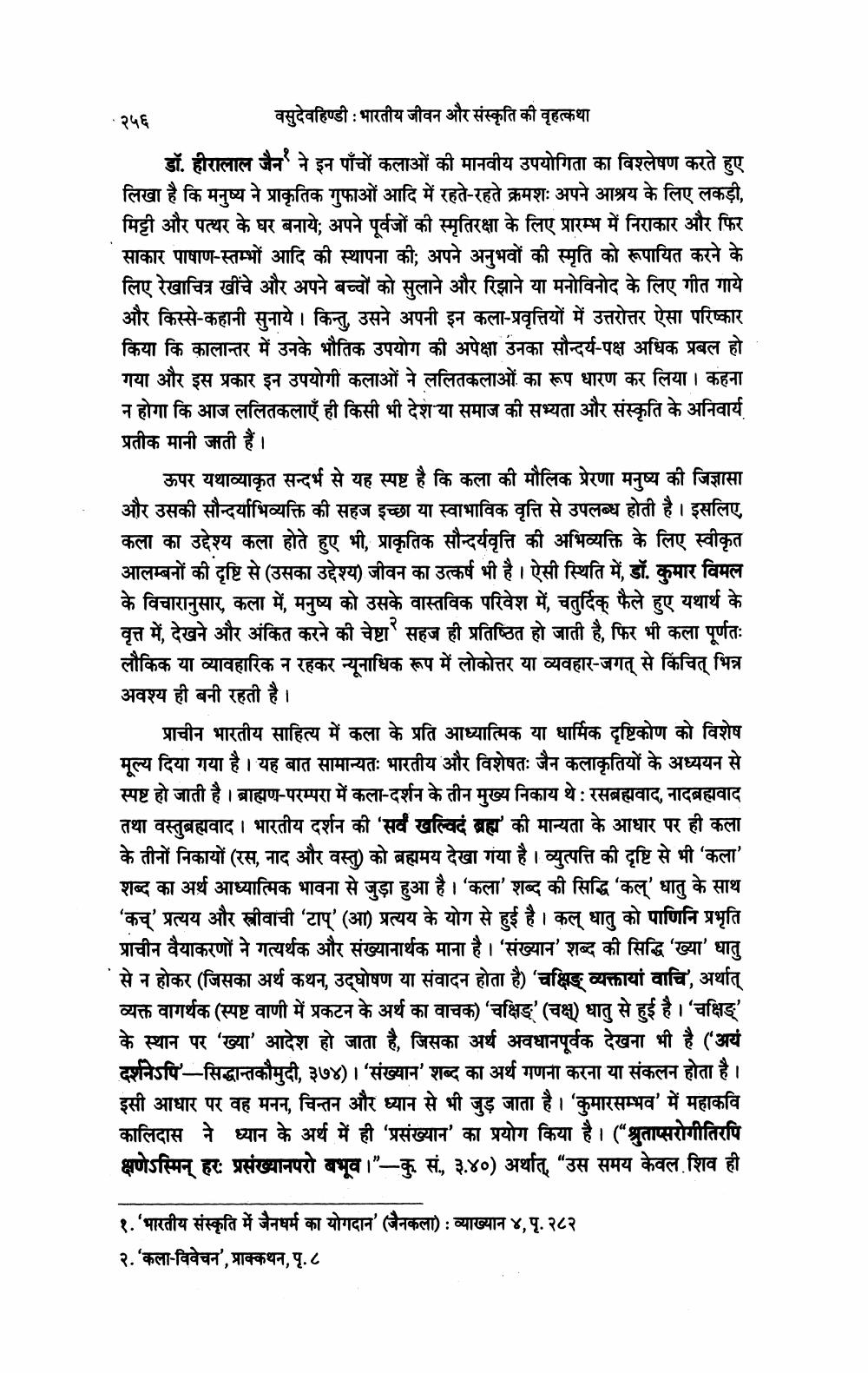________________
• २५६
वसुदेवहिण्डी : भारतीय जीवन और संस्कृति की वृहत्कथा ___ डॉ. हीरालाल जैन ने इन पाँचों कलाओं की मानवीय उपयोगिता का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि मनुष्य ने प्राकृतिक गुफाओं आदि में रहते-रहते क्रमशः अपने आश्रय के लिए लकड़ी, मिट्टी और पत्थर के घर बनाये; अपने पूर्वजों की स्मृतिरक्षा के लिए प्रारम्भ में निराकार और फिर साकार पाषाण-स्तम्भों आदि की स्थापना की; अपने अनुभवों की स्मृति को रूपायित करने के लिए रेखाचित्र खींचे और अपने बच्चों को सुलाने और रिझाने या मनोविनोद के लिए गीत गाये
और किस्से-कहानी सुनाये। किन्तु, उसने अपनी इन कला-प्रवृत्तियों में उत्तरोत्तर ऐसा परिष्कार किया कि कालान्तर में उनके भौतिक उपयोग की अपेक्षा उनका सौन्दर्य-पक्ष अधिक प्रबल हो गया और इस प्रकार इन उपयोगी कलाओं ने ललितकलाओं का रूप धारण कर लिया। कहना न होगा कि आज ललितकलाएँ ही किसी भी देश या समाज की सभ्यता और संस्कृति के अनिवार्य प्रतीक मानी जाती हैं। __ऊपर यथाव्याकृत सन्दर्भ से यह स्पष्ट है कि कला की मौलिक प्रेरणा मनुष्य की जिज्ञासा और उसकी सौन्दर्याभिव्यक्ति की सहज इच्छा या स्वाभाविक वृत्ति से उपलब्ध होती है। इसलिए, कला का उद्देश्य कला होते हुए भी, प्राकृतिक सौन्दर्यवृत्ति की अभिव्यक्ति के लिए स्वीकृत आलम्बनों की दृष्टि से (उसका उद्देश्य) जीवन का उत्कर्ष भी है। ऐसी स्थिति में, डॉ. कुमार विमल के विचारानुसार, कला में, मनुष्य को उसके वास्तविक परिवेश में, चतुर्दिक फैले हुए यथार्थ के वृत्त में, देखने और अंकित करने की चेष्टा सहज ही प्रतिष्ठित हो जाती है, फिर भी कला पूर्णतः लौकिक या व्यावहारिक न रहकर न्यूनाधिक रूप में लोकोत्तर या व्यवहार-जगत् से किंचित् भिन्न अवश्य ही बनी रहती है।
प्राचीन भारतीय साहित्य में कला के प्रति आध्यात्मिक या धार्मिक दृष्टिकोण को विशेष मूल्य दिया गया है। यह बात सामान्यतः भारतीय और विशेषतः जैन कलाकृतियों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाती है। ब्राह्मण-परम्परा में कला-दर्शन के तीन मुख्य निकाय थे : रसब्रह्मवाद, नादब्रह्मवाद तथा वस्तुब्रह्मवाद । भारतीय दर्शन की ‘सर्वं खल्विदं ब्रह्म की मान्यता के आधार पर ही कला के तीनों निकायों (रस, नाद और वस्तु) को ब्रह्ममय देखा गया है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से भी 'कला' शब्द का अर्थ आध्यात्मिक भावना से जुड़ा हुआ है। 'कला' शब्द की सिद्धि 'कल्' धातु के साथ 'कच्' प्रत्यय और स्त्रीवाची 'टाप्' (आ) प्रत्यय के योग से हुई है। कल् धातु को पाणिनि प्रभृति प्राचीन वैयाकरणों ने गत्यर्थक और संख्यानार्थक माना है। 'संख्यान' शब्द की सिद्धि 'ख्या' धातु से न होकर (जिसका अर्थ कथन, उद्घोषण या संवादन होता है) 'चक्षिा व्यक्तायां वाचि', अर्थात् व्यक्त वागर्थक (स्पष्ट वाणी में प्रकटन के अर्थ का वाचक) 'चक्षिङ्' (चक्ष्) धातु से हुई है। 'चक्षिङ्' के स्थान पर 'ख्या' आदेश हो जाता है, जिसका अर्थ अवधानपूर्वक देखना भी है ('अयं दर्शनेऽपि'-सिद्धान्तकौमुदी, ३७४) । 'संख्यान' शब्द का अर्थ गणना करना या संकलन होता है। इसी आधार पर वह मनन, चिन्तन और ध्यान से भी जुड़ जाता है। 'कुमारसम्भव' में महाकवि कालिदास ने ध्यान के अर्थ में ही 'प्रसंख्यान' का प्रयोग किया है। ("श्रुताप्सरोगीतिरपि क्षणेऽस्मिन् हरः प्रसंख्यानपरो बभूव।"-कु सं., ३.४०) अर्थात्, “उस समय केवल शिव ही
१. भारतीय संस्कृति में जैनधर्म का योगदान' (जैनकला) : व्याख्यान ४, पृ. २८२ २. कला-विवेचन',प्राक्कथन, पृ.८