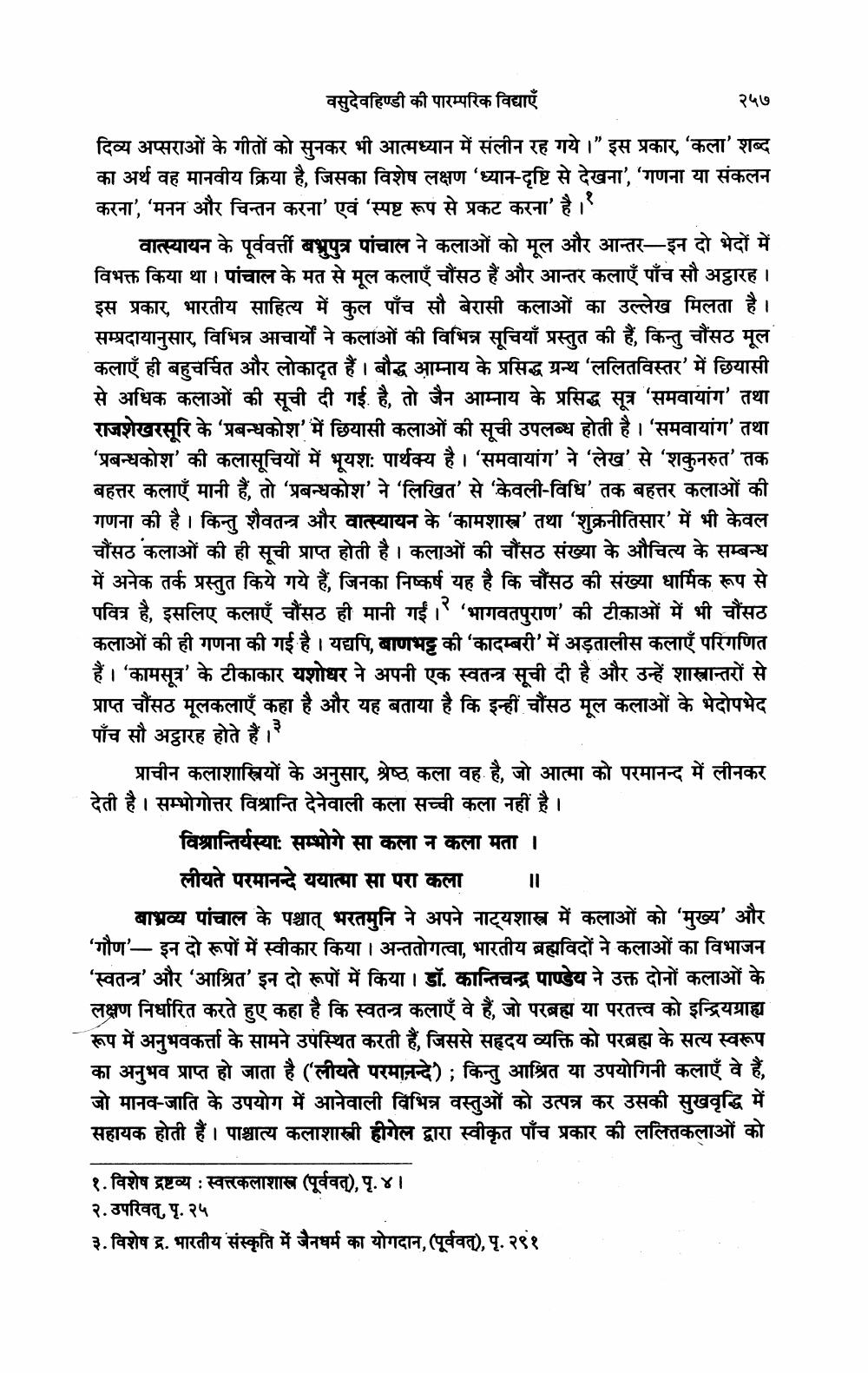________________
वसुदेवहिण्डी की पारम्परिक विद्याएँ
२५७
दिव्य अप्सराओं के गीतों को सुनकर भी आत्मध्यान में संलीन रह गये ।" इस प्रकार, 'कला' शब्द का अर्थ वह मानवीय क्रिया है, जिसका विशेष लक्षण 'ध्यान- दृष्टि से देखना', 'गणना या संकलन करना', 'मनन और चिन्तन करना' एवं 'स्पष्ट रूप से प्रकट करना है । '
वात्स्यायन के पूर्ववर्ती बभ्रुपुत्र पांचाल ने कलाओं को मूल और आन्तर- इन दो भेदों में विभक्त किया था । पांचाल के मत से मूल कलाएँ चौंसठ हैं और आन्तर कलाएँ पाँच सौ अट्ठारह । इस प्रकार, भारतीय साहित्य में कुल पाँच सौ बेरासी कलाओं का उल्लेख मिलता है । सम्प्रदायानुसार, विभिन्न आचार्यों ने कलाओं की विभिन्न सूचियाँ प्रस्तुत की हैं, किन्तु चौंसठ मूल कलाएँ ही बहुचर्चित और लोकादृत हैं। बौद्ध आम्नाय के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'ललितविस्तर' में छियासी से अधिक कलाओं की सूची दी गई है, तो जैन आम्नाय के प्रसिद्ध सूत्र 'समवायांग' तथा राजशेखरसूरि के 'प्रबन्धकोश' में छियासी कलाओं की सूची उपलब्ध होती है । 'समवायांग' तथा 'प्रबन्धकोश' की कलासूचियों में भूयशः पार्थक्य है । 'समवायांग' ने 'लेख' से 'शकुनरुत' तक बहत्तर कलाएँ मानी हैं, तो 'प्रबन्धकोश' ने 'लिखित' से 'केवली - विधि' तक बहत्तर कलाओं की गणना की है। किन्तु शैवतन्त्र और वात्स्यायन के 'कामशास्त्र' तथा 'शुक्रनीतिसार' में भी केवल चौंसठ कलाओं की ही सूची प्राप्त होती । कलाओं की चौंसठ संख्या के औचित्य के सम्बन्ध में अनेक तर्क प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका निष्कर्ष यह है कि चौंसठ की संख्या धार्मिक रूप से पवित्र है, इसलिए कलाएँ चौंसठ ही मानी गईं । 'भागवतपुराण' की टीकाओं में भी चौंसठ कलाओं की ही गणना की गई है। यद्यपि, बाणभट्ट की 'कादम्बरी' में अड़तालीस कलाएँ परिगणित हैं । 'कामसूत्र' के टीकाकार यशोधर ने अपनी एक स्वतन्त्र सूची दी है और उन्हें शास्त्रान्तरों से प्राप्त चौंसठ मूलकलाएँ कहा है और यह बताया है कि इन्हीं चौंसठ मूल कलाओं के भेदोपभेद पाँच सौ अट्ठारह होते हैं । ३
प्राचीन कलाशास्त्रियों के अनुसार, श्रेष्ठ कला वह है, जो आत्मा को परमानन्द में लीनकर देती है । सम्भोगोत्तर विश्रान्ति देनेवाली कला सच्ची कला नहीं है ।
विश्रान्तिर्यस्याः सम्भोगे सा कला न कला मता ।
लीयते परमानन्दे ययात्मा सा परा कला
||
बाभ्रव्य पांचाल के पश्चात् भरतमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में कलाओं को 'मुख्य' और 'गौण'- इन दो रूपों में स्वीकार किया । अन्ततोगत्वा, भारतीय ब्रह्मविदों ने कलाओं का विभाजन 'स्वतन्त्र' और 'आश्रित' इन दो रूपों में किया। डॉ. कान्तिचन्द्र पाण्डेय ने उक्त दोनों कलाओं के लक्षण निर्धारित करते हुए कहा है कि स्वतन्त्र कलाएँ वे हैं, जो परब्रह्म या परतत्त्व को इन्द्रियग्राह्य रूप में अनुभवकर्ता के सामने उपस्थित करती हैं, जिससे सहृदय व्यक्ति को परब्रह्म के सत्य स्वरूप का अनुभव प्राप्त हो जाता है ('लीयते परमानन्दे ) ; किन्तु आश्रित या उपयोगिनी कलाएँ वे हैं, जो मानव-जाति के उपयोग में आनेवाली विभिन्न वस्तुओं को उत्पन्न कर उसकी सुखवृद्धि में सहायक होती हैं । पाश्चात्य कलाशास्त्री हीगेल द्वारा स्वीकृत पाँच प्रकार की ललितकलाओं को
१. विशेष द्रष्टव्य : स्वत्त्कलाशास्त्र (पूर्ववत्), पृ. ४ ।
२. उपरिवत्, पृ. २५
३. विशेष द्र. भारतीय संस्कृति में जैनधर्म का योगदान, (पूर्ववत्, पृ. २९१