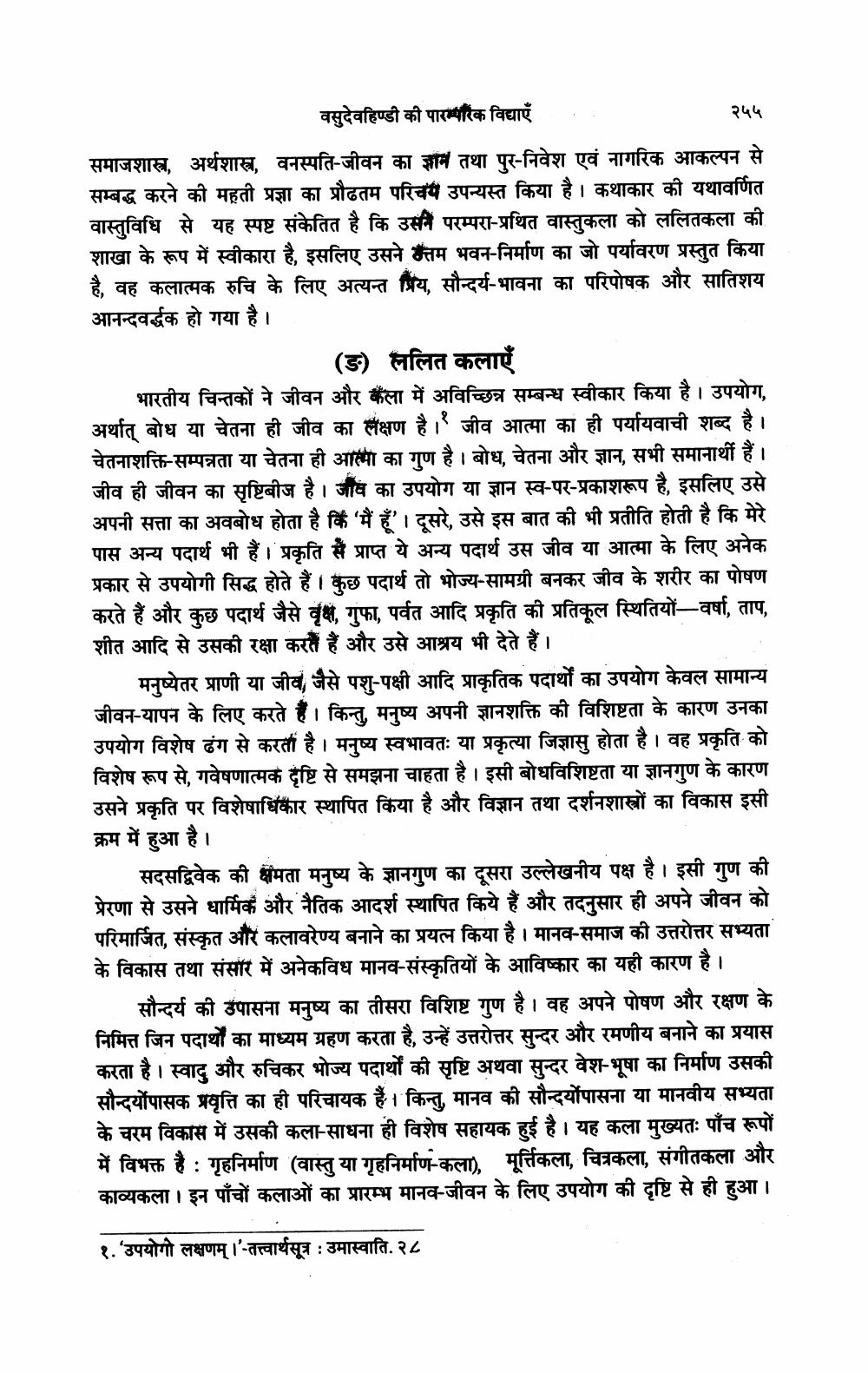________________
वसुदेवहिण्डी की पारम्परिक विद्याएँ
२५५
समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, वनस्पति-जीवन का ज्ञान तथा पुर-निवेश एवं नागरिक आकल्पन से सम्बद्ध करने की महती प्रज्ञा का प्रौढतम परिचय उपन्यस्त किया है। कथाकार की यथावर्णित वास्तुविधि से यह स्पष्ट संकेतित है कि उसने परम्परा-प्रथित वास्तुकला को ललितकला की शाखा के रूप में स्वीकारा है, इसलिए उसने स्तम भवन-निर्माण का जो पर्यावरण प्रस्तुत किया है, वह कलात्मक रुचि के लिए अत्यन्त प्रिय, सौन्दर्य-भावना का परिपोषक और सातिशय आनन्दवर्द्धक हो गया है।
(ङ) ललित कलाएँ भारतीय चिन्तकों ने जीवन और कला में अविच्छिन्न सम्बन्ध स्वीकार किया है। उपयोग, अर्थात् बोध या चेतना ही जीव का लक्षण है।' जीव आत्मा का ही पर्यायवाची शब्द है। चेतनाशक्ति-सम्पन्नता या चेतना ही आत्मा का गुण है। बोध, चेतना और ज्ञान, सभी समानार्थी हैं। जीव ही जीवन का सृष्टिबीज है। जीव का उपयोग या ज्ञान स्व-पर-प्रकाशरूप है, इसलिए उसे अपनी सत्ता का अवबोध होता है कि 'मैं हूँ'। दूसरे, उसे इस बात की भी प्रतीति होती है कि मेरे पास अन्य पदार्थ भी हैं। प्रकृति से प्राप्त ये अन्य पदार्थ उस जीव या आत्मा के लिए अनेक प्रकार से उपयोगी सिद्ध होते हैं । कुछ पदार्थ तो भोज्य-सामग्री बनकर जीव के शरीर का पोषण करते हैं और कुछ पदार्थ जैसे वृक्ष, गुफा, पर्वत आदि प्रकृति की प्रतिकूल स्थितियों-वर्षा, ताप, शीत आदि से उसकी रक्षा करते हैं और उसे आश्रय भी देते हैं।
मनुष्येतर प्राणी या जीव, जैसे पशु-पक्षी आदि प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग केवल सामान्य जीवन-यापन के लिए करते हैं। किन्तु, मनुष्य अपनी ज्ञानशक्ति की विशिष्टता के कारण उनका उपयोग विशेष ढंग से करती है। मनुष्य स्वभावतः या प्रकृत्या जिज्ञासु होता है। वह प्रकृति को विशेष रूप से, गवेषणात्मक दृष्टि से समझना चाहता है। इसी बोधविशिष्टता या ज्ञानगुण के कारण उसने प्रकृति पर विशेषाधिकार स्थापित किया है और विज्ञान तथा दर्शनशास्त्रों का विकास इसी क्रम में हुआ है।
सदसद्विवेक की क्षमता मनुष्य के ज्ञानगुण का दूसरा उल्लेखनीय पक्ष है। इसी गुण की प्रेरणा से उसने धार्मिक और नैतिक आदर्श स्थापित किये हैं और तदनुसार ही अपने जीवन को परिमार्जित, संस्कृत और कलावरेण्य बनाने का प्रयत्न किया है। मानव-समाज की उत्तरोत्तर सभ्यता के विकास तथा संसार में अनेकविध मानव-संस्कतियों के आविष्कार का यही कारण है। ___सौन्दर्य की उपासना मनुष्य का तीसरा विशिष्ट गुण है। वह अपने पोषण और रक्षण के निमित्त जिन पदार्थों का माध्यम ग्रहण करता है, उन्हें उत्तरोत्तर सुन्दर और रमणीय बनाने का प्रयास करता है। स्वादु और रुचिकर भोज्य पदार्थों की सृष्टि अथवा सुन्दर वेश-भूषा का निर्माण उसकी सौन्दर्योपासक प्रवृत्ति का ही परिचायक हैं। किन्तु मानव की सौन्दर्योपासना या मानवीय सभ्यता के चरम विकास में उसकी कला-साधना ही विशेष सहायक हुई है। यह कला मुख्यतः पाँच रूपों में विभक्त है : गृहनिर्माण (वास्तु या गृहनिर्माण कला), मूर्तिकला, चित्रकला, संगीतकला और काव्यकला। इन पाँचों कलाओं का प्रारम्भ मानव-जीवन के लिए उपयोग की दृष्टि से ही हुआ।
१. उपयोगो लक्षणम्।'-तत्त्वार्थसूत्र : उमास्वाति. २८