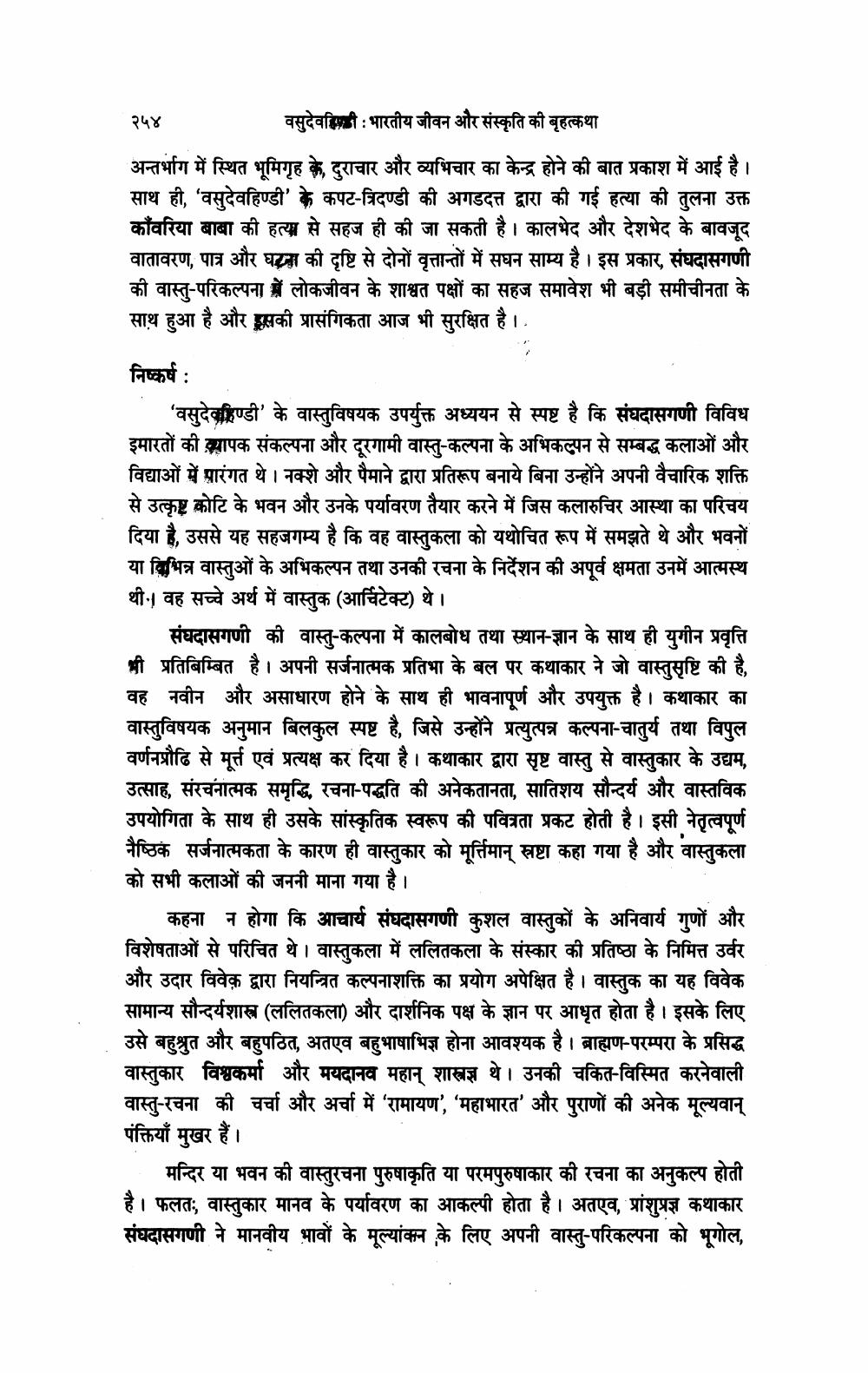________________
२५४
वसुदेवसिडी : भारतीय जीवन और संस्कृति की बृहत्कथा अन्तर्भाग में स्थित भूमिगृह के, दुराचार और व्यभिचार का केन्द्र होने की बात प्रकाश में आई है। साथ ही, 'वसुदेवहिण्डी' के कपट-त्रिदण्डी की अगडदत्त द्वारा की गई हत्या की तुलना उक्त काँवरिया बाबा की हत्या से सहज ही की जा सकती है। कालभेद और देशभेद के बावजूद वातावरण, पात्र और घटना की दृष्टि से दोनों वृत्तान्तों में सघन साम्य है। इस प्रकार, संघदासगणी की वास्तु-परिकल्पना में लोकजीवन के शाश्वत पक्षों का सहज समावेश भी बड़ी समीचीनता के साथ हुआ है और इसकी प्रासंगिकता आज भी सुरक्षित है। .
निष्कर्ष : ___'वसुदेवहिण्डी' के वास्तुविषयक उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि संघदासगणी विविध इमारतों की व्यापक संकल्पना और दूरगामी वास्तु-कल्पना के अभिकल्पन से सम्बद्ध कलाओं और विद्याओं में पारंगत थे। नक्शे और पैमाने द्वारा प्रतिरूप बनाये बिना उन्होंने अपनी वैचारिक शक्ति से उत्कृष्ट कोटि के भवन और उनके पर्यावरण तैयार करने में जिस कलारुचिर आस्था का परिचय दिया है, उससे यह सहजगम्य है कि वह वास्तुकला को यथोचित रूप में समझते थे और भवनों या विभिन्न वास्तुओं के अभिकल्पन तथा उनकी रचना के निर्देशन की अपूर्व क्षमता उनमें आत्मस्थ थी। वह सच्चे अर्थ में वास्तुक (आचिंटेक्ट) थे।
संघदासगणी की वास्तु-कल्पना में कालबोध तथा स्थान-ज्ञान के साथ ही युगीन प्रवृत्ति श्री प्रतिबिम्बित है। अपनी सर्जनात्मक प्रतिभा के बल पर कथाकार ने जो वास्तुसृष्टि की है, वह नवीन और असाधारण होने के साथ ही भावनापूर्ण और उपयुक्त है। कथाकार का वास्तुविषयक अनुमान बिलकुल स्पष्ट है, जिसे उन्होंने प्रत्युत्पन्न कल्पना-चातुर्य तथा विपुल वर्णनप्रौढि से मूर्त एवं प्रत्यक्ष कर दिया है। कथाकार द्वारा सृष्ट वास्तु से वास्तुकार के उद्यम, उत्साह, संरचनात्मक समृद्धि, रचना-पद्धति की अनेकतानता, सातिशय सौन्दर्य और वास्तविक उपयोगिता के साथ ही उसके सांस्कृतिक स्वरूप की पवित्रता प्रकट होती है। इसी नेतृत्वपूर्ण नैष्ठिक सर्जनात्मकता के कारण ही वास्तुकार को मूर्तिमान् स्रष्टा कहा गया है और वास्तुकला को सभी कलाओं की जननी माना गया है।
कहना न होगा कि आचार्य संघदासगणी कुशल वास्तुकों के अनिवार्य गुणों और विशेषताओं से परिचित थे। वास्तुकला में ललितकला के संस्कार की प्रतिष्ठा के निमित्त उर्वर
और उदार विवेक द्वारा नियन्त्रित कल्पनाशक्ति का प्रयोग अपेक्षित है। वास्तुक का यह विवेक सामान्य सौन्दर्यशास्त्र (ललितकला) और दार्शनिक पक्ष के ज्ञान पर आधृत होता है। इसके लिए उसे बहुश्रुत और बहुपठित, अतएव बहुभाषाभिज्ञ होना आवश्यक है। ब्राह्मण-परम्परा के प्रसिद्ध वास्तुकार विश्वकर्मा और मयदानव महान् शास्त्रज्ञ थे। उनकी चकित-विस्मित करनेवाली वास्तु-रचना की चर्चा और अर्चा में 'रामायण', 'महाभारत' और पुराणों की अनेक मूल्यवान् पंक्तियाँ मुखर हैं।
मन्दिर या भवन की वास्तुरचना पुरुषाकृति या परमपुरुषाकार की रचना का अनुकल्प होती है। फलतः, वास्तुकार मानव के पर्यावरण का आकल्पी होता है। अतएव, प्रांशुप्रज्ञ कथाकार संघदासगणी ने मानवीय भावों के मूल्यांकन के लिए अपनी वास्तु-परिकल्पना को भूगोल,