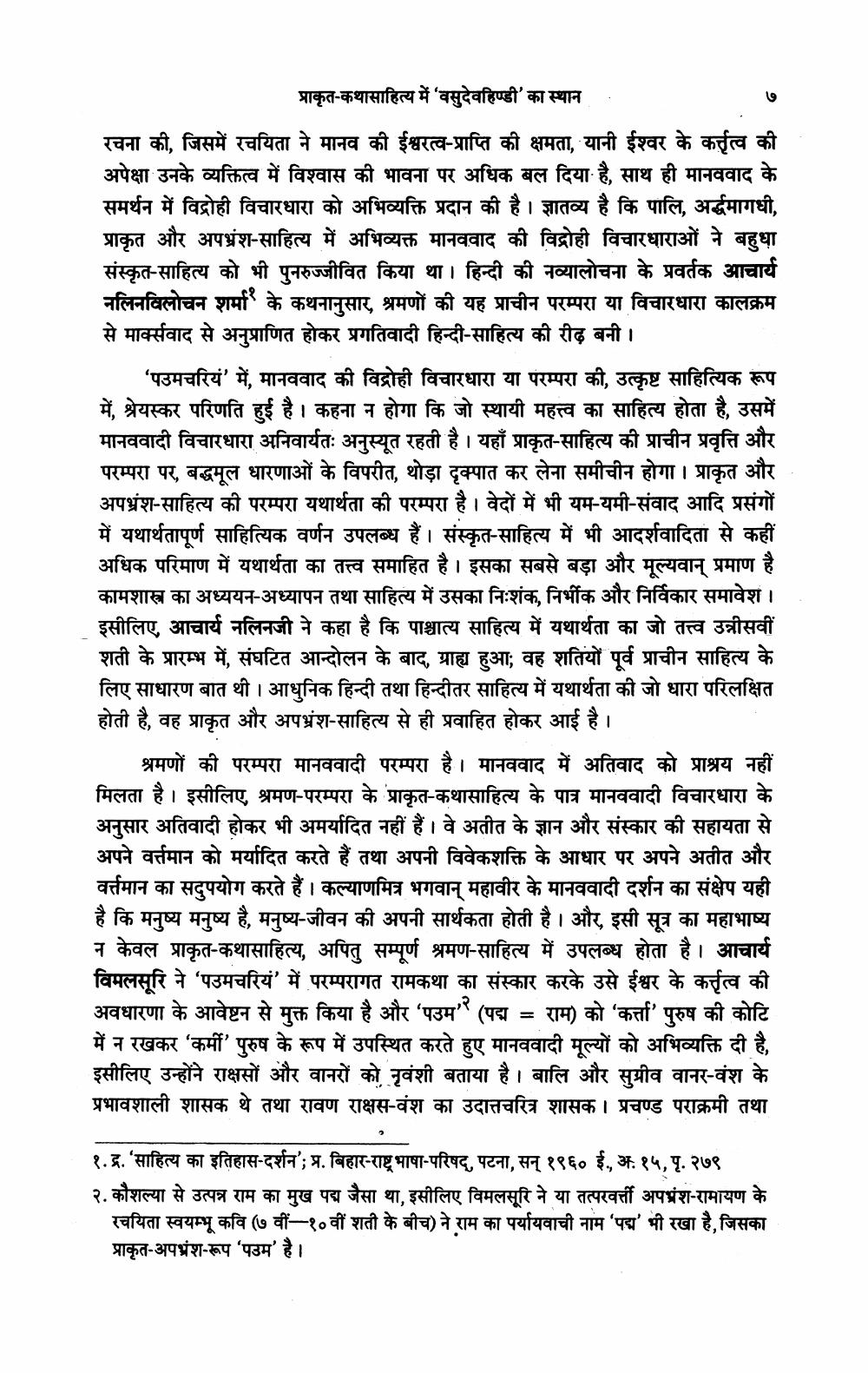________________
प्राकृत-कथासाहित्य में 'वसुदेवहिण्डी' का स्थान
रचना की, जिसमें रचयिता ने मानव की ईश्वरत्व - प्राप्ति की क्षमता, यानी ईश्वर के कर्तृत्व की अपेक्षा उनके व्यक्तित्व में विश्वास की भावना पर अधिक बल दिया है, साथ ही मानववाद के समर्थन में विद्रोही विचारधारा को अभिव्यक्ति प्रदान की है । ज्ञातव्य है कि पालि, अर्द्धमागधी, प्राकृत और अपभ्रंश-साहित्य में अभिव्यक्त मानववाद की विद्रोही विचारधाराओं ने बहुधा संस्कृत-साहित्य को भी पुनरुज्जीवित किया था । हिन्दी की नव्यालोचना के प्रवर्तक आचार्य नलिनविलोचन शर्मा' के कथनानुसार, श्रमणों की यह प्राचीन परम्परा या विचारधारा कालक्रम से मार्क्सवाद से अनुप्राणित होकर प्रगतिवादी हिन्दी - साहित्य की रीढ़ बनी ।
'पउमचरियं' में, मानववाद की विद्रोही विचारधारा या परम्परा की, उत्कृष्ट साहित्यिक रूप में, श्रेयस्कर परिणति हुई है। कहना न होगा कि जो स्थायी महत्त्व का साहित्य होता है, उसमें मानववादी विचारधारा अनिवार्यतः अनुस्यूत रहती है। यहाँ प्राकृत-साहित्य की प्राचीन प्रवृत्ति और परम्परा पर, बद्धमूल धारणाओं के विपरीत, थोड़ा दृक्पात कर लेना समीचीन होगा । प्राकृत और अपभ्रंश-साहित्य की परम्परा यथार्थता की परम्परा है। वेदों में भी यम-यमी - संवाद आदि प्रसंगों में यथार्थतापूर्ण साहित्यिक वर्णन उपलब्ध हैं। संस्कृत - साहित्य में भी आदर्शवादिता से कहीं अधिक परिमाण में यथार्थता का तत्त्व समाहित है । इसका सबसे बड़ा और मूल्यवान् प्रमाण है कामशास्त्र का अध्ययन-अध्यापन तथा साहित्य में उसका निःशंक, निर्भीक और निर्विकार समावेश । इसीलिए, आचार्य नलिनजी ने कहा है कि पाश्चात्य साहित्य में यथार्थता का जो तत्त्व उन्नीसवीं शती के प्रारम्भ में, संघटित आन्दोलन के बाद ग्राह्य हुआ; वह शतियों पूर्व प्राचीन साहित्य के लिए साधारण बात थी । आधुनिक हिन्दी तथा हिन्दीतर साहित्य में यथार्थता की जो धारा परिलक्षित होती है, वह प्राकृत और अपभ्रंश - साहित्य से ही प्रवाहित होकर आई है ।
श्रमणों की परम्परा मानववादी परम्परा है। मानववाद में अतिवाद को प्राश्रय नहीं मिलता है। इसीलिए, श्रमण- परम्परा के प्राकृत - कथासाहित्य के पात्र मानववादी विचारधारा के अनुसार अतिवादी होकर भी अमर्यादित नहीं हैं । वे अतीत के ज्ञान और संस्कार की सहायता से अपने वर्तमान को मर्यादित करते हैं तथा अपनी विवेकशक्ति के आधार पर अपने अतीत और वर्त्तमान का सदुपयोग करते हैं । कल्याणमित्र भगवान् महावीर के मानववादी दर्शन का संक्षेप यही है कि मनुष्य मनुष्य है, मनुष्य-जीवन की अपनी सार्थकता होती है । और, इसी सूत्र का महाभाष्य न केवल प्राकृत-कथासाहित्य, अपितु सम्पूर्ण श्रमण- साहित्य में उपलब्ध होता है। आचार्य विमलसूरि ने 'पउमचरियं' में परम्परागत रामकथा का संस्कार करके उसे ईश्वर के कर्तृत्व की अवधारणा के आवेष्टन से मुक्त किया है और 'पउम ? (पद्म राम) को 'कर्ता' पुरुष की कोटि में न रखकर 'कर्मी' पुरुष के रूप में उपस्थित करते हुए मानववादी मूल्यों को अभिव्यक्ति दी है, इसीलिए उन्होंने राक्षसों और वानरों को नृवंशी बताया है। बालि और सुग्रीव वानर-वंश के प्रभावशाली शासक थे तथा रावण राक्षस- वंश का उदात्तचरित्र शासक । प्रचण्ड पराक्रमी तथा
--
१. द्र. 'साहित्य का इतिहास-दर्शन'; प्र. बिहार- राष्ट्र भाषा-परिषद्, पटना, सन् १९६० ई., अ. १५, पृ. २७९ २. कौशल्या से उत्पन्न राम का मुख पद्म जैसा था, इसीलिए विमलसूरि ने या तत्परवर्त्ती अपभ्रंश- रामायण के रचयिता स्वयम्भू कवि (७ वीं - १०वीं शती के बीच) ने राम का पर्यायवाची नाम 'पद्म' भी रखा है, जिसका प्राकृत- अपभ्रंश रूप 'पउम' है।