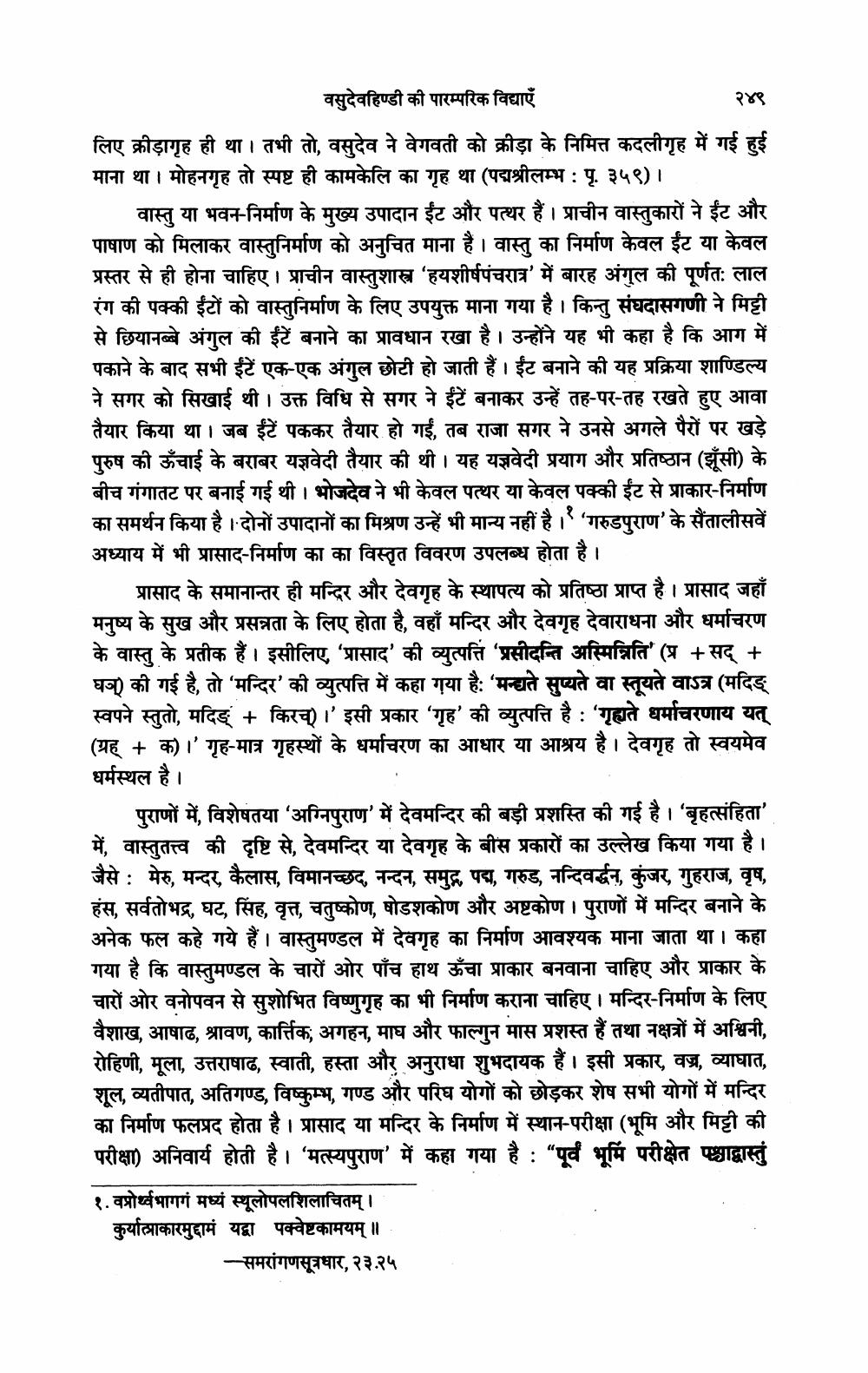________________
वसुदेवहिण्डी की पारम्परिक विद्याएँ
२४९ लिए क्रीड़ागृह ही था। तभी तो, वसुदेव ने वेगवती को क्रीड़ा के निमित्त कदलीगृह में गई हुई माना था। मोहनगृह तो स्पष्ट ही कामकेलि का गृह था (पद्यश्रीलम्भ : पृ. ३५९)।
वास्तु या भवन निर्माण के मुख्य उपादान ईंट और पत्थर हैं। प्राचीन वास्तुकारों ने ईंट और पाषाण को मिलाकर वास्तुनिर्माण को अनुचित माना है। वास्तु का निर्माण केवल ईंट या केवल प्रस्तर से ही होना चाहिए। प्राचीन वास्तुशास्त्र ‘हयशीर्षपंचरात्र' में बारह अंगुल की पूर्णत: लाल रंग की पक्की ईंटों को वास्तुनिर्माण के लिए उपयुक्त माना गया है। किन्तु संघदासगणी ने मिट्टी से छियानब्बे अंगुल की ईंटें बनाने का प्रावधान रखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि आग में पकाने के बाद सभी ईंटें एक-एक अंगुल छोटी हो जाती हैं। ईंट बनाने की यह प्रक्रिया शाण्डिल्य ने सगर को सिखाई थी। उक्त विधि से सगर ने ईंटें बनाकर उन्हें तह-पर-तह रखते हुए आवा तैयार किया था। जब ईंटें पककर तैयार हो गईं, तब राजा सगर ने उनसे अगले पैरों पर खड़े पुरुष की ऊँचाई के बराबर यज्ञवेदी तैयार की थी। यह यज्ञवेदी प्रयाग और प्रतिष्ठान (झूसी) के बीच गंगातट पर बनाई गई थी। भोजदेव ने भी केवल पत्थर या केवल पक्की ईंट से प्राकार-निर्माण का समर्थन किया है। दोनों उपादानों का मिश्रण उन्हें भी मान्य नहीं है। 'गरुडपुराण' के सैंतालीसवें अध्याय में भी प्रासाद-निर्माण का का विस्तृत विवरण उपलब्ध होता है।
प्रासाद के समानान्तर ही मन्दिर और देवगृह के स्थापत्य को प्रतिष्ठा प्राप्त है। प्रासाद जहाँ मनुष्य के सुख और प्रसन्नता के लिए होता है, वहाँ मन्दिर और देवगृह देवाराधना और धर्माचरण के वास्तु के प्रतीक हैं। इसीलिए, 'प्रासाद' की व्युत्पत्तिं 'प्रसीदन्ति अस्मिन्निति' (प्र + सद् + घ) की गई है, तो 'मन्दिर' की व्युत्पत्ति में कहा गया है: 'मन्द्यते सुप्यते वा स्तूयते वाऽत्र (मदिङ् स्वपने स्तुतो, मदिङ् + किरच्)।' इसी प्रकार 'गृह' की व्युत्पत्ति है : 'गृह्यते धर्माचरणाय यत् (ग्रह् + क)।' गृह-मात्र गृहस्थों के धर्माचरण का आधार या आश्रय है। देवगृह तो स्वयमेव धर्मस्थल है।
पुराणों में, विशेषतया 'अग्निपुराण' में देवमन्दिर की बड़ी प्रशस्ति की गई है। 'बृहत्संहिता' में, वास्तुतत्त्व की दृष्टि से, देवमन्दिर या देवगृह के बीस प्रकारों का उल्लेख किया गया है।
जैसे : मेरु, मन्दर, कैलास, विमानच्छद, नन्दन, समुद्ग, पदा, गरुड, नन्दिवर्द्धन, कुंजर, गुहराज, वृष, हंस, सर्वतोभद्र, घट, सिंह, वृत्त, चतुष्कोण, षोडशकोण और अष्टकोण । पुराणों में मन्दिर बनाने के अनेक फल कहे गये हैं। वास्तुमण्डल में देवगृह का निर्माण आवश्यक माना जाता था। कहा गया है कि वास्तुमण्डल के चारों ओर पाँच हाथ ऊँचा प्राकार बनवाना चाहिए और प्राकार के चारों ओर वनोपवन से सुशोभित विष्णुगृह का भी निर्माण कराना चाहिए। मन्दिर निर्माण के लिए वैशाख, आषाढ, श्रावण, कार्तिक; अगहन, माघ और फाल्गुन मास प्रशस्त हैं तथा नक्षत्रों में अश्विनी, रोहिणी, मूला, उत्तराषाढ, स्वाती, हस्ता और अनुराधा शुभदायक हैं। इसी प्रकार, वज्र, व्याघात, शूल, व्यतीपात, अतिगण्ड, विष्कुम्भ, गण्ड और परिघ योगों को छोड़कर शेष सभी योगों में मन्दिर का निर्माण फलप्रद होता है। प्रासाद या मन्दिर के निर्माण में स्थान परीक्षा (भूमि और मिट्टी की परीक्षा) अनिवार्य होती है। 'मत्स्यपुराण' में कहा गया है : “पूर्व भूमि परीक्षेत पछाद्वास्तुं १. वपोर्श्वभागगं मध्यं स्थूलोपलशिलाचितम् । कुर्यात्राकारमुद्दामं यद्वा पक्वेष्टकामयम् ॥
-समरांगणसूत्रधार, २३.२५