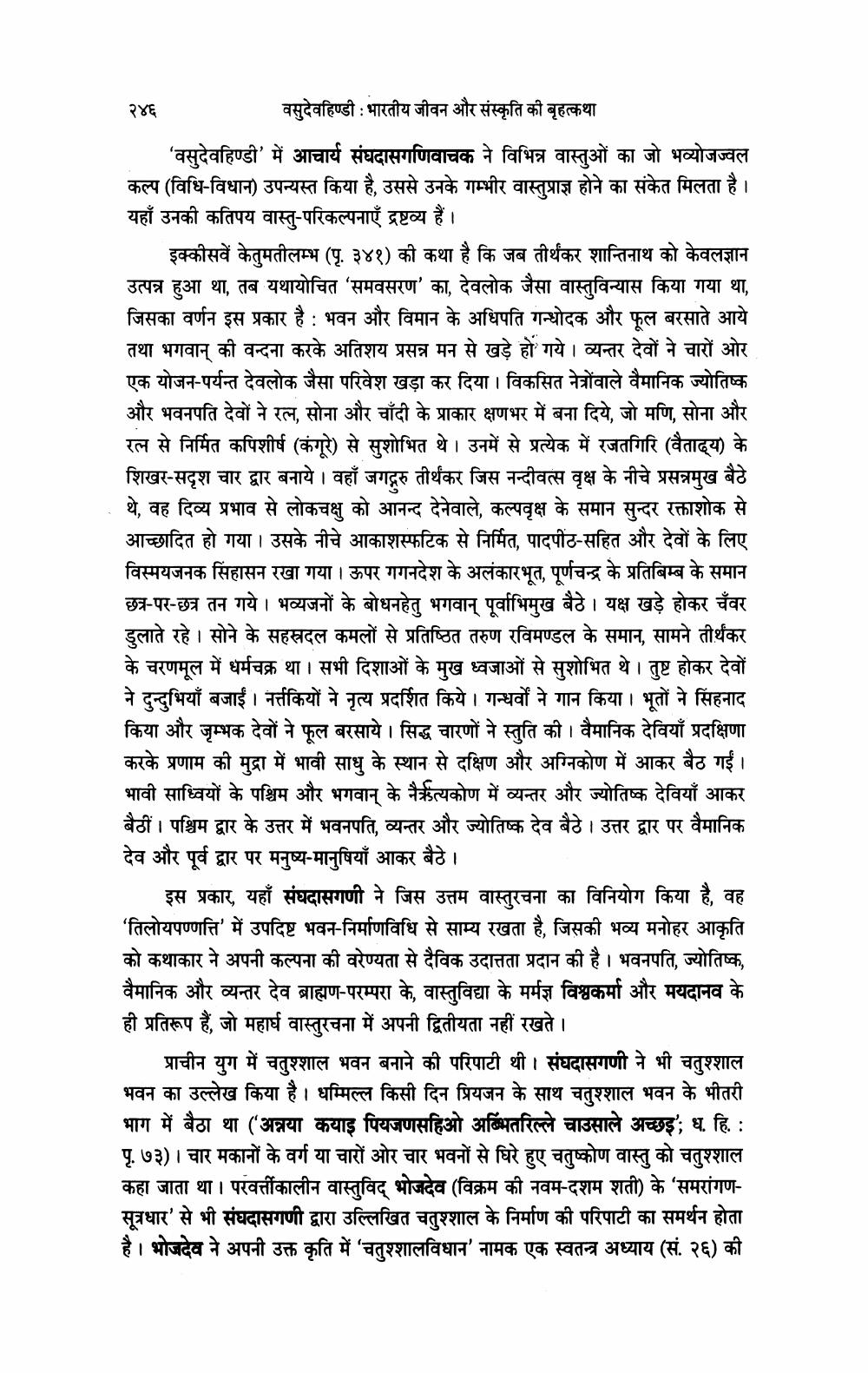________________
वसुदेवहिण्डी : भारतीय जीवन और संस्कृति की बृहत्कथा
‘वसुदेवहिण्डी' में आचार्य संघदासगणिवाचक ने विभिन्न वास्तुओं का जो भव्योजज्वल कल्प (विधि-विधान) उपन्यस्त किया है, उससे उनके गम्भीर वास्तुप्राज्ञ होने का संकेत मिलता है । यहाँ उनकी कतिपय वास्तु- परिकल्पनाएँ द्रष्टव्य हैं ।
२४६
इक्कीसवें केतुमतीलम्भ (पृ. ३४१ ) की कथा है कि जब तीर्थंकर शान्तिनाथ को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था, तब यथायोचित 'समवसरण' का, देवलोक जैसा वास्तुविन्यास किया गया था, जिसका वर्णन इस प्रकार है : भवन और विमान के अधिपति गन्धोदक और फूल बरसाते आये तथा भगवान् की वन्दना करके अतिशय प्रसन्न मन से खड़े हो गये । व्यन्तर देवों ने चारों ओर एक योजन-पर्यन्त देवलोक जैसा परिवेश खड़ा कर दिया। विकसित नेत्रोंवाले वैमानिक ज्योतिष्क और भवनपति देवों ने रत्न, सोना और चाँदी के प्राकार क्षणभर में बना दिये, जो मणि, सोना और रत्न से निर्मित कपिशीर्ष ( कंगूरे) से सुशोभित थे । उनमें से प्रत्येक में रजतगिरि (वैताढ्य ) के शिखर-सदृश चार द्वार बनाये। वहाँ जगद्गुरु तीर्थंकर जिस नन्दीवत्स वृक्ष के नीचे प्रसन्नमुख बैठे थे, वह दिव्य प्रभाव से लोकचक्षु को आनन्द देनेवाले, कल्पवृक्ष के समान सुन्दर रक्ताशोक से आच्छादित हो गया। उसके नीचे आकाशस्फटिक से निर्मित, पादपीठ- सहित और देवों के लिए विस्मयजनक सिंहासन रखा गया। ऊपर गगनदेश के अलंकारभूत, पूर्णचन्द्र के प्रतिबिम्ब के समान छत्र-पर-छत्र तन गये। भव्यजनों के बोधनहेतु भगवान् पूर्वाभिमुख बैठे। यक्ष खड़े होकर चँवर डुलाते रहे। सोने के सहस्त्रदल कमलों से प्रतिष्ठित तरुण रविमण्डल के समान, सामने तीर्थंकर के चरणमूल में धर्मचक्र था। सभी दिशाओं के मुख ध्वजाओं से सुशोभित थे । तुष्ट होकर देवों ने दुन्दुभियाँ बजाईं। नर्त्तकियों ने नृत्य प्रदर्शित किये । गन्धर्वों ने गान किया। भूतों ने सिंहनाद किया और जृम्भक देवों ने फूल बरसाये । सिद्ध चारणों ने स्तुति की। वैमानिक देवियाँ प्रदक्षिणा करके प्रणाम की मुद्रा में भावी साधु के स्थान से दक्षिण और अग्निकोण में आकर बैठ गईं। भावी साध्वियों के पश्चिम और भगवान् के नैर्ऋत्यकोण में व्यन्तर और ज्योतिष्क देवियाँ आ बैठीं । पश्चिम द्वार के उत्तर में भवनपति, व्यन्तर और ज्योतिष्क देव बैठे । उत्तर द्वार पर वैमानिक देव और पूर्व द्वार पर मनुष्य मानुषियाँ आकर बैठे ।
इस प्रकार, यहाँ संघदासगणी ने जिस उत्तम वास्तुरचना का विनियोग किया है, वह ‘तिलोयपण्णत्ति' में उपदिष्ट भवन-निर्माणविधि से साम्य रखता है, जिसकी भव्य मनोहर आकृति को कथाकार ने अपनी कल्पना की वरेण्यता से दैविक उदात्तता प्रदान की है । भवनपति, ज्योतिष्क, वैमानिक और व्यन्तर देव ब्राह्मण-परम्परा के, वास्तुविद्या के मर्मज्ञ विश्वकर्मा और मयदानव के ही प्रतिरूप हैं, जो महार्घ वास्तुरचना में अपनी द्वितीयता नहीं रखते ।
प्राचीन युग में चतुश्शाल भवन बनाने की परिपाटी थी । संघदासगणी ने भी चतुश्शाल भवन का उल्लेख किया है । धम्मिल्ल किसी दिन प्रियजन के साथ चतुश्शाल भवन के भीतरी भाग में बैठा था ('अन्नया कयाइ पियजणसहिओ अब्भितरिल्ले चाउसाले अच्छइ; ध. हि. : पृ. ७३) । चार मकानों के वर्ग या चारों ओर चार भवनों से घिरे हुए चतुष्कोण वास्तु को चतुश्शाल कहा जाता था। परवर्त्तीकालीन वास्तुविद् भोजदेव (विक्रम की नवम-दशम शती) के 'समरांगणसूत्रधार' से भी संघदासगणी द्वारा उल्लिखित चतुश्शाल के निर्माण की परिपाटी का समर्थन होता है। भोजदेव ने अपनी उक्त कृति में 'चतुश्शालविधान' नामक एक स्वतन्त्र अध्याय (सं. २६) की