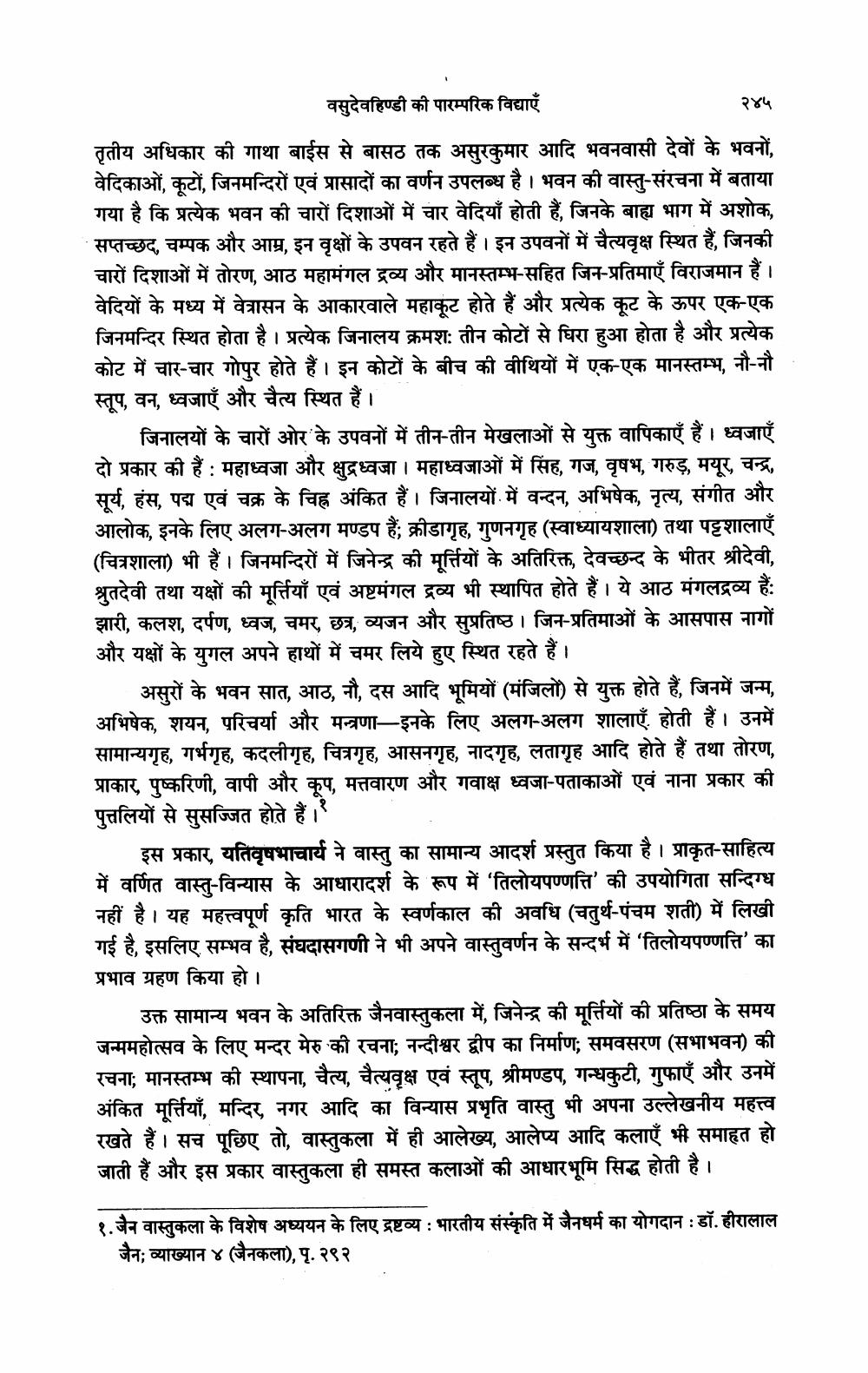________________
वसुदेवहिण्डी की पारम्परिक विद्याएँ
२४५
तृतीय अधिकार की गाथा बाईस से बासठ तक असुरकुमार आदि भवनवासी देवों के भवनों, वेदिकाओं, कूटों, जिनमन्दिरों एवं प्रासादों का वर्णन उपलब्ध है। भवन की वास्तु-संरचना में बताया गया है कि प्रत्येक भवन की चारों दिशाओं में चार वेदियाँ होती हैं, जिनके बाह्य भाग में अशोक, सप्तच्छद, चम्पक और आम्र, इन वृक्षों के उपवन रहते हैं । इन उपवनों में चैत्यवृक्ष स्थित हैं, जिनकी चारों दिशाओं में तोरण, आठ महामंगल द्रव्य और मानस्तम्भ - सहित जिन - प्रतिमाएँ विराजमान हैं । वेदियों के मध्य में वेत्रासन के आकारवाले महाकूट होते हैं और प्रत्येक कूट के ऊपर एक-एक जिनमन्दिर स्थित होता है। प्रत्येक जिनालय क्रमशः तीन कोटों से घिरा हुआ होता है और प्रत्येक कोट में चार-चार गोपुर होते हैं। इन कोटों के बीच की वीथियों में एक-एक मानस्तम्भ, नौ-नौ स्तूप, वन, ध्वजाएँ और चैत्य स्थित हैं ।
जिनालयों के चारों ओर के उपवनों में तीन-तीन मेखलाओं से युक्त वापिकाएँ हैं । ध्वजाएँ दो प्रकार की हैं : महाध्वजा और क्षुद्रध्वजा । महाध्वजाओं में सिंह, गज, वृषभ, गरुड़, मयूर, चन्द्र, सूर्य, हंस, पद्म एवं चक्र के चिह्न अंकित हैं। जिनालयों में वन्दन, अभिषेक, नृत्य, संगीत और आलोक, इनके लिए अलग-अलग मण्डप हैं; क्रीडागृह, गुणनगृह ( स्वाध्यायशाला) तथा पट्टशालाएँ (चित्रशाला) भी हैं । जिनमन्दिरों में जिनेन्द्र की मूर्तियों के अतिरिक्त, देवच्छन्द के भीतर श्रीदेवी, श्रुतदेवी तथा यक्षों की मूर्तियाँ एवं अष्टमंगल द्रव्य भी स्थापित होते हैं। ये आठ मंगलद्रव्य हैं: झारी, कलश, दर्पण, ध्वज, चमर, छत्र, व्यजन और सुप्रतिष्ठ । जिन - प्रतिमाओं के आसपास नागों और यक्षों के युगल अपने हाथों में चमर लिये हुए स्थित रहते हैं ।
असुरों के भवन सात, आठ, नौ, दस आदि भूमियों (मंजिलों) से युक्त होते हैं, जिनमें जन्म, अभिषेक, शयन, परिचर्या और मन्त्रणा – इनके लिए अलग-अलग शालाएँ होती । उनमें सामान्यगृह, गर्भगृह, कदलीगृह, चित्रगृह, आसनगृह, नादगृह, लतागृह आदि होते हैं तथा तोरण, प्राकार, पुष्करिणी, वापी और कूप, मत्तवारण और गवाक्ष ध्वजा-पताकाओं एवं नाना प्रकार की पुतलियों से सुसज्जित होते हैं।
इस प्रकार, यतिवृषभाचार्य ने वास्तु का सामान्य आदर्श प्रस्तुत किया है। प्राकृत-साहित्य में वर्णित वास्तु-विन्यास के आधारादर्श के रूप में 'तिलोयपण्णत्ति' की उपयोगिता सन्दिग्ध नहीं है । यह महत्त्वपूर्ण कृति भारत के स्वर्णकाल की अवधि (चतुर्थ पंचम शती) में लिखी गई है, इसलिए सम्भव है, संघदासगणी ने भी अपने वास्तुवर्णन के सन्दर्भ में 'तिलोयपण्णत्ति' का प्रभाव ग्रहण किया हो ।
उक्त सामान्य भवन के अतिरिक्त जैनवास्तुकला में, जिनेन्द्र की मूर्तियों की प्रतिष्ठा के समय जन्ममहोत्सव के लिए मन्दर मेरु की रचना; नन्दीश्वर द्वीप का निर्माण; समवसरण (सभाभवन) की रचना; मानस्तम्भ की स्थापना, चैत्य, चैत्यवृक्ष एवं स्तूप, श्रीमण्डप, गन्धकुटी, गुफाएँ और उनमें अंकित मूर्तियाँ, मन्दिर, नगर आदि का विन्यास प्रभृति वास्तु भी अपना उल्लेखनीय महत्त्व रखते हैं। सच पूछिए तो, वास्तुकला में ही आलेख्य, आलेप्य आदि कलाएँ भी समाहृत हो जाती हैं और इस प्रकार वास्तुकला ही समस्त कलाओं की आधारभूमि सिद्ध होती है ।
१. जैन वास्तुकला के विशेष अध्ययन के लिए द्रष्टव्य : भारतीय संस्कृति में जैनधर्म का योगदान : डॉ. हीरालाल जैन; व्याख्यान ४ (जैनकला), पृ. २९२