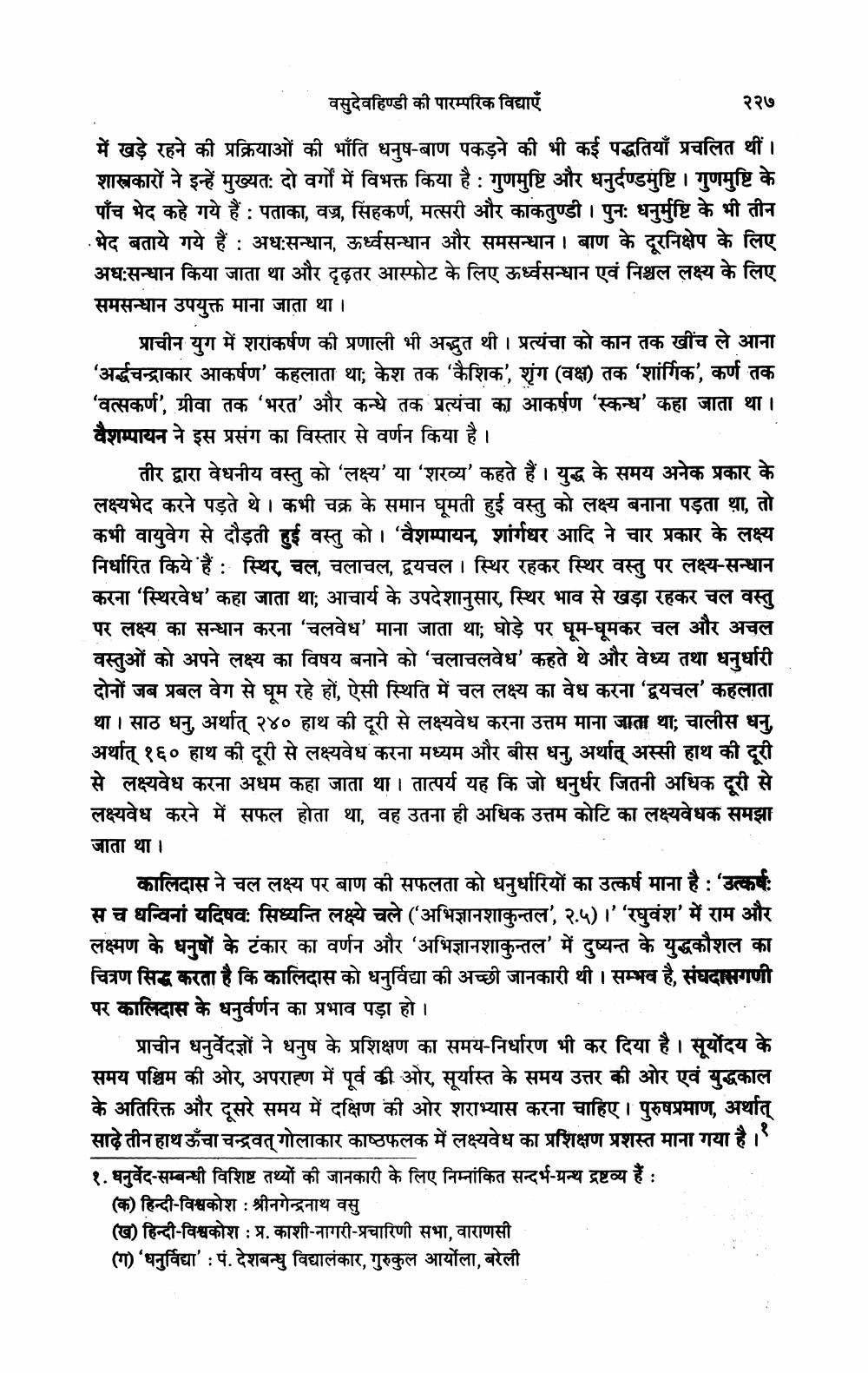________________
वसुदेवहिण्डी की पारम्परिक विद्याएँ
२२७ में खड़े रहने की प्रक्रियाओं की भाँति धनुष-बाण पकड़ने की भी कई पद्धतियाँ प्रचलित थीं। शास्त्रकारों ने इन्हें मुख्यत: दो वर्गों में विभक्त किया है : गुणमुष्टि और धनुर्दण्डमुष्टि । गुणमुष्टि के पाँच भेद कहे गये हैं : पताका, वज्र, सिंहकर्ण, मत्सरी और काकतुण्डी । पुन: धनुर्मुष्टि के भी तीन भेद बताये गये हैं : अध:सन्धान, ऊर्ध्वसन्धान और समसन्धान । बाण के दूरनिक्षेप के लिए अधःसन्धान किया जाता था और दृढ़तर आस्फोट के लिए ऊर्ध्वसन्धान एवं निश्चल लक्ष्य के लिए समसन्धान उपयुक्त माना जाता था।
प्राचीन युग में शराकर्षण की प्रणाली भी अद्भुत थी। प्रत्यंचा को कान तक खींच ले आना 'अर्द्धचन्द्राकार आकर्षण' कहलाता था; केश तक 'कैशिक', शृंग (वक्ष) तक 'शांर्गिक', कर्ण तक 'वत्सकर्ण', ग्रीवा तक 'भरत' और कन्धे तक प्रत्यंचा का आकर्षण 'स्कन्ध' कहा जाता था। वैशम्पायन ने इस प्रसंग का विस्तार से वर्णन किया है।
तीर द्वारा वेधनीय वस्तु को 'लक्ष्य' या 'शरव्य' कहते हैं। युद्ध के समय अनेक प्रकार के लक्ष्यभेद करने पड़ते थे। कभी चक्र के समान घूमती हुई वस्तु को लक्ष्य बनाना पड़ता था, तो कभी वायुवेग से दौड़ती हुई वस्तु को। वैशम्पायन, शांर्गधर आदि ने चार प्रकार के लक्ष्य निर्धारित किये हैं : स्थिर, चल, चलाचल, द्वयचल। स्थिर रहकर स्थिर वस्तु पर लक्ष्य-सन्धान करना 'स्थिरवेध' कहा जाता था; आचार्य के उपदेशानुसार, स्थिर भाव से खड़ा रहकर चल वस्तु पर लक्ष्य का सन्धान करना 'चलवेध' माना जाता था; घोड़े पर घूम-घूमकर चल और अचल वस्तुओं को अपने लक्ष्य का विषय बनाने को 'चलाचलवेध' कहते थे और वेध्य तथा धनुर्धारी दोनों जब प्रबल वेग से घूम रहे हों, ऐसी स्थिति में चल लक्ष्य का वेध करना 'द्वयचल' कहलाता था। साठ धनु, अर्थात् २४० हाथ की दूरी से लक्ष्यवेध करना उत्तम माना जाता था; चालीस धनु, अर्थात् १६० हाथ की दूरी से लक्ष्यवेध करना मध्यम और बीस धनु, अर्थात् अस्सी हाथ की दूरी से लक्ष्यवेध करना अधम कहा जाता था। तात्पर्य यह कि जो धनुर्धर जितनी अधिक दूरी से लक्ष्यवेध करने में सफल होता था, वह उतना ही अधिक उत्तम कोटि का लक्ष्यवेधक समझा जाता था।
कालिदास ने चल लक्ष्य पर बाण की सफलता को धनुर्धारियों का उत्कर्ष माना है : 'उत्कर्षः स च धन्विनां यदिषव: सिध्यन्ति लक्ष्ये चले ('अभिज्ञानशाकुन्तल', २.५)।' 'रघुवंश' में राम और लक्ष्मण के धनुषों के टंकार का वर्णन और 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में दुष्यन्त के युद्धकौशल का चित्रण सिद्ध करता है कि कालिदास को धनुर्विद्या की अच्छी जानकारी थी। सम्भव है, संघदासगणी पर कालिदास के धनुर्वर्णन का प्रभाव पड़ा हो।
प्राचीन धनुर्वेदज्ञों ने धनुष के प्रशिक्षण का समय-निर्धारण भी कर दिया है। सूर्योदय के समय पश्चिम की ओर, अपराह्य में पूर्व की ओर, सूर्यास्त के समय उत्तर की ओर एवं युद्धकाल के अतिरिक्त और दूसरे समय में दक्षिण की ओर शराभ्यास करना चाहिए। पुरुषप्रमाण, अर्थात् साढ़े तीन हाथ ऊँचा चन्द्रवत् गोलाकार काष्ठफलक में लक्ष्यवेध का प्रशिक्षण प्रशस्त माना गया है।' १. धनुर्वेद-सम्बन्धी विशिष्ट तथ्यों की जानकारी के लिए निम्नांकित सन्दर्भ-ग्रन्थ द्रष्टव्य हैं : (क) हिन्दी-विश्वकोश : श्रीनगेन्द्रनाथ वसु (ख) हिन्दी-विश्वकोश : प्र. काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा, वाराणसी (ग) धनुर्विद्या' : पं. देशबन्धु विद्यालंकार, गुरुकुल आर्योला, बरेली