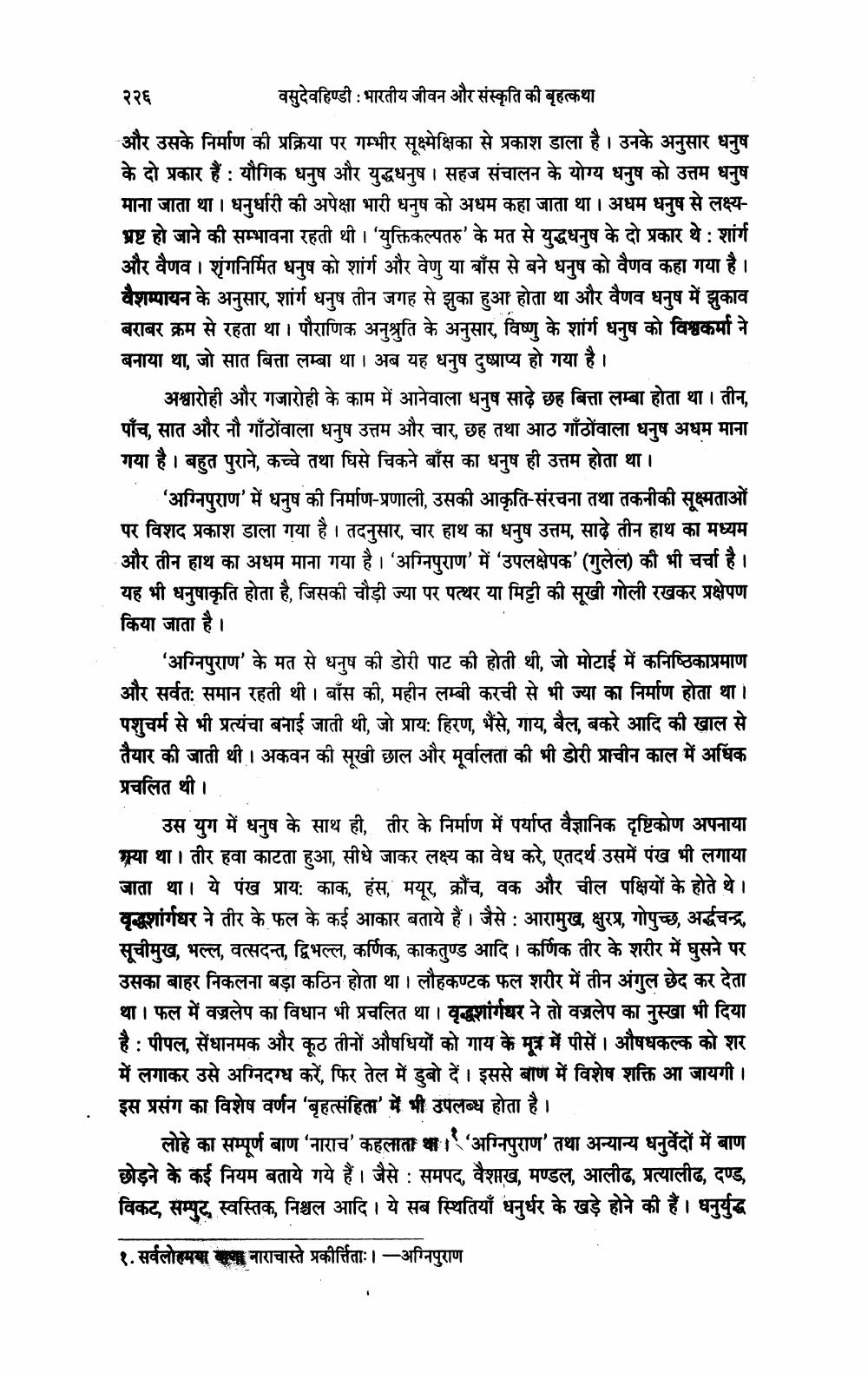________________
२२६
वसुदेवहिण्डी : भारतीय जीवन और संस्कृति की बृहत्कथा
- और उसके निर्माण की प्रक्रिया पर गम्भीर सूक्ष्मेक्षिका से प्रकाश डाला है। उनके अनुसार धनुष
दो प्रकार हैं : यौगिक धनुष और युद्धधनुष । सहज संचालन के योग्य धनुष को उत्तम धनुष माना जाता था । धनुर्धारी की अपेक्षा भारी धनुष को अधम कहा जाता था । अधम धनुष से लक्ष्यभ्रष्ट हो जाने की सम्भावना रहती थी। 'युक्तिकल्पतरु' के मत से युद्धधनुष के दो प्रकार थे : शांर्ग और वैणव । शृंगनिर्मित धनुष को शांर्ग और वेणु या बाँस से बने धनुष को वैणव कहा गया है। वैशम्पायन के अनुसार, शांर्ग धनुष तीन जगह से झुका हुआ होता था और वैणव धनुष में झुकाव बराबर क्रम से रहता था। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार, विष्णु के शांर्ग धनुष को विश्वकर्मा ने बनाया था, जो सात बित्ता लम्बा था। अब यह धनुष दुष्प्राप्य हो गया है।
अश्वारोही और गजारोही के काम में आनेवाला धनुष साढ़े छह बित्ता लम्बा होता था । तीन, पाँच, सात और नौ गाँठोंवाला धनुष उत्तम और चार, छह तथा आठ गाँठोंवाला धनुष अधम माना गया है। बहुत पुराने, कच्चे तथा घिसे चिकने बाँस का धनुष ही उत्तम होता था ।
'अग्निपुराण' में धनुष की निर्माण प्रणाली, उसकी आकृति संरचना तथा तकनीकी सूक्ष्मताओं पर विशद प्रकाश डाला गया है। तदनुसार, चार हाथ का धनुष उत्तम, साढ़े तीन हाथ का मध्यम और तीन हाथ का अधम माना गया है । 'अग्निपुराण' में 'उपलक्षेपक' (गुलेल) की भी चर्चा है । यह भी धनुषाकृति होता है, जिसकी चौड़ी ज्या पर पत्थर या मिट्टी की सूखी गोली रखकर प्रक्षेपण किया जाता है ।
'अग्निपुराण' के मत से धनुष की डोरी पाट की होती थी, जो मोटाई में कनिष्ठिकाप्रमाण और सर्वतः समान रहती थी। बाँस की, महीन लम्बी करची से भी ज्या का निर्माण होता था । पशुचर्म से भी प्रत्यंचा बनाई जाती थी, जो प्राय: हिरण, भैंसे, गाय, बैल, बकरे आदि की खाल से तैयार की जाती थी । अकवन की सूखी छाल और मूर्वालता की भी डोरी प्राचीन काल में अधिक प्रचलित थी ।
उस युग में धनुष के साथ ही, तीर के निर्माण में पर्याप्त वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया या था। तीर हवा काटता हुआ, सीधे जाकर लक्ष्य का वेध करे, एतदर्थ उसमें पंख भी लगाया जाता था । ये पंख प्रायः काक, हंस, मयूर, क्रौंच, वक और चील पक्षियों के होते थे । वृद्धशांर्गधर ने तीर के फल के कई आकार बताये हैं। जैसे : आरामुख, क्षुरप्र, गोपुच्छ, अर्द्धचन्द्र, सूचीमुख, भल्ल, वत्सदन्त, द्विभल्ल, कर्णिक, काकतुण्ड आदि। कर्णिक तीर के शरीर में घुसने पर उसका बाहर निकलना बड़ा कठिन होता था। लौहकण्टक फल शरीर में तीन अंगुल छेद कर देता था । फल में वज्रलेप का विधान भी प्रचलित था । वृद्धशर्गधर ने तो वज्रलेप का नुस्खा भी दिया है : पीपल, सेंधानमक और कूठ तीनों औषधियों को गाय के मूत्र में पीसें औषधकल्क को शर में लगाकर उसे अग्निदग्ध करें, फिर तेल में डुबो दें। इससे बाण में विशेष शक्ति आ जायगी । इस प्रसंग का विशेष वर्णन 'बृहत्संहिता' में भी उपलब्ध होता है ।
लोहे का सम्पूर्ण बाण 'नाराच' कहलाता था।' 'अग्निपुराण' तथा अन्यान्य धनुर्वेदों में बाण छोड़ने के कई नियम बताये गये हैं। जैसे: समपद, वैशाख, मण्डल, आलीढ, प्रत्यालीढ, दण्ड, विकट, सम्पुट स्वस्तिक, निश्चल आदि । ये सब स्थितियाँ धनुर्धर के खड़े होने की हैं। धनुर्युद्ध
१. सर्वलोहमया वाणा नाराचास्ते प्रकीर्त्तिताः । - अग्निपुराण