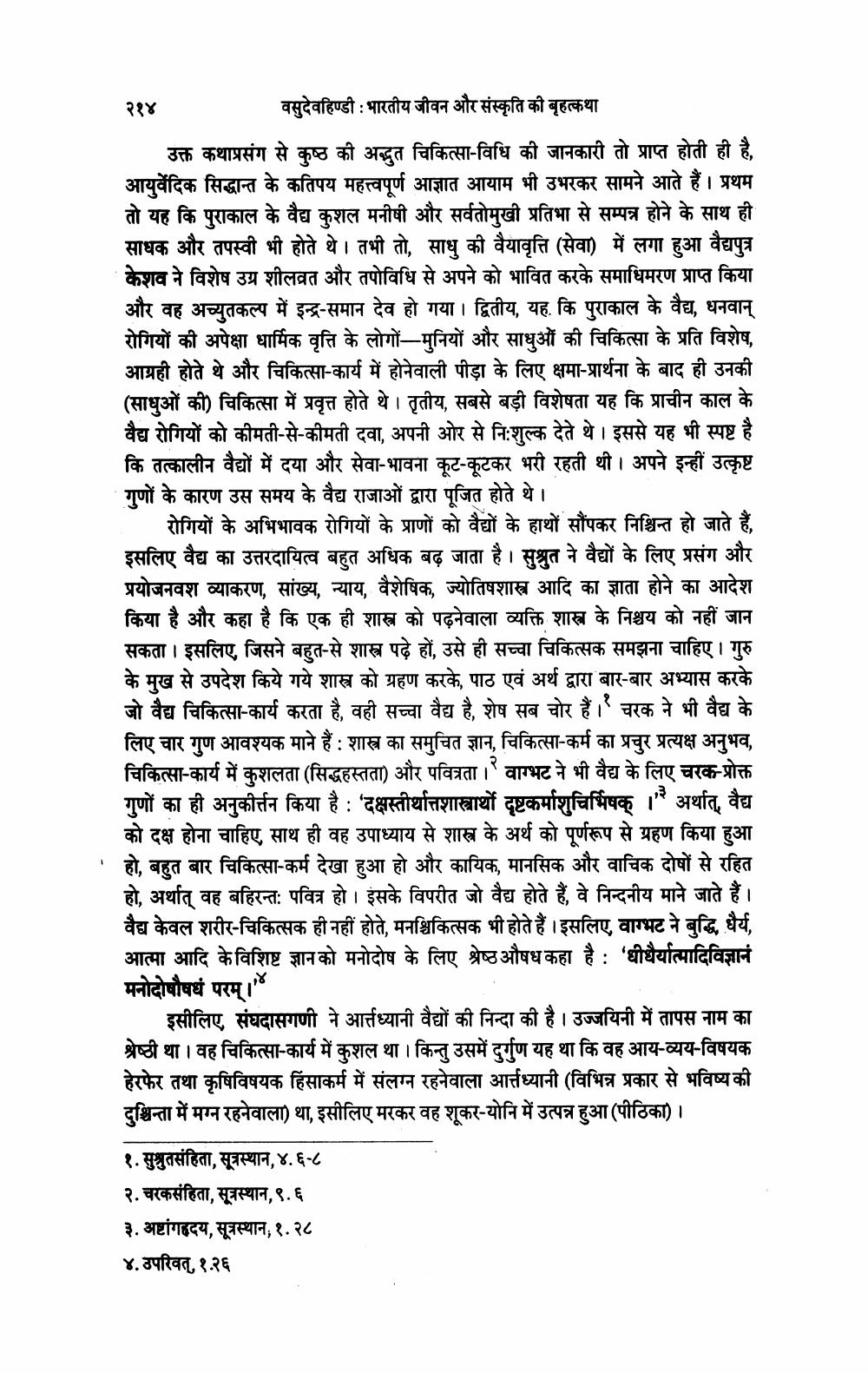________________
वसुदेवहिण्डी : भारतीय जीवन और संस्कृति की बृहत्कथा
उक्त कथाप्रसंग से कुष्ठ की अद्भुत चिकित्सा-विधि की जानकारी तो प्राप्त होती ही है, आयुर्वेदिक सिद्धान्त के कतिपय महत्त्वपूर्ण आज्ञात आयाम भी उभरकर सामने आते हैं। प्रथम तो यह कि पुराकाल के वैद्य कुशल मनीषी और सर्वतोमुखी प्रतिभा से सम्पन्न होने के साथ ही साधक और तपस्वी भी होते थे। तभी तो, साधु की वैयावृत्ति (सेवा) में लगा हुआ वैद्यपुत्र केशव ने विशेष उग्र शीलव्रत और तपोविधि से अपने को भावित करके समाधिमरण प्राप्त किया और वह अच्युतकल्प में इन्द्र- समान देव हो गया । द्वितीय, यह कि पुराकाल के वैद्य, धनवान् रोगियों की अपेक्षा धार्मिक वृत्ति के लोगों-मुनियों और साधुओं की चिकित्सा के प्रति विशेष, आग्रही होते थे और चिकित्सा-कार्य में होनेवाली पीड़ा के लिए क्षमा-प्रार्थना के बाद ही उनकी (साधुओं की ) चिकित्सा में प्रवृत्त होते थे । तृतीय, सबसे बड़ी विशेषता यह कि प्राचीन काल के वैद्य रोगियों को कीमती-से-कीमती दवा, अपनी ओर से निःशुल्क देते थे। इससे यह भी स्पष्ट है कि तत्कालीन वैद्यों में दया और सेवा - भावना कूट-कूटकर भरी रहती थी। अपने इन्हीं उत्कृष्ट गुणों के कारण उस समय के वैद्य राजाओं द्वारा पूजित होते थे ।
रोगियों के अभिभावक रोगियों के प्राणों को वैद्यों के हाथों सौंपकर निश्चिन्त हो जाते हैं, इसलिए वैद्य का उत्तरदायित्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। सुश्रुत ने वैद्यों के लिए प्रसंग और प्रयोजनवश व्याकरण, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, ज्योतिषशास्त्र आदि का ज्ञाता होने का आदेश किया है और कहा है कि एक ही शास्त्र को पढ़नेवाला व्यक्ति शास्त्र के निश्चय को नहीं जान सकता। इसलिए, जिसने बहुत-से शास्त्र पढ़े हों, उसे ही सच्चा चिकित्सक समझना चाहिए। गुरु के मुख से उपदेश किये गये शास्त्र को ग्रहण करके, पाठ एवं अर्थ द्वारा बार-बार अभ्यास करके जो वैद्य चिकित्सा-कार्य करता है, वही सच्चा वैद्य है, शेष सब चोर हैं। ' चरक ने भी वैद्य के लिए चार गुण आवश्यक माने हैं : शास्त्र का समुचित ज्ञान, चिकित्सा-कर्म का प्रचुर प्रत्यक्ष अनुभव, चिकित्सा-कार्य में कुशलता (सिद्धहस्तता) और पवित्रता । वाग्भट ने भी वैद्य के लिए चरक - प्रोक्त गुणों का ही अनुकीर्त्तन किया है : 'दक्षस्तीर्थात्तशास्त्रार्थो दृष्टकर्माशुचिर्भिषक् । अर्थात्, वैद्य को दक्ष होना चाहिए, साथ ही वह उपाध्याय से शास्त्र के अर्थ को पूर्णरूप से ग्रहण किया हुआ हो, बहुत बार चिकित्सा-कर्म देखा हुआ हो और कायिक, मानसिक और वाचिक दोषों से रहित हो, अर्थात् वह बहिरन्तः पवित्र हो । इसके विपरीत जो वैद्य होते हैं, वे निन्दनीय माने जाते हैं । वैद्य केवल शरीर-चिकित्सक ही नहीं होते, मनश्चिकित्सक भी होते हैं। इसलिए, वाग्भट ने बुद्धि, धैर्य, आत्मा आदि के विशिष्ट ज्ञान को मनोदोष के लिए श्रेष्ठ औषध कहा है : 'धीधैर्यात्मादिविज्ञानं मनोदोषौषधं परम्।”
२१४
इसीलिए, संघदासगणी ने आर्त्तध्यानी वैद्यों की निन्दा की है। उज्जयिनी में तापस नाम का श्रेष्ठी था । वह चिकित्सा-कार्य में कुशल था । किन्तु उसमें दुर्गुण यह था कि वह आय-व्यय-विषयक हेरफेर तथा कृषिविषयक हिंसाकर्म में संलग्न रहनेवाला आर्त्तध्यानी ( विभिन्न प्रकार से भविष्य की दुश्चिन्ता में मग्न रहनेवाला) था, इसीलिए मरकर वह शूकर- योनि में उत्पन्न हुआ (पीठिका) ।
१. सुश्रुतसंहिता, सूत्रस्थान, ४. ६-८
२. चरकसंहिता, सूत्रस्थान, ९.६
३. अष्टांगहृदय, सूत्रस्थान, १.२८
४. उपरिवत्, १.२६