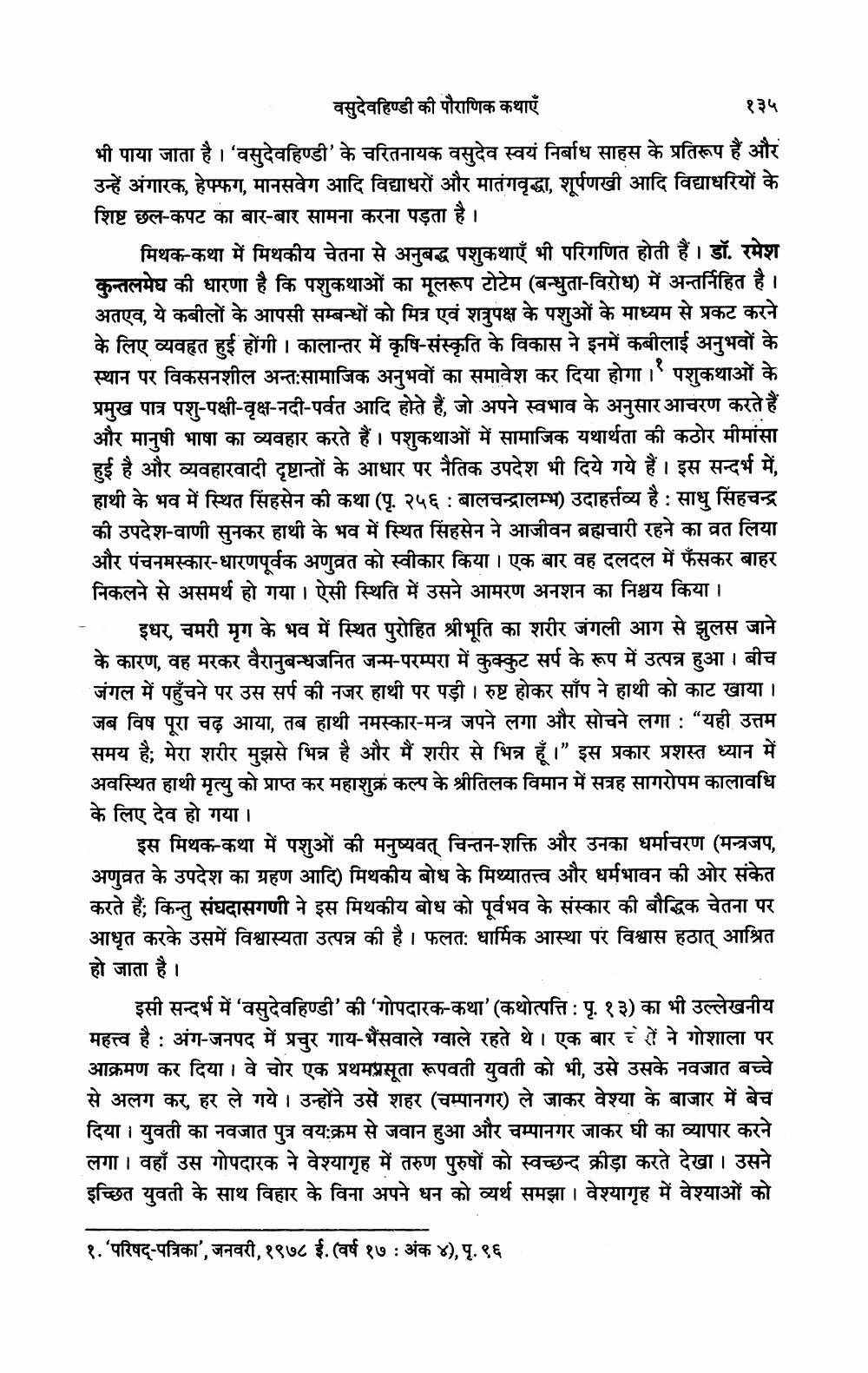________________
वसुदेवहिण्डी की पौराणिक कथाएँ
१३५ भी पाया जाता है । 'वसुदेवहिण्डी' के चरितनायक वसुदेव स्वयं निर्बाध साहस के प्रतिरूप हैं और उन्हें अंगारक, हेफ्फग, मानसवेग आदि विद्याधरों और मातंगवृद्धा, शूर्पणखी आदि विद्याधरियों के शिष्ट छल-कपट का बार-बार सामना करना पड़ता है।
मिथक कथा में मिथकीय चेतना से अनुबद्ध पशुकथाएँ भी परिगणित होती हैं। डॉ. रमेश कुन्तलमेघ की धारणा है कि पशुकथाओं का मूलरूप टोटेम (बन्धुता-विरोध) में अन्तर्निहित है। अतएव, ये कबीलों के आपसी सम्बन्धों को मित्र एवं शत्रुपक्ष के पशुओं के माध्यम से प्रकट करने के लिए व्यवहृत हुई होंगी। कालान्तर में कृषि-संस्कृति के विकास ने इनमें कबीलाई अनुभवों के स्थान पर विकसनशील अन्त:सामाजिक अनुभवों का समावेश कर दिया होगा। पशुकथाओं के प्रमुख पात्र पशु-पक्षी-वृक्ष-नदी-पर्वत आदि होते हैं, जो अपने स्वभाव के अनुसार आचरण करते हैं
और मानुषी भाषा का व्यवहार करते हैं। पशुकथाओं में सामाजिक यथार्थता की कठोर मीमांसा हुई है और व्यवहारवादी दृष्टान्तों के आधार पर नैतिक उपदेश भी दिये गये हैं। इस सन्दर्भ में, हाथी के भव में स्थित सिंहसेन की कथा (पृ. २५६ : बालचन्द्रालम्भ) उदाहर्त्तव्य है : साधु सिंहचन्द्र की उपदेश-वाणी सुनकर हाथी के भव में स्थित सिंहसेन ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया
और पंचनमस्कार-धारणपूर्वक अणुव्रत को स्वीकार किया। एक बार वह दलदल में फँसकर बाहर निकलने से असमर्थ हो गया। ऐसी स्थिति में उसने आमरण अनशन का निश्चय किया। - इधर, चमरी मृग के भव में स्थित पुरोहित श्रीभूति का शरीर जंगली आग से झुलस जाने
के कारण, वह मरकर वैरानुबन्धजनित जन्म-परम्परा में कुक्कुट सर्प के रूप में उत्पन्न हुआ। बीच जंगल में पहुँचने पर उस सर्प की नजर हाथी पर पड़ी। रुष्ट होकर साँप ने हाथी को काट खाया। जब विष पूरा चढ़ आया, तब हाथी नमस्कार-मन्त्र जपने लगा और सोचने लगा : “यही उत्तम समय है; मेरा शरीर मुझसे भिन्न है और मैं शरीर से भिन्न हूँ।" इस प्रकार प्रशस्त ध्यान में अवस्थित हाथी मृत्यु को प्राप्त कर महाशुक्र कल्प के श्रीतिलक विमान में सत्रह सागरोपम कालावधि के लिए देव हो गया।
इस मिथक कथा में पशुओं की मनुष्यवत् चिन्तन-शक्ति और उनका धर्माचरण (मन्त्रजप, अणुव्रत के उपदेश का ग्रहण आदि) मिथकीय बोध के मिथ्यातत्त्व और धर्मभावन की ओर संकेत करते हैं; किन्तु संघदासगणी ने इस मिथकीय बोध को पूर्वभव के संस्कार की बौद्धिक चेतना पर आधृत करके उसमें विश्वास्यता उत्पन्न की है। फलत: धार्मिक आस्था पर विश्वास हठात् आश्रित हो जाता है।
इसी सन्दर्भ में 'वसुदेवहिण्डी' की 'गोपदारक-कथा' (कथोत्पत्ति : पृ. १३) का भी उल्लेखनीय महत्त्व है : अंग-जनपद में प्रचुर गाय-भैंसवाले ग्वाले रहते थे। एक बार चरों ने गोशाला पर आक्रमण कर दिया। वे चोर एक प्रथमप्रसूता रूपवती युवती को भी, उसे उसके नवजात बच्चे से अलग कर, हर ले गये। उन्होंने उसे शहर (चम्पानगर) ले जाकर वेश्या के बाजार में बेच दिया। युवती का नवजात पुत्र वय:क्रम से जवान हुआ और चम्पानगर जाकर घी का व्यापार करने लगा। वहाँ उस गोपदारक ने वेश्यागृह में तरुण पुरुषों को स्वच्छन्द क्रीड़ा करते देखा। उसने इच्छित युवती के साथ विहार के विना अपने धन को व्यर्थ समझा। वेश्यागृह में वेश्याओं को
१. परिषद्-पत्रिका',जनवरी, १९७८ ई. (वर्ष १७ : अंक ४), पृ.९६