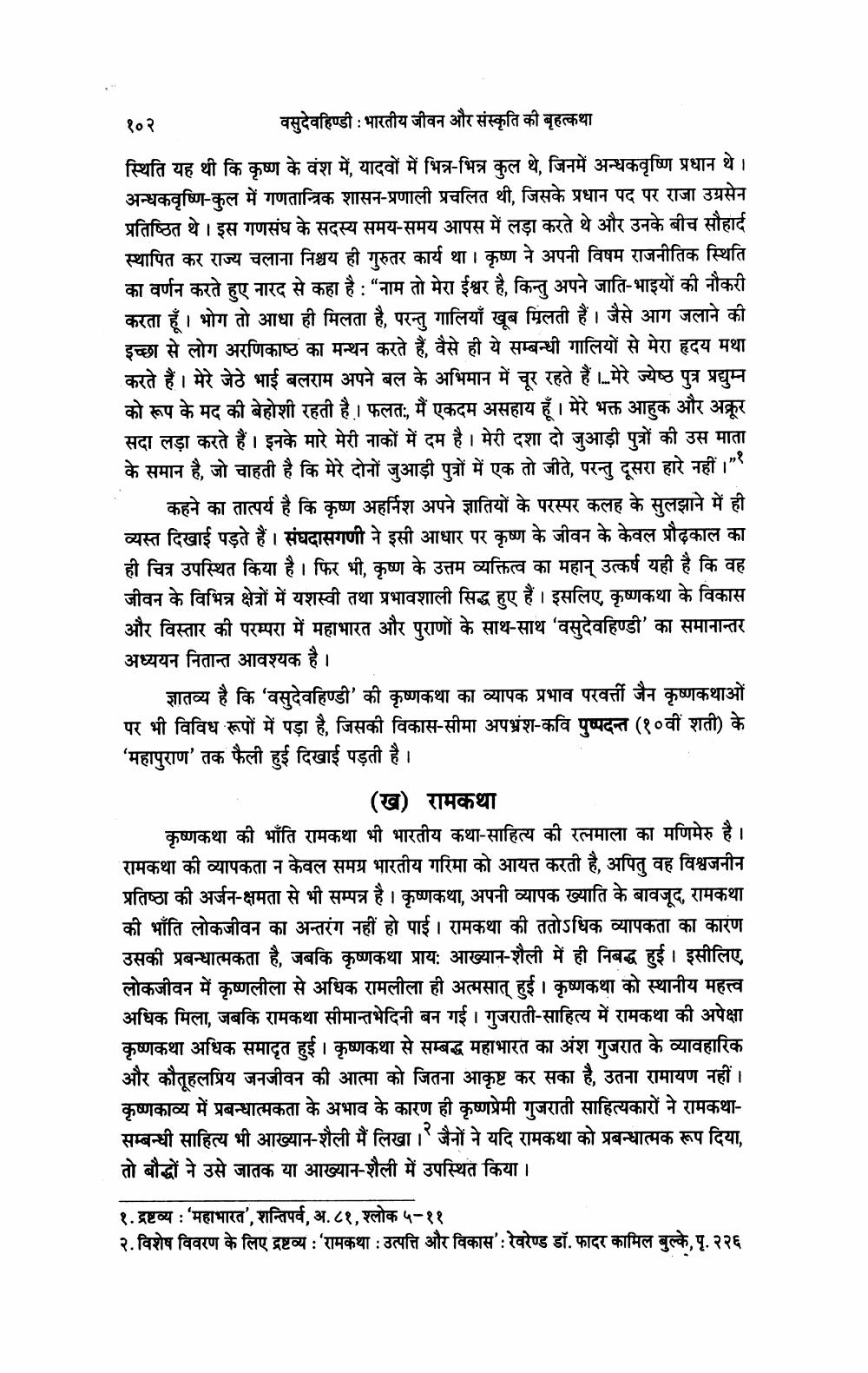________________
१०२
वसुदेवहिण्डी : भारतीय जीवन और संस्कृति की बृहत्कथा
स्थिति यह कि कृष्ण के वंश में, यादवों में भिन्न-भिन्न कुल थे, जिनमें अन्धकवृष्णि प्रधान थे । अन्धकवृष्णि - कुल में गणतान्त्रिक शासन प्रणाली प्रचलित थी, जिसके प्रधान पद पर राजा उग्रसेन प्रतिष्ठित थे । इस गणसंघ के सदस्य समय-समय आपस में लड़ा करते थे और उनके बीच सौहार्द स्थापित कर राज्य चलाना निश्चय ही गुरुतर कार्य था। कृष्ण ने अपनी विषम राजनीतिक स्थिति का वर्णन करते हुए नारद से कहा है: “नाम तो मेरा ईश्वर है, किन्तु अपने जाति - भाइयों की नौकरी करता हूँ । भोग तो आधा ही मिलता है, परन्तु गालियाँ खूब मिलती हैं। जैसे आग जलाने की इच्छा से लोग अरणिकाष्ठ का मन्थन करते हैं, वैसे ही ये सम्बन्धी गालियों से मेरा हृदय मथा करते हैं । मेरे जेठे भाई बलराम अपने बल के अभिमान में चूर रहते हैं ।..मेरे ज्येष्ठ पुत्र प्रद्युम्न को रूप के मद की बेहोशी रहती है । फलतः, मैं एकदम असहाय हूँ । मेरे भक्त आहुक और अक्रूर सदा लड़ा करते हैं । इनके मारे मेरी नाकों में दम है । मेरी दशा दो जुआड़ी पुत्रों की उस माता के समान है, जो चाहती है कि मेरे दोनों जुआड़ी पुत्रों में एक तो जीते, परन्तु दूसरा हारे नहीं ।'
"१
कहने का तात्पर्य है कि कृष्ण अहर्निश अपने ज्ञातियों के परस्पर कलह के सुलझाने में ही व्यस्त दिखाई पड़ते हैं । संघदासगणी ने इसी आधार पर कृष्ण के जीवन के केवल प्रौढ़काल का ही चित्र उपस्थित किया है। फिर भी, कृष्ण के उत्तम व्यक्तित्व का महान् उत्कर्ष यही है कि वह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में यशस्वी तथा प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं। इसलिए, कृष्णकथा के विकास और विस्तार की परम्परा में महाभारत और पुराणों के साथ-साथ 'वसुदेवहिण्डी' का समानान्तर अध्ययन नितान्त आवश्यक है ।
ज्ञातव्य है कि 'वसुदेवहिण्डी' की कृष्णकथा का व्यापक प्रभाव परवर्त्ती जैन कृष्णकथाओं पर भी विविध रूपों में पड़ा है, जिसकी विकास-सीमा अपभ्रंश- कवि पुष्पदन्त (१०वीं शती) के 'महापुराण' तक फैली हुई दिखाई पड़ती है ।
(ख)
रामकथा
कृष्णकथा की भाँति रामकथा भी भारतीय कथा - साहित्य की रत्नमाला का मणिमेरु है । रामकथा की व्यापकता न केवल समग्र भारतीय गरिमा को आयत्त करती है, अपितु वह विश्वजनीन प्रतिष्ठा की अर्जन-क्षमता से भी सम्पन्न है । कृष्णकथा, अपनी व्यापक ख्याति के बावजूद, रामकथा की भाँति लोकजीवन का अन्तरंग नहीं हो पाई। रामकथा की ततोऽधिक व्यापकता का कारण उसकी प्रबन्धात्मकता है, जबकि कृष्णकथा प्राय: आख्यान - शैली में ही निबद्ध हुई । इसीलिए, लोकजीवन में कृष्णलीला से अधिक रामलीला ही अत्मसात् हुई । कृष्णकथा को स्थानीय महत्त्व अधिक मिला, जबकि रामकथा सीमान्तभेदिनी बन गई। गुजराती - साहित्य में रामकथा की अपेक्षा कृष्णकथा अधिक समादृत हुई । कृष्णकथा से सम्बद्ध महाभारत का अंश गुजरात के व्यावहारिक और कौतूहलप्रिय जनजीवन की आत्मा को जितना आकृष्ट कर सका है, उतना रामायण नहीं । कृष्णकाव्य में प्रबन्धात्मकता के अभाव के कारण ही कृष्णप्रेमी गुजराती साहित्यकारों ने रामकथासम्बन्धी साहित्य भी आख्यान - शैली मैं लिखा । जैनों ने यदि रामकथा को प्रबन्धात्मक रूप दिया, तो बौद्धों ने उसे जातक या आख्यान - शैली में उपस्थित किया ।
१. द्रष्टव्य : 'महाभारत', शन्तिपर्व, अ. ८१, श्लोक ५-११
२. विशेष विवरण के लिए द्रष्टव्य : 'रामकथा : उत्पत्ति और विकास' : रेवरेण्ड डॉ. फादर कामिल बुल्के, पृ. २२६