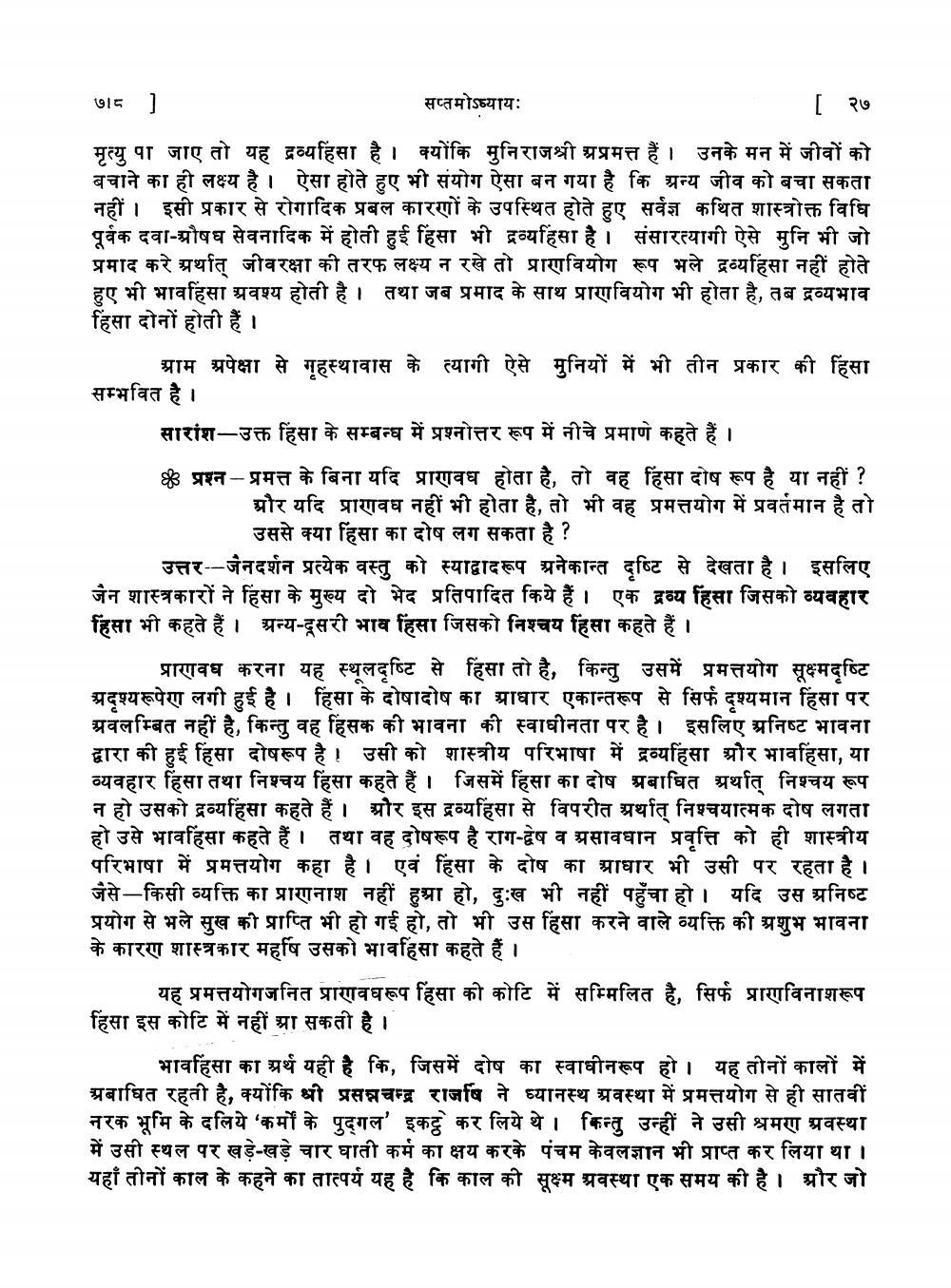________________
७८ ]
सप्तमोऽध्यायः
[ २७
मृत्यु पा जाए तो यह द्रव्यहिंसा है। क्योंकि मुनिराजश्री अप्रमत्त हैं। उनके मन में जीवों को बचाने का ही लक्ष्य है। ऐसा होते हुए भी संयोग ऐसा बन गया है कि अन्य जीव को बचा सकता नहीं। इसी प्रकार से रोगादिक प्रबल कारणों के उपस्थित होते हुए सर्वज्ञ कथित शास्त्रोक्त विधि पूर्वक दवा-औषध सेवनादिक में होती हुई हिंसा भी द्रव्याहिंसा है। संसारत्यागी ऐसे मुनि भी जो प्रमाद करे अर्थात् जीवरक्षा की तरफ लक्ष्य न रखे तो प्राणवियोग रूप भले द्रव्यहिंसा नहीं होते हुए भी भावहिंसा अवश्य होती है। तथा जब प्रमाद के साथ प्राणवियोग भी होता है, तब द्रव्यभाव हिंसा दोनों होती हैं।
आम अपेक्षा से गृहस्थावास के त्यागी ऐसे मुनियों में भी तीन प्रकार की हिंसा सम्भवित है।
सारांश-उक्त हिंसा के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर रूप में नीचे प्रमाणे कहते हैं। * प्रश्न-प्रमत्त के बिना यदि प्राणवध होता है, तो वह हिंसा दोष रूप है या नहीं?
और यदि प्राणवध नहीं भी होता है, तो भी वह प्रमत्तयोग में प्रवर्तमान है तो
उससे क्या हिंसा का दोष लग सकता है ? । उत्तर--जैनदर्शन प्रत्येक वस्तु को स्याद्वादरूप अनेकान्त दृष्टि से देखता है। इसलिए जैन शास्त्रकारों ने हिंसा के मुख्य दो भेद प्रतिपादित किये हैं। एक द्रव्य हिंसा जिसको व्यवहार हिंसा भी कहते हैं। अन्य-दूसरी भाव हिंसा जिसको निश्चय हिंसा कहते हैं ।
प्राणवध करना यह स्थूलदृष्टि से हिंसा तो है, किन्तु उसमें प्रमत्तयोग सूक्ष्मदृष्टि अदृश्यरूपेण लगी हुई है। हिंसा के दोषादोष का आधार एकान्तरूप से सिर्फ दृश्यमान हिंसा पर अवलम्बित नहीं है, किन्तु वह हिंसक की भावना की स्वाधीनता पर है। इसलिए अनिष्ट भावना द्वारा की हुई हिंसा दोषरूप है। उसी को शास्त्रीय परिभाषा में द्रव्यहिंसा और भावहिंसा, या व्यवहार हिंसा तथा निश्चय हिंसा कहते हैं। जिसमें हिंसा का दोष अबाधित अर्थात् निश्चय रूप न हो उसको द्रव्याहिंसा कहते हैं। और इस द्रव्यहिंसा से विपरीत अर्थात् निश्चयात्मक दोष लगता हो उसे भावहिंसा कहते हैं। तथा वह दोषरूप है राग-द्वेष व असावधान प्रवृत्ति को ही शास्त्रीय परिभाषा में प्रमत्तयोग कहा है। एवं हिंसा के दोष का आधार भी उसी पर रहता है। जैसे-किसी व्यक्ति का प्राणनाश नहीं हुआ हो, दुःख भी नहीं पहुँचा हो। यदि उस अनिष्ट प्रयोग से भले सुख की प्राप्ति भी हो गई हो, तो भी उस हिंसा करने वाले व्यक्ति की अशुभ भावना के कारण शास्त्रकार महर्षि उसको भावहिंसा कहते हैं ।
यह प्रमत्तयोगजनित प्राणवघरूप हिंसा को कोटि में सम्मिलित है, सिर्फ प्राणविनाशरूप हिंसा इस कोटि में नहीं आ सकती है।
भावहिंसा का अर्थ यही है कि, जिसमें दोष का स्वाधीनरूप हो। यह तीनों कालों में अबाधित रहती है, क्योंकि श्री प्रसन्नचन्द्र राजर्षि ने ध्यानस्थ अवस्था में प्रमत्तयोग से ही सातवीं नरक भूमि के दलिये 'कर्मों के पुद्गल' इकट्ठ कर लिये थे। किन्तु उन्हीं ने उसी श्रमण अवस्था में उसी स्थल पर खड़े-खड़े चार घाती कर्म का क्षय करके पंचम केवलज्ञान भी प्राप्त कर लिया था। यहाँ तीनों काल के कहने का तात्पर्य यह है कि काल की सूक्ष्म अवस्था एक समय की है। और जो