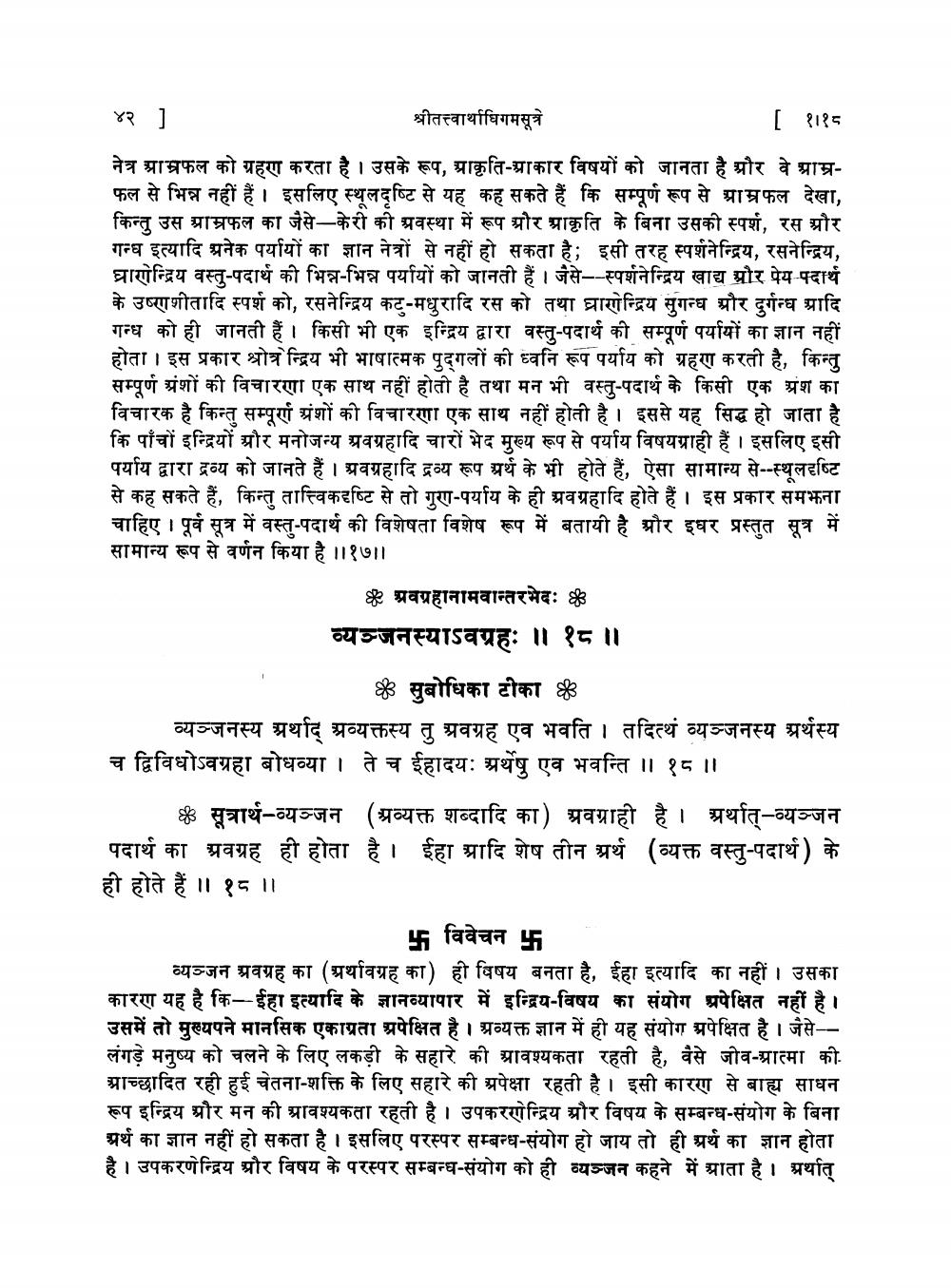________________
४२ ]
श्रीतत्त्वार्थाधिगमसूत्रे
[ ११८
नेत्र आम्रफल को ग्रहण करता है । उसके रूप, प्राकृति प्रकार विषयों को जानता है और वे श्राम्रफल से भिन्न नहीं हैं । इसलिए स्थूल दृष्टि से यह कह सकते हैं कि सम्पूर्ण रूप से प्राम्रफल देखा, किन्तु उस फल का जैसे - केरी की अवस्था में रूप और प्राकृति के बिना उसकी स्पर्श, रस और गन्ध इत्यादि अनेक पर्यायों का ज्ञान नेत्रों से नहीं हो सकता है; इसी तरह स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय वस्तु-पदार्थ की भिन्न-भिन्न पर्यायों को जानती हैं। जैसे- स्पर्शनेन्द्रिय खाद्य और पेय पदार्थ
उष्णशीतादि स्पर्श को, रसनेन्द्रिय कटु-मधुरादि रस को तथा घ्राणेन्द्रिय सुगन्ध और दुर्गन्ध प्रादि गन्ध को ही जानती हैं। किसी भी एक इन्द्रिय द्वारा वस्तु-पदार्थ की सम्पूर्ण पर्यायों का ज्ञान नहीं होता । इस प्रकार श्रोत्र न्द्रिय भी भाषात्मक पुद्गलों की ध्वनि रूप पर्याय को ग्रहण करती है, किन्तु सम्पूर्ण अंशों की विचारणा एक साथ नहीं होती है तथा मन भी वस्तु पदार्थ के किसी एक अंश का विचारक है किन्तु सम्पूर्ण अंशों की विचारणा एक साथ नहीं होती है । इससे यह सिद्ध हो जाता है कि पाँचों इन्द्रियों और मनोजन्य प्रवग्रहादि चारों भेद मुख्य रूप से पर्याय विषयग्राही हैं । इसलिए इसी पर्याय द्वारा द्रव्य को जानते हैं । अवग्रहादि द्रव्य रूप अर्थ के भी होते हैं, ऐसा सामान्य से स्थूलदृष्टि से कह सकते हैं, किन्तु तात्त्विकदृष्टि से तो गुरण-पर्याय के ही अवग्रहादि होते हैं । इस प्रकार समझना चाहिए । पूर्व सूत्र में वस्तु पदार्थ की विशेषता विशेष रूप में बतायी है और इधर प्रस्तुत सूत्र सामान्य रूप से वर्णन किया है ।।१७।।
में
* श्रवग्रहानामवान्तरभेदः
व्यञ्जनस्याऽवग्रहः ॥ १८ ॥
* सुबोधिका टीका
व्यञ्जनस्य अर्थाद् अव्यक्तस्य तु अवग्रह एव भवति । तदित्थं व्यञ्जनस्य र्थस्य चद्विविधोऽवग्रहा बोधव्या । ते च ईहादयः अर्थेषु एव भवन्ति ॥ १८ ॥
* सूत्रार्थ - व्यञ्जन ( अव्यक्त शब्दादि का ) अवग्राही है । अर्थात् व्यञ्जन पदार्थ का अवग्रह ही होता है । ईहा आदि शेष तीन अर्थ ( व्यक्त वस्तु-पदार्थ) के ही होते हैं ।। १८ ॥
5 विवेचन 5
व्यञ्जन अवग्रह का (अर्थावग्रह का ) ही विषय बनता है, ईहा इत्यादि का नहीं । उसका कारण यह है कि- ईहा इत्यादि के ज्ञानव्यापार में इन्द्रिय विषय का संयोग अपेक्षित नहीं है । उसमें तो मुख्यपने मानसिक एकाग्रता अपेक्षित है । अव्यक्त ज्ञान में ही यह संयोग अपेक्षित है । जैसे-लंगड़े मनुष्य को चलने के लिए लकड़ी के सहारे की आवश्यकता रहती है, वैसे जीव- प्रात्मा की आच्छादित रही हुई चेतना शक्ति के लिए सहारे की अपेक्षा रहती है । इसी कारण से बाह्य साधन रूप इन्द्रिय और मन की श्रावश्यकता रहती है । उपकरणेन्द्रिय और विषय के सम्बन्ध-संयोग के बिना अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता है । इसलिए परस्पर सम्बन्ध-संयोग हो जाय तो ही अर्थ का ज्ञान होता है । उपकरणेन्द्रिय और विषय के परस्पर सम्बन्ध-संयोग को ही व्यञ्जन कहने में आता है । अर्थात्