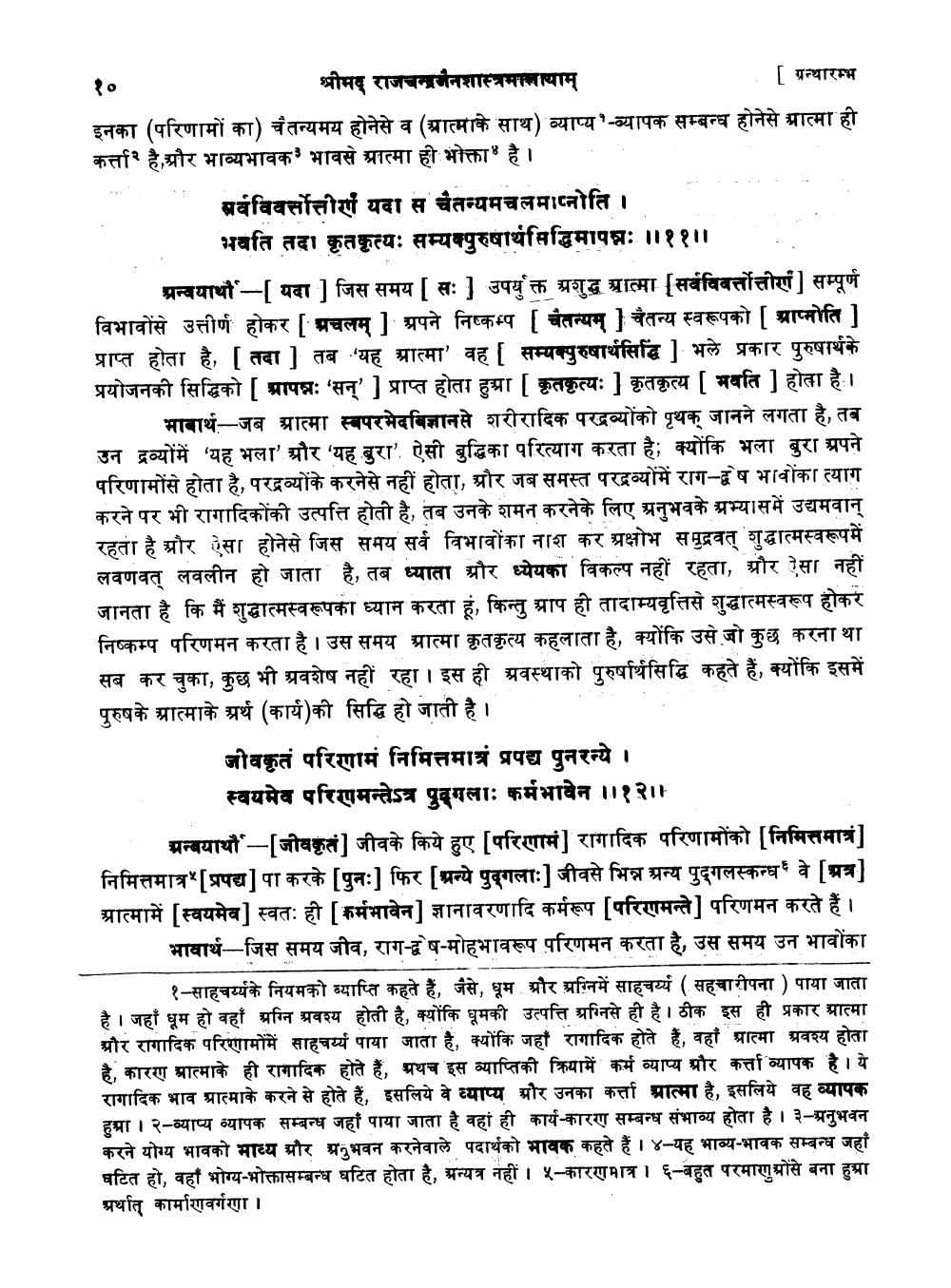________________
१०
श्रीमद् राजचनाननशास्त्रमालायाम्
[ ग्रन्थारम्भ इनका (परिणामों का) चैतन्यमय होनेसे व (प्रात्माके साथ) व्याप्य'-व्यापक सम्बन्ध होनेसे आत्मा ही कर्ता है,और भाव्यभावक भावसे प्रात्मा ही भोक्ता' है।
पर्वविवर्मोत्तीर्ण यदा स चैतन्यमचलमाप्नोति ।
भवति तदा कृतकृत्यः सम्यक्पुरुषार्थसिद्धिमापन्नः ॥११॥ अन्वयार्थी-[यदा ] जिस समय [ सः ] उपर्युक्त अशुद्ध प्रात्मा [सर्वविवर्तोत्तोणं] सम्पूर्ण विभावोंसे उत्तीर्ण होकर [ प्रचलम् ] अपने निष्कम्प [ चैतन्यम् ] चैतन्य स्वरूपको [ प्राप्नोति ] प्राप्त होता है, [ तदा ] तब “यह आत्मा' वह [ सम्यक्पुरुषार्थसिद्धि ] भले प्रकार पुरुषार्थके प्रयोजनकी सिद्धिको [ प्रापन्नः 'सन्' ] प्राप्त होता हुआ [ कृतकृत्यः ] कृतकृत्य [ भवति ] होता है।
भावार्थ-जब आत्मा स्वपरभेदविज्ञानसे शरीरादिक परद्रव्योंको पृथक् जानने लगता है, तब उन द्रव्योंमें 'यह भला' और 'यह बुरा' ऐसी बुद्धिका परित्याग करता है; क्योंकि भला बुरा अपने परिणामोंसे होता है, परद्रव्योंके करनेसे नहीं होता, और जब समस्त परद्रव्योंमें राग-द्वेष भावोंका त्याग करने पर भी रागादिकोंकी उत्पत्ति होती है, तब उनके शमन करनेके लिए अनुभवके अभ्यासमें उद्यमवान् रहता है और ऐसा होनेसे जिस समय सर्व विभावोंका नाश कर अक्षोभ समुद्रवत् शुद्धात्मस्वरूप में लवणवत् लवलीन हो जाता है, तब ध्याता और ध्येयका विकल्प नहीं रहता, और ऐसा नहीं जानता है कि मैं शुद्धात्मस्वरूपका ध्यान करता हूं, किन्तु आप ही तादाम्यवृत्तिसे शुद्धात्मस्वरूप होकर निष्कम्प परिणमन करता है । उस समय प्रात्मा कृतकृत्य कहलाता है, क्योंकि उसे जो कुछ करना था सब कर चुका, कुछ भी अवशेष नहीं रहा। इस ही अवस्थाको पुरुर्षार्थसिद्धि कहते हैं, क्योंकि इसमें पुरुषके आत्माके अर्थ (कार्य)की सिद्धि हो जाती है।
जीवकृतं परिणामं निमित्तमात्रं प्रपद्य पुनरन्ये ।
स्वयमेव परिणमन्तेऽत्र पुद्गलाः कर्मभावेन ॥१२॥ अन्वयाथों-[जीवकृतं] जीवके किये हुए [परिणाम] रागादिक परिणामोंको [निमित्तमात्र] निमित्तमात्र [प्रपद्य] पा करके [पुनः] फिर [अन्ये पुद्गलाः] जीवसे भिन्न अन्य पुद्गलस्कन्ध वे [अत्र] आत्मामें [स्वयमेव] स्वतः ही [कर्मभावेन] ज्ञानावरणादि कर्मरूप [परिणमन्ते] परिणमन करते हैं।
भावार्थ-जिस समय जीव, राग-द्वेष-मोहभावरूप परिणमन करता है, उस समय उन भावोंका
१-साहचर्यके नियमको व्याप्ति कहते हैं, जैसे, धूम और अग्निमें साहचर्या ( सहचारीपना ) पाया जाता है । जहाँ धूम हो वहाँ अग्नि अवश्य होती है, क्योंकि धूमकी उत्पत्ति अग्निसे ही है। ठीक इस ही प्रकार प्रात्मा और रागादिक परिणामोंमें साहचर्य पाया जाता है, क्योंकि जहाँ रागादिक होते हैं, वहाँ प्रात्मा अवश्य होता है, कारण आत्माके ही रागादिक होते हैं, प्रथच इस व्याप्तिकी क्रियामें कर्म व्याप्य और कर्ता व्यापक है। ये रागादिक भाव प्रात्माके करने से होते हैं, इसलिये वे व्याप्य और उनका कर्ता प्रात्मा है, इसलिये वह व्यापक हुमा । २-व्याप्य व्यापक सम्बन्ध जहाँ पाया जाता है वहां ही कार्य-कारण सम्बन्ध संभाव्य होता है । ३-अनुभवन करने योग्य भावको भाव्य और अनुभवन करनेवाले पदार्थको भावक कहते हैं । ४-यह भाव्य-भावक सम्बन्ध जहाँ घटित हो, वहाँ भोग्य-भोक्तासम्बन्ध घटित होता है, अन्यत्र नहीं। ५-कारणमात्र । ६-बहुत परमाणुगोसे बना हुआ अर्थात् कार्माणवर्गणा।