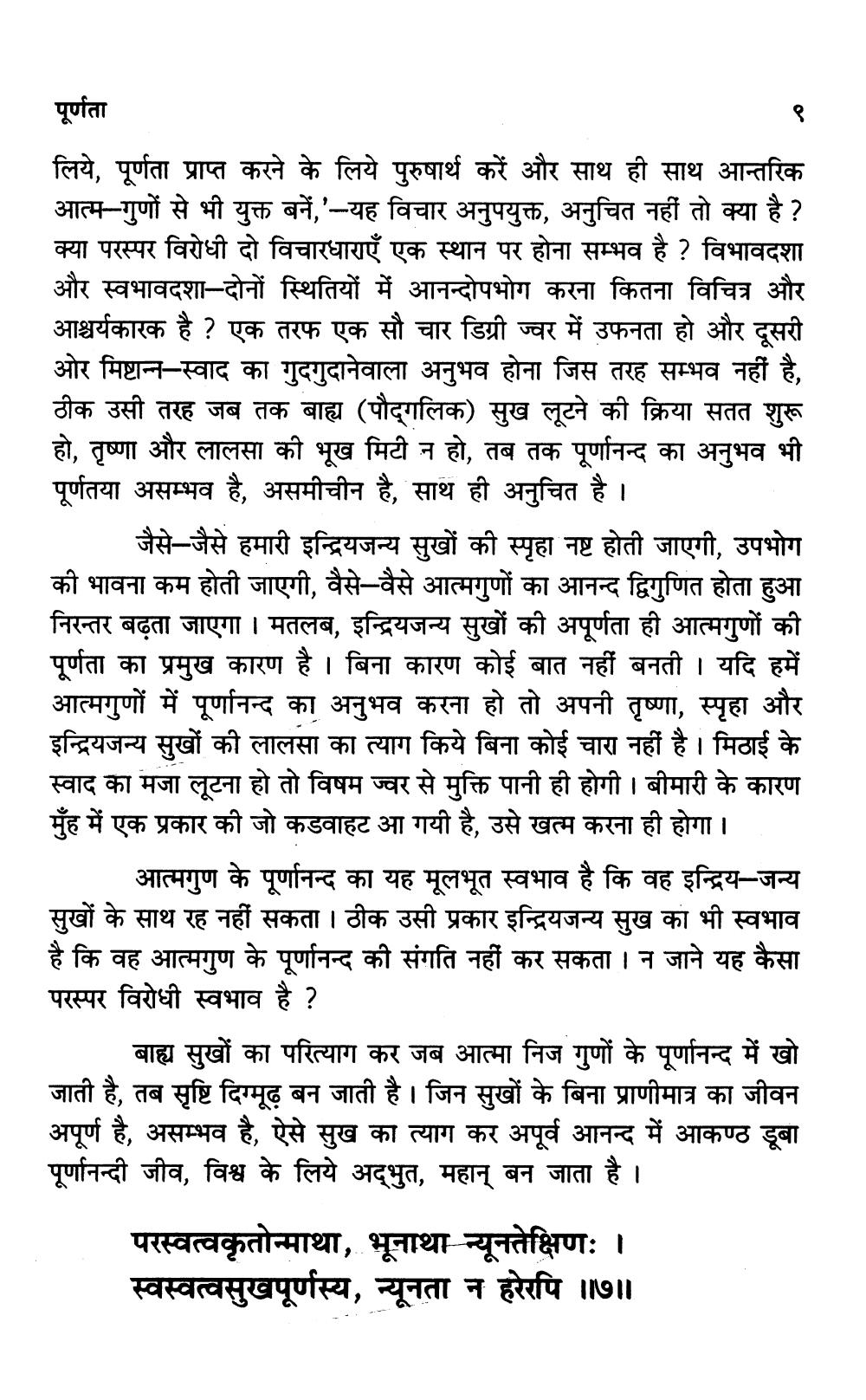________________
पूर्णता
लिये, पूर्णता प्राप्त करने के लिये पुरुषार्थ करें और साथ ही साथ आन्तरिक आत्म- गुणों से भी युक्त बनें, ' - यह विचार अनुपयुक्त, अनुचित नहीं तो क्या है ? क्या परस्पर विरोधी दो विचारधाराएँ एक स्थान पर होना सम्भव है ? विभावदशा और स्वभावदशा- दोनों स्थितियों में आनन्दोपभोग करना कितना विचित्र और आश्चर्यकारक है ? एक तरफ एक सौ चार डिग्री ज्वर में उफनता हो और दूसरी ओर मिष्टान्न - स्वाद का गुदगुदानेवाला अनुभव होना जिस तरह सम्भव नहीं है, ठीक उसी तरह जब तक बाह्य (पौद्गलिक) सुख लूटने की क्रिया सतत शुरू हो, तृष्णा और लालसा की भूख मिटी न हो, तब तक पूर्णानन्द का अनुभव भी पूर्णतया असम्भव है, असमीचीन है, साथ ही अनुचित है ।
जैसे-जैसे हमारी इन्द्रियजन्य सुखों की स्पृहा नष्ट होती जाएगी, उपभोग की भावना कम होती जाएगी, वैसे-वैसे आत्मगुणों का आनन्द द्विगुणित होता हुआ निरन्तर बढ़ता जाएगा । मतलब, इन्द्रियजन्य सुखों की अपूर्णता ही आत्मगुणों की पूर्णता का प्रमुख कारण है । बिना कारण कोई बात नहीं बनती । यदि हमें आत्मगुणों में पूर्णानन्द का अनुभव करना हो तो अपनी तृष्णा, स्पृहा और इन्द्रियजन्य सुखों की लालसा का त्याग किये बिना कोई चारा नहीं है। मिठाई के स्वाद का मजा लूटना हो तो विषम ज्वर से मुक्ति पानी ही होगी। बीमारी के कारण मुँह में एक प्रकार की जो कडवाहट आ गयी है, उसे खत्म करना ही होगा ।
आत्मगुण के पूर्णानन्द का यह मूलभूत स्वभाव है कि वह इन्द्रिय-जन्य सुखों के साथ रह नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार इन्द्रियजन्य सुख का भी स्वभाव है कि वह आत्मगुण के पूर्णानन्द की संगति नहीं कर सकता । न जाने यह कैसा परस्पर विरोधी स्वभाव है ?
बाह्य सुखों का परित्याग कर जब आत्मा निज गुणों के पूर्णानन्द में खो जाती है, तब सृष्टि दिग्मूढ़ बन जाती है। जिन सुखों के बिना प्राणीमात्र का जीवन अपूर्ण है, असम्भव है, ऐसे सुख का त्याग कर अपूर्व आनन्द में आकण्ठ डूबा पूर्णानन्दी जीव, विश्व के लिये अद्भुत, महान् बन जाता है ।
परस्वत्वकृतोन्माथा, भूनाथा न्यूनतेक्षिणः । स्वस्वत्वसुखपूर्णस्य, न्यूनता न हरेरपि ॥७॥