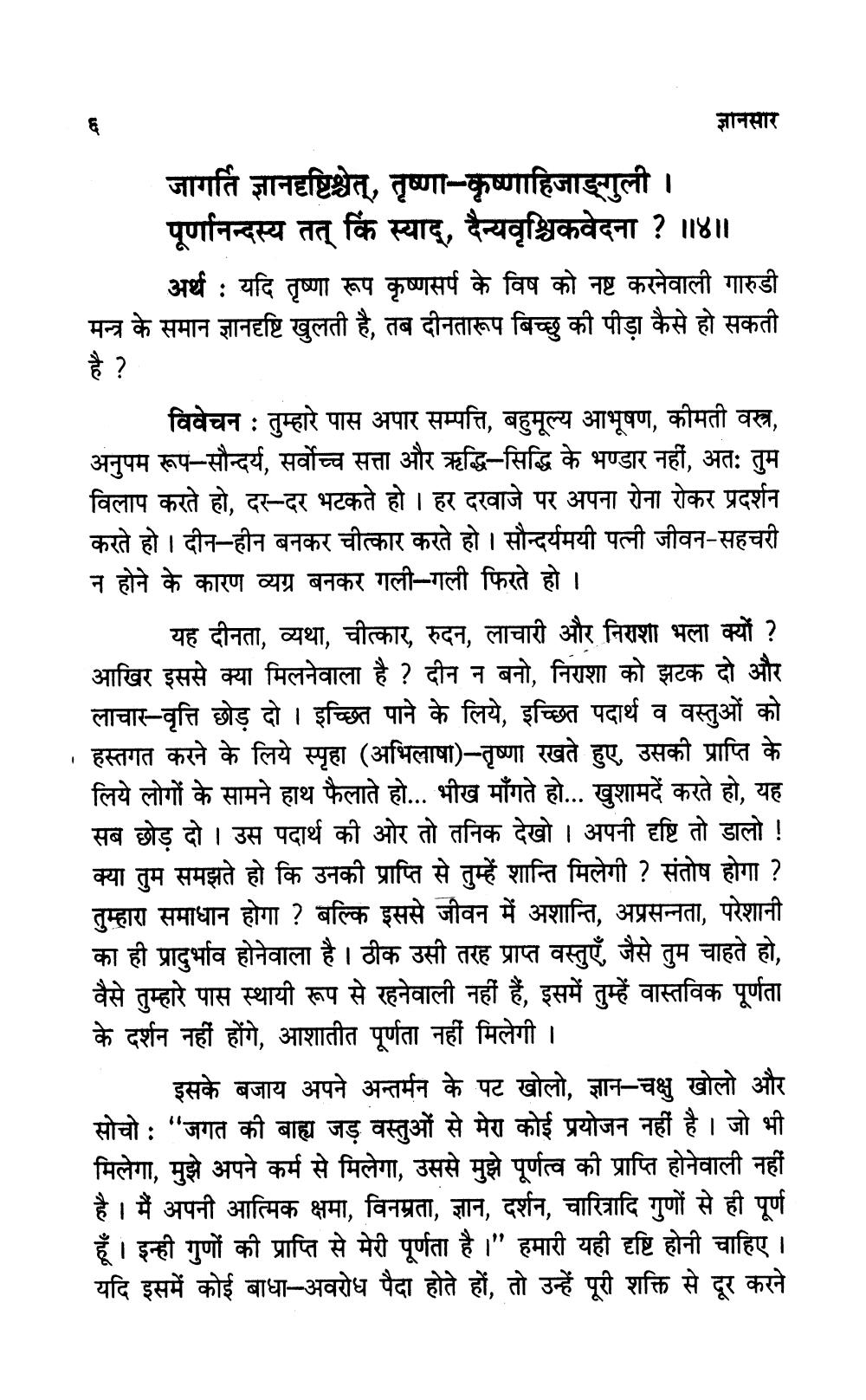________________
ज्ञानसार
जागर्ति ज्ञानदृष्टिश्चेत्, तृष्णा-कृष्णाहिजाङ्गुली । पूर्णानन्दस्य तत् किं स्याद्, दैन्यवृश्चिकवेदना ? ॥४॥
अर्थ : यदि तृष्णा रूप कृष्णसर्प के विष को नष्ट करनेवाली गारुडी मन्त्र के समान ज्ञानदृष्टि खुलती है, तब दीनतारूप बिच्छु की पीड़ा कैसे हो सकती है ?
विवेचन : तुम्हारे पास अपार सम्पत्ति, बहुमूल्य आभूषण, कीमती वस्त्र, अनुपम रूप-सौन्दर्य, सर्वोच्च सत्ता और ऋद्धि-सिद्धि के भण्डार नहीं, अतः तुम विलाप करते हो, दर-दर भटकते हो । हर दरवाजे पर अपना रोना रोकर प्रदर्शन करते हो । दीन-हीन बनकर चीत्कार करते हो । सौन्दर्यमयी पत्नी जीवन-सहचरी न होने के कारण व्यग्र बनकर गली-गली फिरते हो ।
यह दीनता, व्यथा, चीत्कार, रुदन, लाचारी और निराशा भला क्यों ? आखिर इससे क्या मिलनेवाला है ? दीन न बनो, निराशा को झटक दो और लाचार-वृत्ति छोड़ दो । इच्छित पाने के लिये, इच्छित पदार्थ व वस्तुओं को हस्तगत करने के लिये स्पृहा (अभिलाषा)-तृष्णा रखते हुए, उसकी प्राप्ति के लिये लोगों के सामने हाथ फैलाते हो... भीख माँगते हो... खुशामदें करते हो, यह सब छोड़ दो । उस पदार्थ की ओर तो तनिक देखो । अपनी दृष्टि तो डालो ! क्या तुम समझते हो कि उनकी प्राप्ति से तुम्हें शान्ति मिलेगी ? संतोष होगा? तुम्हारा समाधान होगा ? बल्कि इससे जीवन में अशान्ति, अप्रसन्नता, परेशानी का ही प्रादुर्भाव होनेवाला है । ठीक उसी तरह प्राप्त वस्तुएँ, जैसे तुम चाहते हो, वैसे तुम्हारे पास स्थायी रूप से रहनेवाली नहीं हैं, इसमें तुम्हें वास्तविक पूर्णता के दर्शन नहीं होंगे, आशातीत पूर्णता नहीं मिलेगी।
इसके बजाय अपने अन्तर्मन के पट खोलो, ज्ञान-चक्षु खोलो और सोचो : "जगत की बाह्य जड़ वस्तुओं से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है । जो भी मिलेगा, मुझे अपने कर्म से मिलेगा, उससे मुझे पूर्णत्व की प्राप्ति होनेवाली नहीं है । मैं अपनी आत्मिक क्षमा, विनम्रता, ज्ञान, दर्शन, चारित्रादि गुणों से ही पूर्ण हूँ। इन्ही गुणों की प्राप्ति से मेरी पूर्णता है।" हमारी यही दृष्टि होनी चाहिए । यदि इसमें कोई बाधा अवरोध पैदा होते हों, तो उन्हें पूरी शक्ति से दूर करने