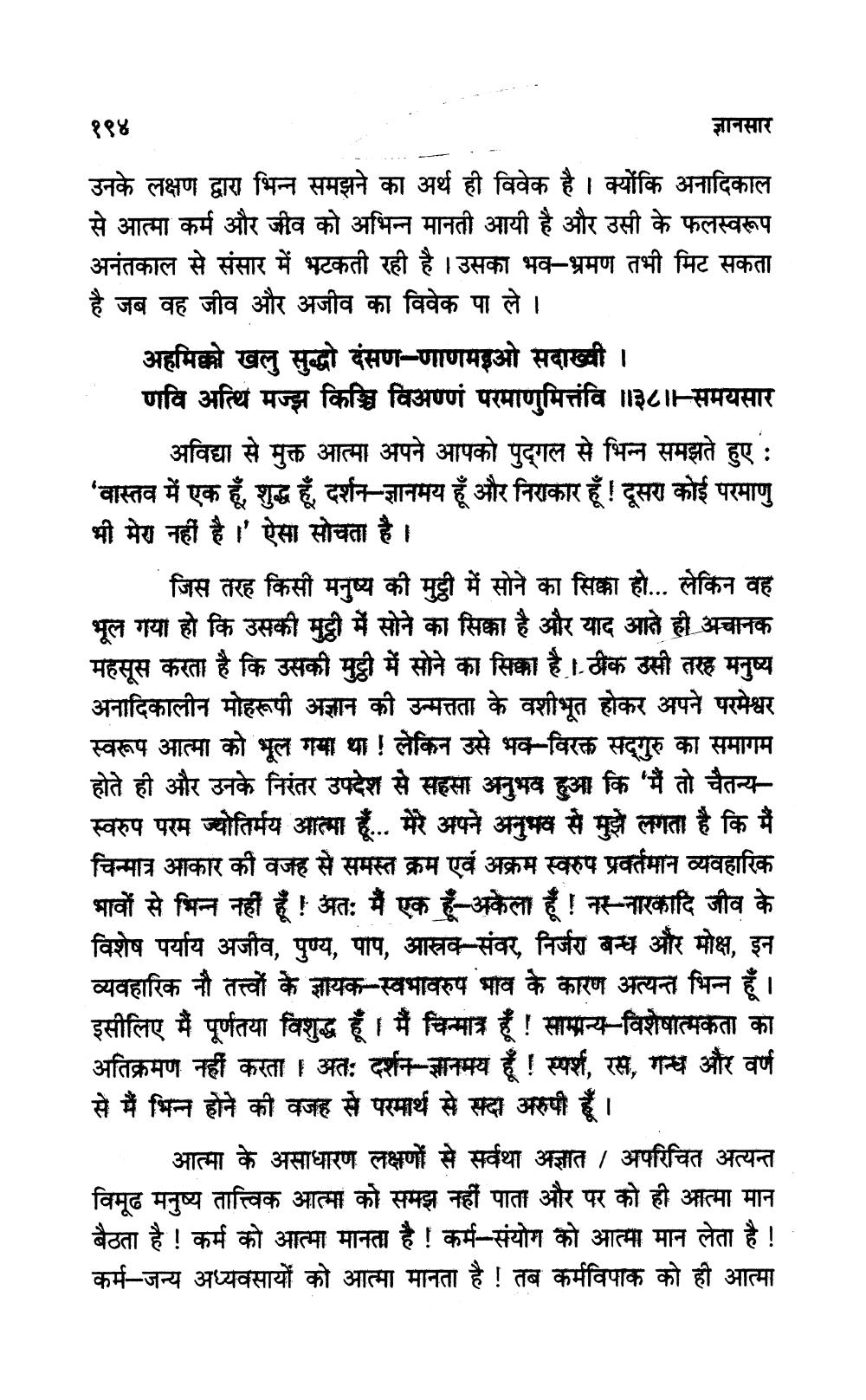________________
१९४
ज्ञानसार
उनके लक्षण द्वारा भिन्न समझने का अर्थ ही विवेक है। क्योंकि अनादिकाल से आत्मा कर्म और जीव को अभिन्न मानती आयी है और उसी के फलस्वरूप अनंतकाल से संसार में भटकती रही है । उसका भव-भ्रमण तभी मिट सकता है जब वह जीव और अजीव का विवेक पा ले ।
अहमिको खलु सुद्धो सण-णाणमइओ सदाबी । णवि अस्थि मज्झ किञ्चि विअण्णं परमाणुमित्तंवि ॥३८॥ समयसार
अविद्या से मुक्त आत्मा अपने आपको पुद्गल से भिन्न समझते हुए : 'वास्तव में एक हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शन-ज्ञानमय हूँ और निराकार हूँ ! दूसरा कोई परमाणु भी मेरा नहीं है।' ऐसा सोचता है।
जिस तरह किसी मनुष्य की मुट्ठी में सोने का सिक्का हो... लेकिन वह भूल गया हो कि उसकी मुट्ठी में सोने का सिक्का है और याद आते ही अचानक महसूस करता है कि उसकी मुट्ठी में सोने का सिक्का है। ठीक उसी तरह मनुष्य अनादिकालीन मोहरूपी अज्ञान की उन्मत्तता के वशीभूत होकर अपने परमेश्वर स्वरूप आत्मा को भूल गया था ! लेकिन उसे भक्-विरक्त सद्गुरु का समागम होते ही और उनके निरंतर उपदेश से सहसा अनुभव हुआ कि 'मैं तो चैतन्यस्वरुप परम ज्योतिर्मय आत्मा हूँ... मेरे अपने अनुभव से मुझे लगता है कि मैं चिन्मात्र आकार की वजह से समस्त क्रम एवं अक्रम स्वरुप प्रवर्तमान व्यवहारिक भावों से भिन्न नहीं हूँ ! अत: मैं एक हूँ-अकेला हूँ ! नर-नारकादि जीव के विशेष पर्याय अजीव, पुण्य, पाप, आस्त्रक-संवर, निर्जरा बन्ध और मोक्ष, इन व्यवहारिक नौ तत्त्वों के ज्ञायक-स्वभावरुप भाव के कारण अत्यन्त भिन्न हूँ। इसीलिए मैं पूर्णतया विशुद्ध हूँ। मैं चिमात्र हूँ ! साम्प्रन्य-विशेषात्मकता का अतिक्रमण नहीं करता । अत: दर्शन-ज्ञानमय हूँ ! स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण से मैं भिन्न होने की वजह से परमार्थ से सदा अरुपी हूँ।
आत्मा के असाधारण लक्षणों से सर्वथा अज्ञात / अपरिचित अत्यन्त विमूढ मनुष्य तात्त्विक आत्मा को समझ नहीं पाता और पर को ही आत्मा मान बैठता है ! कर्म को आत्मा मानता है ! कर्म-संयोग को आत्मा मान लेता है ! कर्म-जन्य अध्यवसायों को आत्मा मानता है ! तब कर्मविपाक को ही आत्मा