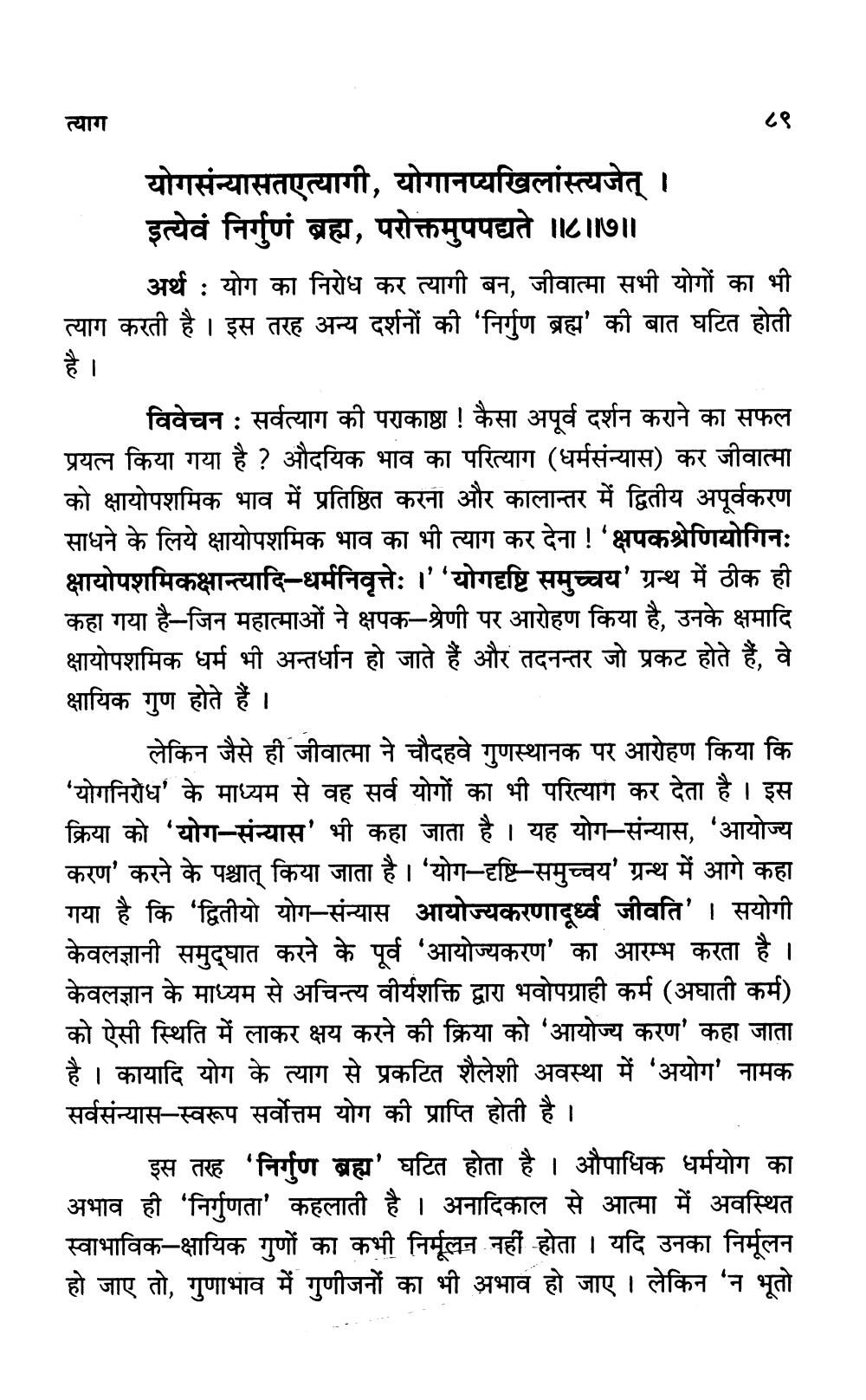________________
त्याग
योगसंन्यासतएत्यागी, योगानप्यखिलांस्त्यजेत् । इत्येवं निर्गुणं ब्रह्म, परोक्तमुपपद्यते ॥८॥७॥
८९
अर्थ : योग का निरोध कर त्यागी बन, जीवात्मा सभी योगों का भी त्याग करती है । इस तरह अन्य दर्शनों की 'निर्गुण ब्रह्म' की बात घटित होती है ।
विवेचन : सर्वत्याग की पराकाष्ठा ! कैसा अपूर्व दर्शन कराने का सफल प्रयत्न किया गया है ? औदयिक भाव का परित्याग ( धर्मसंन्यास) कर जीवात्मा को क्षायोपशमिक भाव में प्रतिष्ठित करना और कालान्तर में द्वितीय अपूर्वकरण साधने के लिये क्षायोपशमिक भाव का भी त्याग कर देना ! 'क्षपकश्रेणियोगिनः क्षायोपशमिकक्षान्त्यादि - धर्मनिवृत्तेः ।' 'योगदृष्टि समुच्चय' ग्रन्थ में ठीक ही कहा गया है - जिन महात्माओं ने क्षपक - श्रेणी पर आरोहण किया है, उनके क्षमादि क्षायोपशमिक धर्म भी अन्तर्धान हो जाते हैं और तदनन्तर जो प्रकट होते हैं, वे क्षायिक गुण होते हैं ।
लेकिन जैसे ही जीवात्मा ने चौदहवे गुणस्थानक पर आरोहण किया कि ‘योगनिरोध' के माध्यम से वह सर्व योगों का भी परित्याग कर देता है । इस क्रिया को 'योग - संन्यास' भी कहा जाता है । यह योग - संन्यास, 'आयोज्य करण' करने के पश्चात् किया जाता है । 'योग - दृष्टि - समुच्चय' ग्रन्थ में आगे कहा गया है कि 'द्वितीयो योग-संन्यास आयोज्यकरणादूर्ध्व जीवति' । सयोगी केवलज्ञानी समुद्घात करने के पूर्व 'आयोज्यकरण' का आरम्भ करता है । केवलज्ञान के माध्यम से अचिन्त्य वीर्यशक्ति द्वारा भवोपग्राही कर्म (अघाती कर्म) को ऐसी स्थिति में लाकर क्षय करने की क्रिया को 'आयोज्य करण' कहा जाता है । कायादि योग के त्याग से प्रकटित शैलेशी अवस्था में 'अयोग' नामक सर्वसंन्यास - स्वरूप सर्वोत्तम योग की प्राप्ति होती है ।
इस तरह 'निर्गुण ब्रह्म' घटित होता है । औपाधिक धर्मयोग का अभाव ही 'निर्गुणता' कहलाती है । अनादिकाल से आत्मा में अवस्थित स्वाभाविक - क्षायिक गुणों का कभी निर्मूलन नहीं होता । यदि उनका निर्मूलन हो जाए तो, गुणाभाव में गुणीजनों का भी अभाव हो जाए। लेकिन 'न भूतो