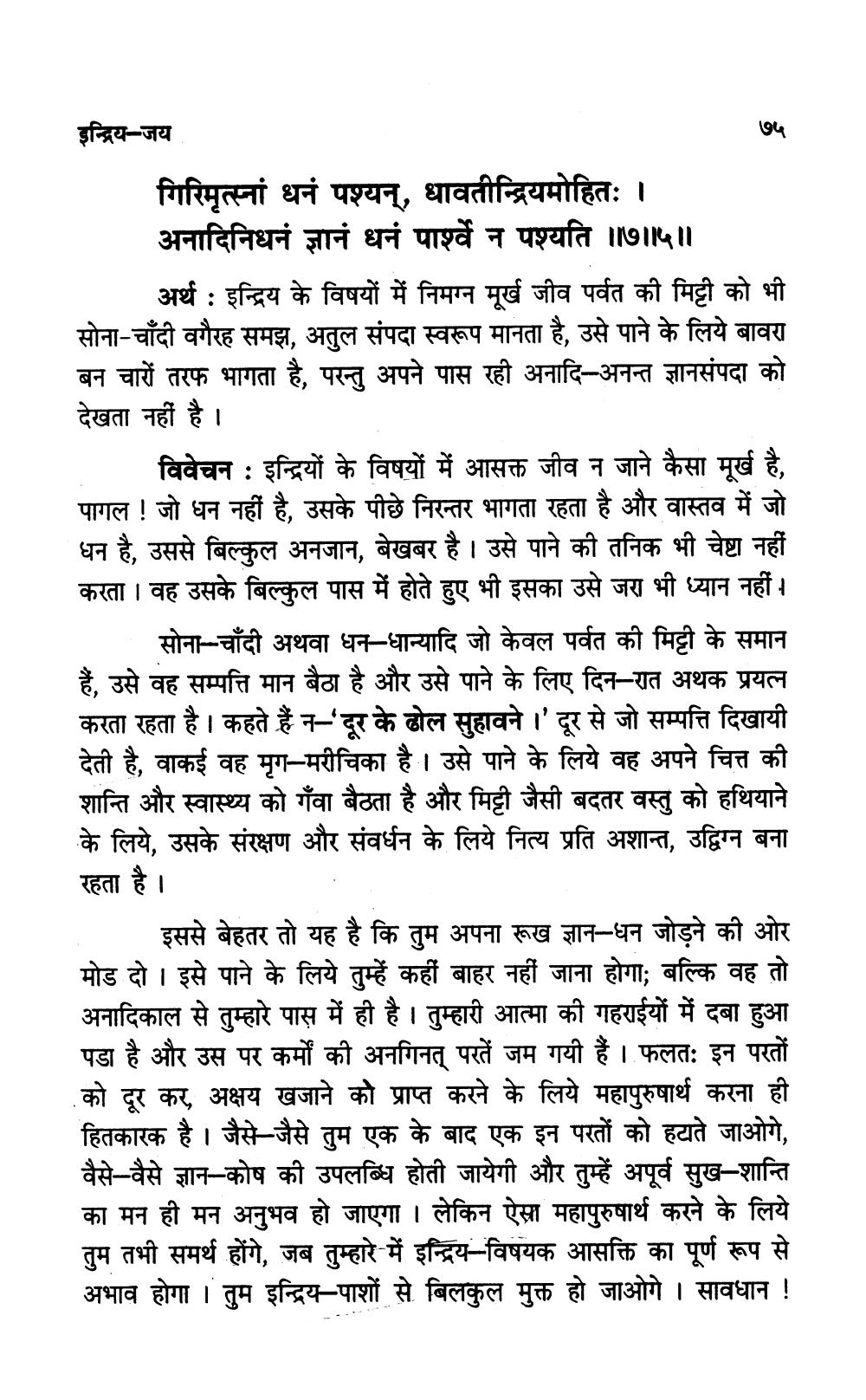________________
इन्द्रिय-जय
गिरिमृत्स्नां धनं पश्यन्, धावतीन्द्रियमोहितः । अनादिनिधनं ज्ञानं धनं पार्वे न पश्यति ॥७॥५॥
अर्थ : इन्द्रिय के विषयों में निमग्न मूर्ख जीव पर्वत की मिट्टी को भी सोना-चाँदी वगैरह समझ, अतुल संपदा स्वरूप मानता है, उसे पाने के लिये बावरा बन चारों तरफ भागता है, परन्तु अपने पास रही अनादि-अनन्त ज्ञानसंपदा को देखता नहीं है।
विवेचन : इन्द्रियों के विषयों में आसक्त जीव न जाने कैसा मूर्ख है, पागल ! जो धन नहीं है, उसके पीछे निरन्तर भागता रहता है और वास्तव में जो धन है, उससे बिल्कुल अनजान, बेखबर है । उसे पाने की तनिक भी चेष्टा नहीं करता । वह उसके बिल्कुल पास में होते हुए भी इसका उसे जरा भी ध्यान नहीं ।
सोनाचाँदी अथवा धन-धान्यादि जो केवल पर्वत की मिट्टी के समान हैं, उसे वह सम्पत्ति मान बैठा है और उसे पाने के लिए दिन-रात अथक प्रयत्न करता रहता है। कहते हैं न 'दूर के ढोल सुहावने ।' दूर से जो सम्पत्ति दिखायी देती है, वाकई वह मृग-मरीचिका है। उसे पाने के लिये वह अपने चित्त की शान्ति और स्वास्थ्य को गँवा बैठता है और मिट्टी जैसी बदतर वस्तु को हथियाने के लिये, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिये नित्य प्रति अशान्त, उद्विग्न बना रहता है।
इससे बेहतर तो यह है कि तुम अपना रूख ज्ञान-धन जोड़ने की ओर मोड दो । इसे पाने के लिये तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना होगा; बल्कि वह तो अनादिकाल से तुम्हारे पास में ही है । तुम्हारी आत्मा की गहराईयों में दबा हुआ पडा है और उस पर कर्मों की अनगिनत परतें जम गयी हैं। फलतः इन परतों को दूर कर, अक्षय खजाने को प्राप्त करने के लिये महापुरुषार्थ करना ही हितकारक है । जैसे-जैसे तुम एक के बाद एक इन परतों को हटाते जाओगे, वैसे-वैसे ज्ञान-कोष की उपलब्धि होती जायेगी और तुम्हें अपूर्व सुख-शान्ति का मन ही मन अनुभव हो जाएगा । लेकिन ऐसा महापुरुषार्थ करने के लिये तुम तभी समर्थ होंगे, जब तुम्हारे में इन्द्रिय-विषयक आसक्ति का पूर्ण रूप से अभाव होगा । तुम इन्द्रिय-पाशों से बिलकुल मुक्त हो जाओगे । सावधान !