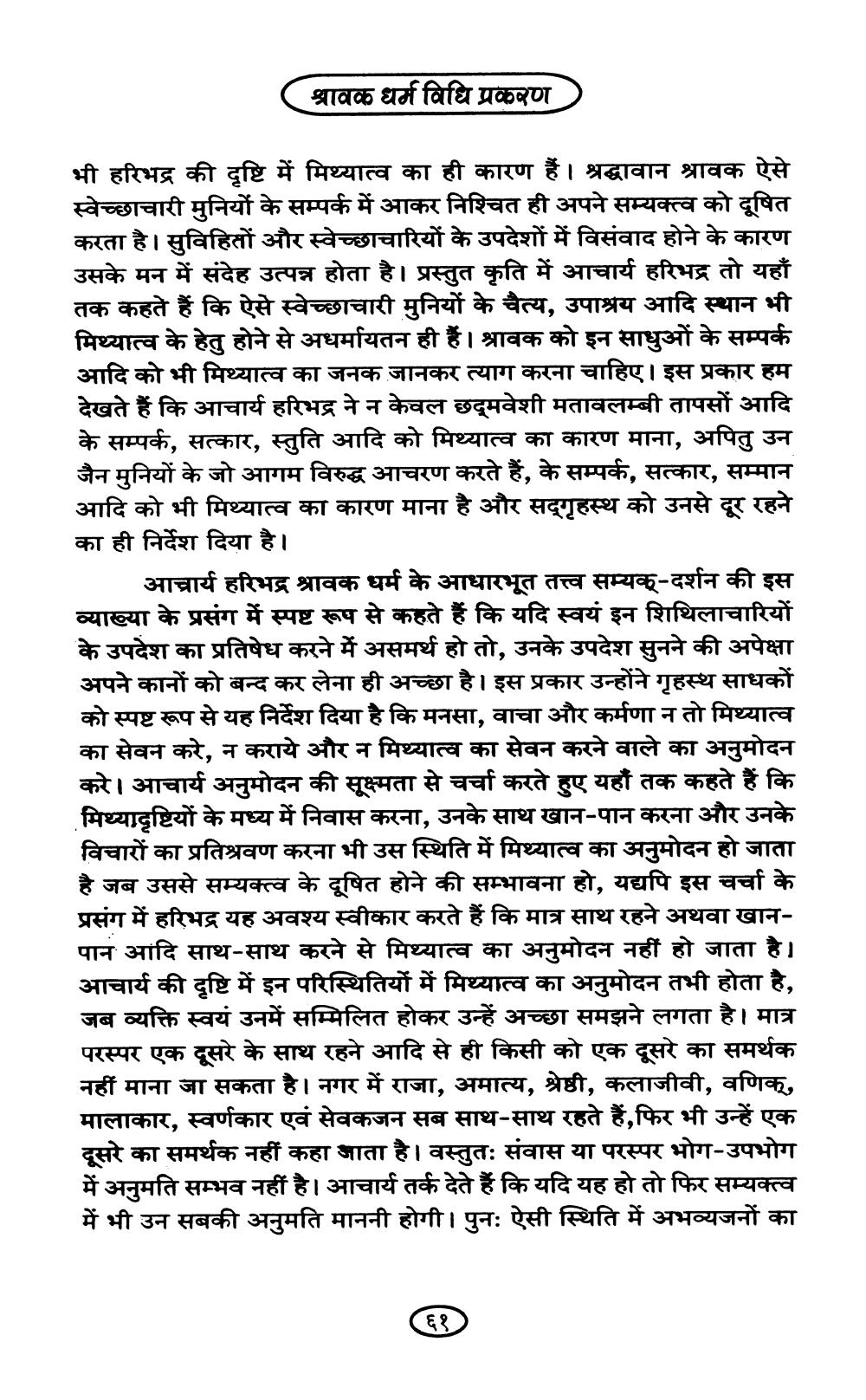________________
(श्रावक धर्म विधि प्रकरण)
भी हरिभद्र की दृष्टि में मिथ्यात्व का ही कारण हैं। श्रद्धावान श्रावक ऐसे स्वेच्छाचारी मुनियों के सम्पर्क में आकर निश्चित ही अपने सम्यक्त्व को दूषित करता है। सुविहितों और स्वेच्छाचारियों के उपदेशों में विसंवाद होने के कारण उसके मन में संदेह उत्पन्न होता है। प्रस्तुत कृति में आचार्य हरिभद्र तो यहाँ तक कहते हैं कि ऐसे स्वेच्छाचारी मुनियों के चैत्य, उपाश्रय आदि स्थान भी मिथ्यात्व के हेतु होने से अधर्मायतन ही हैं। श्रावक को इन साधुओं के सम्पर्क
आदि को भी मिथ्यात्व का जनक जानकर त्याग करना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य हरिभद्र ने न केवल छद्मवेशी मतावलम्बी तापसों आदि के सम्पर्क, सत्कार, स्तुति आदि को मिथ्यात्व का कारण माना, अपितु उन जैन मुनियों के जो आगम विरुद्ध आचरण करते हैं, के सम्पर्क, सत्कार, सम्मान आदि को भी मिथ्यात्व का कारण माना है और सद्गृहस्थ को उनसे दूर रहने का ही निर्देश दिया है।
आचार्य हरिभद्र श्रावक धर्म के आधारभूत तत्त्व सम्यक्-दर्शन की इस व्याख्या के प्रसंग में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यदि स्वयं इन शिथिलाचारियों के उपदेश का प्रतिषेध करने में असमर्थ हो तो, उनके उपदेश सुनने की अपेक्षा अपने कानों को बन्द कर लेना ही अच्छा है। इस प्रकार उन्होंने गृहस्थ साधकों को स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिया है कि मनसा, वाचा और कर्मणा न तो मिथ्यात्व का सेवन करे, न कराये और न मिथ्यात्व का सेवन करने वाले का अनुमोदन करे। आचार्य अनुमोदन की सूक्ष्मता से चर्चा करते हुए यहाँ तक कहते हैं कि मिथ्यादृष्टियों के मध्य में निवास करना, उनके साथ खान-पान करना और उनके विचारों का प्रतिश्रवण करना भी उस स्थिति में मिथ्यात्व का अनुमोदन हो जाता है जब उससे सम्यक्त्व के दूषित होने की सम्भावना हो, यद्यपि इस चर्चा के प्रसंग में हरिभद्र यह अवश्य स्वीकार करते हैं कि मात्र साथ रहने अथवा खानपान आदि साथ-साथ करने से मिथ्यात्व का अनुमोदन नहीं हो जाता है। आचार्य की दृष्टि में इन परिस्थितियों में मिथ्यात्व का अनुमोदन तभी होता है, जब व्यक्ति स्वयं उनमें सम्मिलित होकर उन्हें अच्छा समझने लगता है। मात्र परस्पर एक दूसरे के साथ रहने आदि से ही किसी को एक दूसरे का समर्थक नहीं माना जा सकता है। नगर में राजा, अमात्य, श्रेष्ठी, कलाजीवी, वणिक्, मालाकार, स्वर्णकार एवं सेवकजन सब साथ-साथ रहते हैं,फिर भी उन्हें एक दूसरे का समर्थक नहीं कहा जाता है। वस्तुत: संवास या परस्पर भोग-उपभोग में अनुमति सम्भव नहीं है। आचार्य तर्क देते हैं कि यदि यह हो तो फिर सम्यक्त्व में भी उन सबकी अनुमति माननी होगी। पुन: ऐसी स्थिति में अभव्यजनों का
(६१)